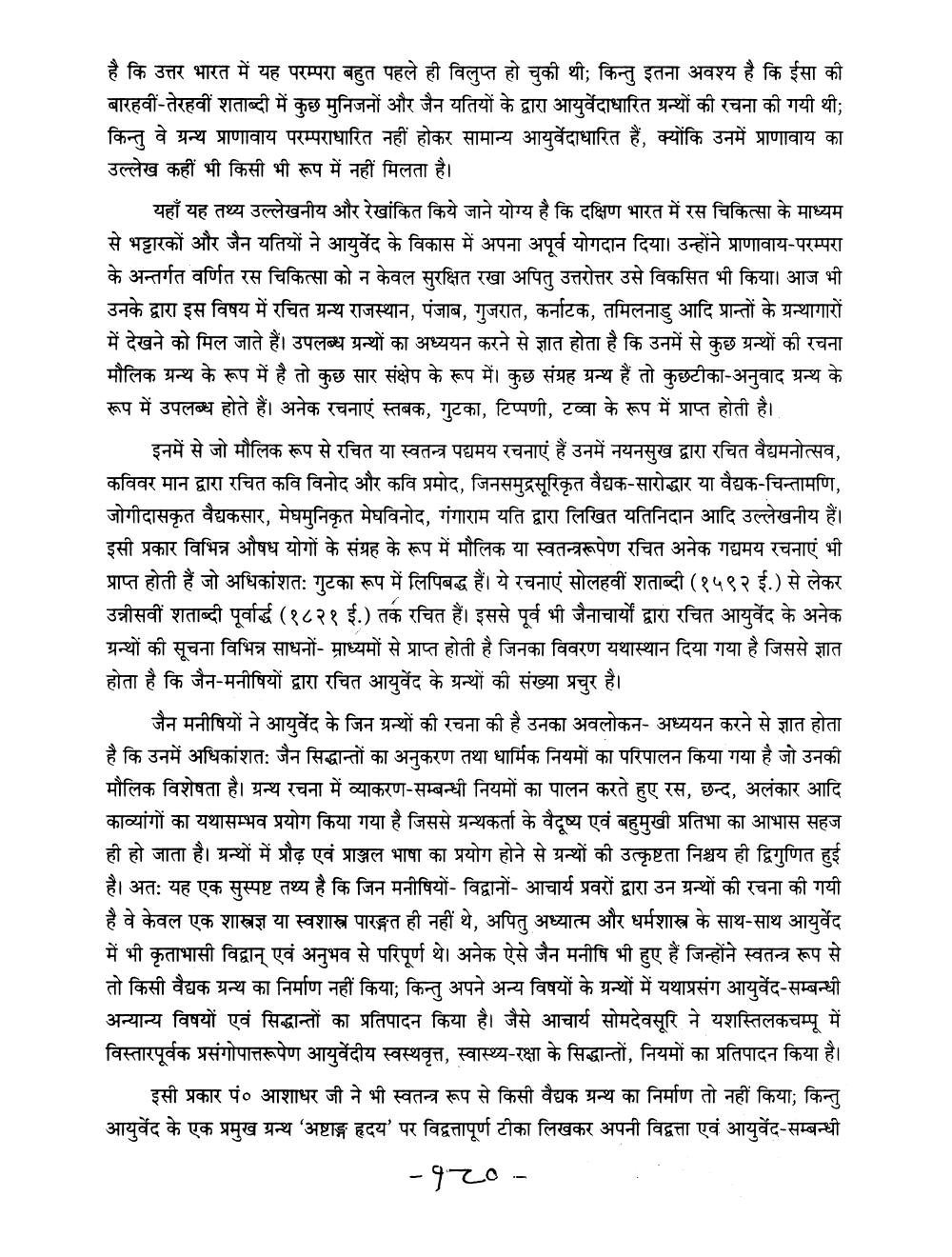________________ है कि उत्तर भारत में यह परम्परा बहुत पहले ही विलुप्त हो चुकी थी; किन्तु इतना अवश्य है कि ईसा की बारहवीं-तेरहवीं शताब्दी में कुछ मुनिजनों और जैन यतियों के द्वारा आयुर्वेदाधारित ग्रन्थों की रचना की गयी थी; किन्तु वे ग्रन्थ प्राणावाय परम्पराधारित नहीं होकर सामान्य आयुर्वेदाधारित हैं, क्योंकि उनमें प्राणावाय का उल्लेख कहीं भी किसी भी रूप में नहीं मिलता है। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय और रेखांकित किये जाने योग्य है कि दक्षिण भारत में रस चिकित्सा के माध्यम से भट्टारकों और जैन यतियों ने आयुर्वेद के विकास में अपना अपूर्व योगदान दिया। उन्होंने प्राणावाय-परम्परा के अन्तर्गत वर्णित रस चिकित्सा को न केवल सुरक्षित रखा अपितु उत्तरोत्तर उसे विकसित भी किया। आज भी उनके द्वारा इस विषय में रचित ग्रन्थ राजस्थान, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि प्रान्तों के ग्रन्थागारों में देखने को मिल जाते हैं। उपलब्ध ग्रन्थों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि उनमें से कुछ ग्रन्थों की रचना मौलिक ग्रन्थ के रूप में है तो कुछ सार संक्षेप के रूप में। कुछ संग्रह ग्रन्थ हैं तो कुछटीका-अनुवाद ग्रन्थ के रूप में उपलब्ध होते हैं। अनेक रचनाएं स्तबक, गुटका, टिप्पणी, टव्वा के रूप में प्राप्त होती है। इनमें से जो मौलिक रूप से रचित या स्वतन्त्र पद्यमय रचनाएं हैं उनमें नयनसुख द्वारा रचित वैद्यमनोत्सव, कविवर मान द्वारा रचित कवि विनोद और कवि प्रमोद, जिनसमुद्रसूरिकृत वैद्यक-सारोद्धार या वैद्यक-चिन्तामणि, जोगीदासकृत वैद्यकसार, मेघमुनिकृत मेघविनोद, गंगाराम यति द्वारा लिखित यतिनिदान आदि उल्लेखनीय हैं। इसी प्रकार विभिन्न औषध योगों के संग्रह के रूप में मौलिक या स्वतन्त्ररूपेण रचित अनेक गद्यमय रचनाएं भी प्राप्त होती हैं जो अधिकांशत: गुटका रूप में लिपिबद्ध हैं। ये रचनाएं सोलहवीं शताब्दी (1592 ई.) से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी पूर्वार्द्ध (1821 ई.) तक रचित हैं। इससे पूर्व भी जैनाचार्यों द्वारा रचित आयुर्वेद के अनेक ग्रन्थों की सूचना विभिन्न साधनों- माध्यमों से प्राप्त होती है जिनका विवरण यथास्थान दिया गया है जिससे ज्ञात होता है कि जैन-मनीषियों द्वारा रचित आयुर्वेद के ग्रन्थों की संख्या प्रचुर है। जैन मनीषियों ने आयुर्वेद के जिन ग्रन्थों की रचना की है उनका अवलोकन- अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि उनमें अधिकांशत: जैन सिद्धान्तों का अनुकरण तथा धार्मिक नियमों का परिपालन किया गया है जो उनकी मौलिक विशेषता है। ग्रन्थ रचना में व्याकरण-सम्बन्धी नियमों का पालन करते हुए रस, छन्द, अलंकार आदि काव्यांगों का यथासम्भव प्रयोग किया गया है जिससे ग्रन्थकर्ता के वैदृष्य एवं बहमुखी प्रतिभा का आभास सहज ही हो जाता है। ग्रन्थों में प्रौढ़ एवं प्राञ्जल भाषा का प्रयोग होने से ग्रन्थों की उत्कृष्टता निश्चय ही द्विगुणित हुई है। अत: यह एक सस्पष्ट तथ्य है कि जिन मनीषियों- विद्वानों- आचार्य प्रवरों द्वारा उन ग्रन्थों की रचना की गयी है वे केवल एक शास्त्रज्ञ या स्वशास्त्र पारङ्गत ही नहीं थे, अपितु अध्यात्म और धर्मशास्त्र के साथ-साथ आयुर्वेद में भी कृताभासी विद्वान् एवं अनुभव से परिपूर्ण थे। अनेक ऐसे जैन मनीषि भी हुए हैं जिन्होंने स्वतन्त्र रूप से तो किसी वैद्यक ग्रन्थ का निर्माण नहीं किया; किन्तु अपने अन्य विषयों के ग्रन्थों में यथाप्रसंग आयुर्वेद-सम्बन्धी अन्यान्य विषयों एवं सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। जैसे आचार्य सोमदेवसूरि ने यशस्तिलकचम्पू में विस्तारपूर्वक प्रसंगोपात्तरूपेण आयुर्वेदीय स्वस्थवृत्त, स्वास्थ्य-रक्षा के सिद्धान्तों, नियमों का प्रतिपादन किया है। इसी प्रकार पं० आशाधर जी ने भी स्वतन्त्र रूप से किसी वैद्यक ग्रन्थ का निर्माण तो नहीं किया; किन्तु आयुर्वेद के एक प्रमुख ग्रन्थ 'अष्टाङ्ग हृदय' पर विद्वत्तापूर्ण टीका लिखकर अपनी विद्वत्ता एवं आयुर्वेद-सम्बन्धी -180 -