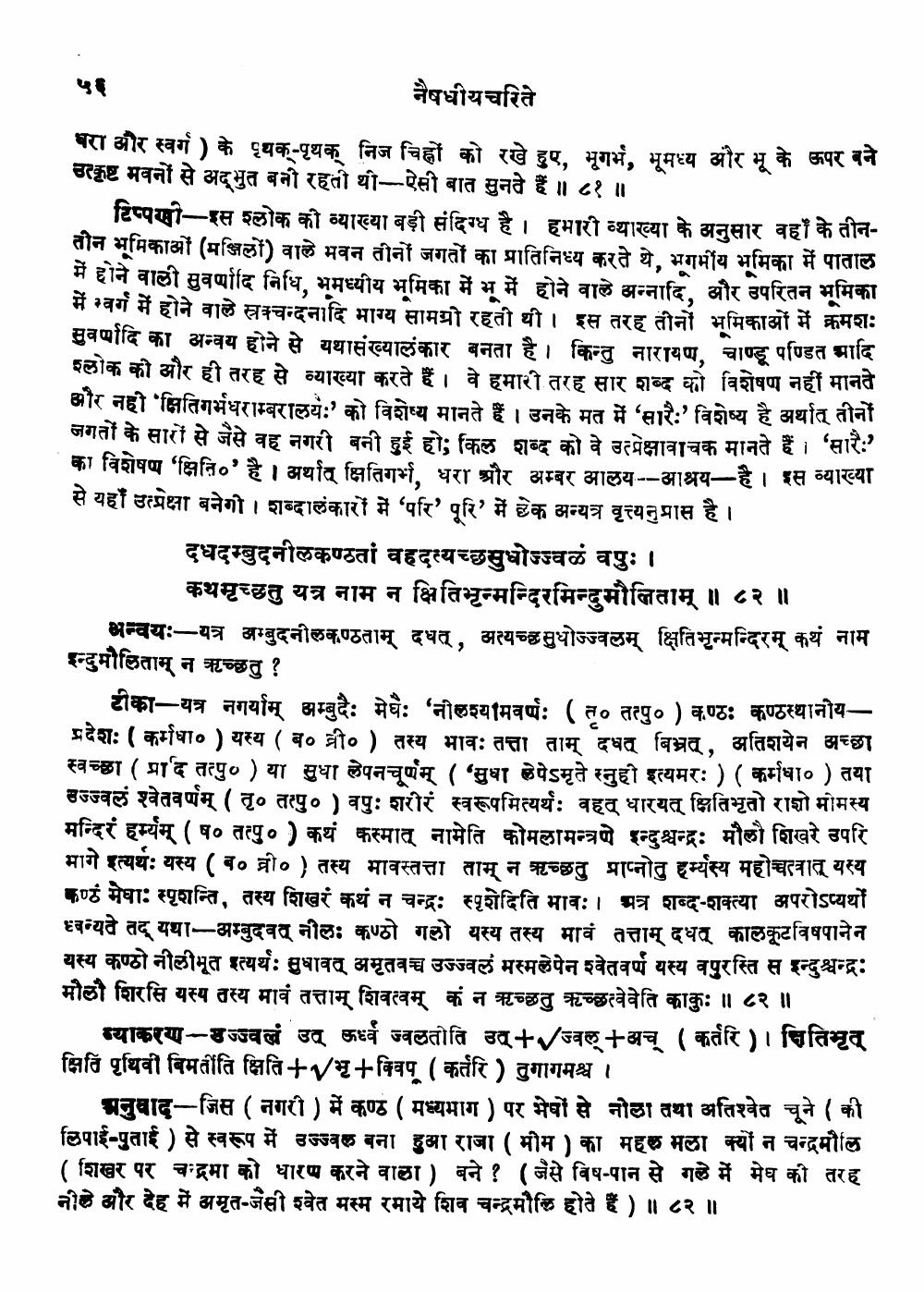________________ नैषधीयचरिते धरा और स्वर्ग) के पृथक्-पृथक् निज चिह्नों को रखे हुए, भूगर्भ, भूमध्य और भू के ऊपर बने उत्कृष्ट मवनों से अद्भुत बनी रहती थी-ऐसी बात सुनते हैं // 81 // टिप्पणी-इस श्लोक की व्याख्या बड़ी संदिग्ध है। हमारी व्याख्या के अनुसार वहाँ के तीनतीन भूमिकाओं (मजिलों) वाले भवन तीनों जगतों का प्रातिनिध्य करते थे, भगर्भीय भूमिका में पाताल में होने वाली सुवर्णादि निधि, भमध्यीय भमिका में भ में होने वाले अन्नादि, और उपरितन भूमिका में स्वर्ग में होने वाले स्रक्चन्दनादि भाग्य सामग्री रहती थी। इस तरह तीनों भूमिकाओं में क्रमशः सुवणादि का अन्वय होने से यथासंख्यालंकार बनता है। किन्तु नारायण, चाण्डू पण्डित मादि श्लोक को और ही तरह से व्याख्या करते हैं। वे हमारी तरह सार शब्द को विशेषण नहीं मानत और नही 'क्षितिगर्भधराम्बरालयः' को विशेष्य मानते हैं। उनके मत में 'सारैः' विशेष्य है अर्थात् तीनों जगतों के सारों से जैसे वह नगरी बनी हुई हो; किल शब्द को वे उत्प्रेक्षावाचक मानते हैं। 'सारः' का विशेषण 'क्षिति०' है। अर्थात् क्षितिगर्भ, धरा और अम्बर आलय--आश्रय-है। इस व्याख्या से यहाँ उत्प्रेक्षा बनेगी। शब्दालंकारों में 'परि' पूरि' में छेक अन्यत्र वृत्त्यनुप्रास है। दधदम्बुदनीलकण्ठतां वहदत्यच्छसुधोज्ज्वळं वपुः / कथमृच्छतु यत्र नाम न क्षितिभृन्मन्दिरमिन्दुमौलिताम् // 82 // अन्वयः-यत्र अम्बुदनीलकण्ठताम् दधत् , अत्यच्छ सुधोज्ज्वलम् क्षितिभृन्मन्दिरम् कथं नाम इन्दुमौलिताम् न ऋच्छतु ? टीका-यत्र नगर्याम् अम्बुदैः मेघैः 'नीलश्यामवर्णः (त. तत्पु० ) कण्ठः कण्ठस्थानीयप्रदेशः ( कर्मधा० ) यस्य (ब० वी० ) तस्य भावः तत्ता ताम् दधत् बिभ्रत् , अतिशयेन अच्छा स्वच्छा ( प्रादि तत्पु० ) या सुधा लेपनचूर्णम् ( 'सुधा लेपेऽमृते स्नुही इत्यमरः) (कर्मधा० ) तया उज्ज्वलं श्वेतवर्णम् ( तृ० तत्पु० ) वपुः शरीरं स्वरूपमित्यर्थः वहत् धारयत् क्षितिभृतो राशो मोमस्य मन्दिरं हर्म्यम् (10 तत्पु०) कथं कस्मात् नामेति कोमलामन्त्रणे इन्दुश्चन्द्रः मौलो शिखरे उपरि मागे इत्यर्थः यस्य (ब० वी० ) तस्य मावस्तत्ता ताम् न ऋच्छतु प्राप्नोतु हर्म्यस्य महोच्चत्वात् यस्य कण्ठं मेघाः स्पृशन्ति, तस्य शिखरं कथं न चन्द्रः स्पृशेदिति भावः। अत्र शब्द-शक्त्या अपरोऽप्यर्थों ध्वन्यते तद् यथा-अम्बुदवत् नीलः कण्ठो गलो यस्य तस्य मावं तत्ताम् दधत् कालकूट विषपानेन यस्य कण्ठो नीलीभूत इत्यर्थः सुधावत् अमृतवच्च उज्ज्वलं मस्मलेपेन श्वेतवर्ण यस्य वपुरस्ति स इन्दुश्चन्द्रः मौली शिरसि यस्य तस्य मावं तत्ताम् शिवत्वम् कं न ऋच्छतु ऋच्छत्वेवेति काकुः // 82 // ज्याकरण-उज्ज्वलं उत् ऊर्ध्व ज्वलतोति उत्+/ज्वल् +अच् ( कर्तरि ) / सितिभृत् क्षितिं पृथिवी बिमतीति क्षिति+/भृ+क्विप ( कर्तरि ) तुगागमश्च / / अनुवाद-जिस ( नगरी ) में कण्ठ ( मध्यभाग) पर भेषों से नोला तथा अतिश्वेत चूने ( की लिपाई-पुताई ) से स्वरूप में उज्ज्वल बना हुआ राजा (भीम ) का महरू मला क्यों न चन्द्रमौलि ( शिखर पर चन्द्रमा को धारण करने वाला) बने ? (जैसे विष-पान से गले में मेघ की तरह नीले और देह में अमृत-जैसी श्वेत मस्म रमाये शिव चन्द्रमौलि होते हैं ) // 82 //