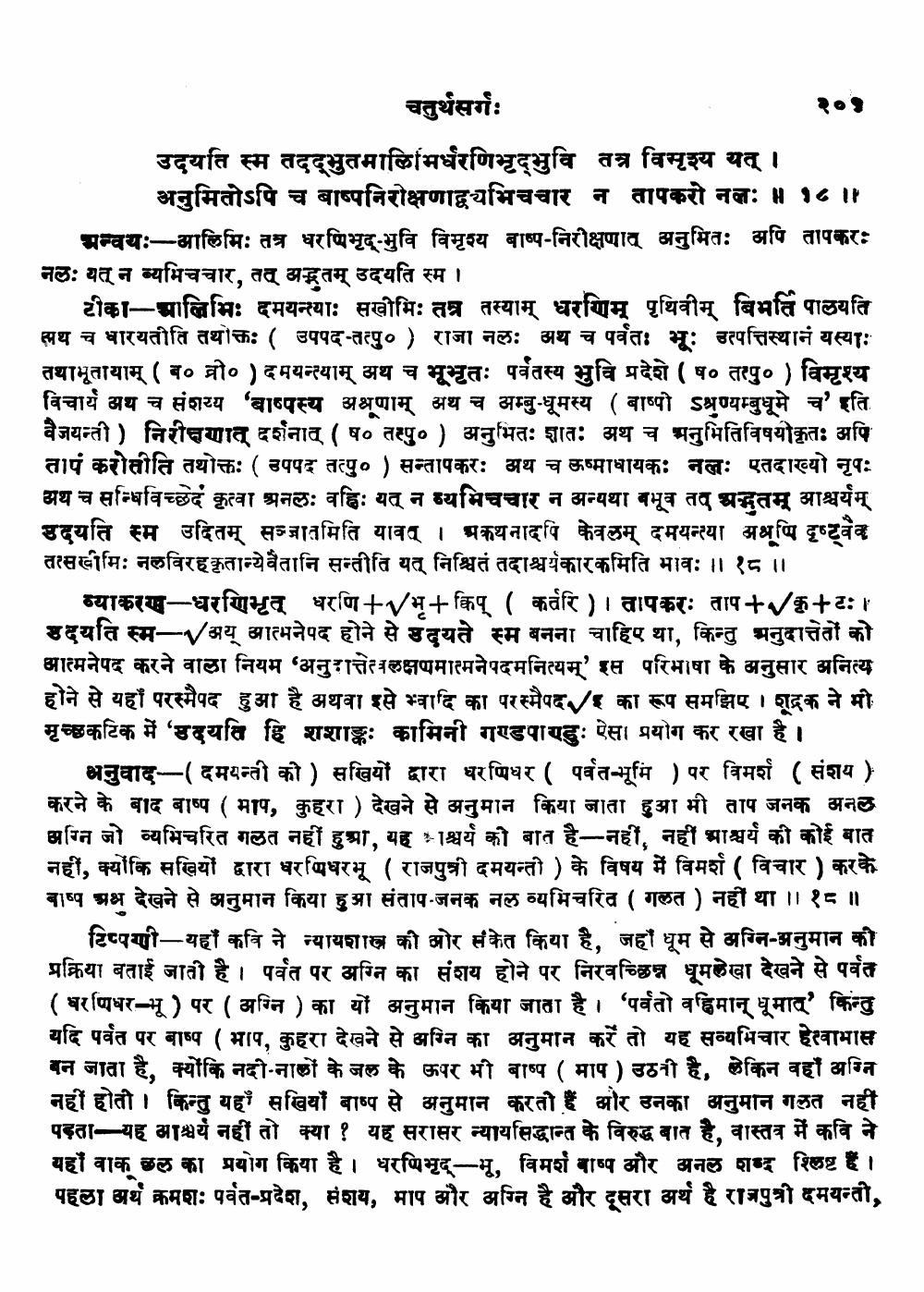________________ चतुर्थसर्गः उदयति स्म तदद्भुतमालिमिर्धरणिभृद्भुवि तत्र विमृश्य यत् / अनुमितोऽपि च बाष्पनिरोक्षणाद्वयभिचचार न तापकरो नलः // 18 // अन्वयः-आलिमिः तत्र धरणिभृद्-भुवि विमृश्य बाष्प-निरीक्षणात् अनुमितः अपि तापकरः नलः यत् न व्यभिचचार, तत् अद्भुतम् उदयति स्म / टीका-प्रालिभिः दमयन्त्याः सखीमिः तत्र तस्याम् धरणिम् पृथिवीम् बिमति पालयति स्मथ च धारयतीति तथोक्तः ( उपपद-तत्पु०) राजा नलः अथ च पर्वतः भूः उत्पत्तिस्थानं यस्याः तथाभूतायाम् (ब० बी० ) दमयन्त्याम् अथ च भूभृतः पर्वतस्य भुवि प्रदेशे (10 तत्पु० ) विमृश्य विचार्य अथ च संशय्य 'बाष्पस्य अश्रणाम् अथ च अम्बु-धूमस्य (बाष्पो ऽश्रुण्यम्बुधूमे च' इति वैजयन्ती) निरीक्षणात् दर्शनात् ( 10 तत्पु० ) अनुभितः ज्ञातः अथ च अनुभितिविषयोकृतः अपि तापं करोतीति तथोक्तः ( उपपद तत्पु० ) सन्तापकरः अथ च ऊष्माधायकः नलः एतदाख्यो नृपः अथ च सन्धिविच्छेदं कृत्वा अनलः वह्निः यत् न व्यमिचचार न अन्यथा बभूव तव अद्भुतम् आश्चर्यम् उदयति स्म उदितम् सनातमिति यावत् / प्रकथनादपि केवलम् दमयन्त्या अणि दृष्ट्वैक तत्सखीमिः नलविरहकृतान्ये वैतानि सन्तीति यत् निश्चितं तदाश्चर्यकारकमिति भावः / / 18 / / व्याकरण-धरणिभृत् धरणि+भ+ विप् ( कर्तरि / तापकरः ताप+V+। उदयति स्म-/अय् आत्मनेपद होने से उदयते स्म बनना चाहिए था, किन्तु अनुदात्तेतों को आत्मनेपद करने वाला नियम 'अनुदात्तत्वलक्षणमात्मनेपदमनित्यम्' इस परिभाषा के अनुसार अनित्य होने से यहाँ परस्मैपद हुआ है अथवा इसे भ्वादि का परस्मैपद का रूप समझिए / शद्रक ने मी मृच्छकटिक में 'उदयति हि शशाङ्कः कामिनी गण्डपाण्डः ऐसा प्रयोग कर रखा है। अनुवाद-(दमयन्ती को) सखियों द्वारा धरणिधर ( पर्वत-भूमि ) पर विमर्श (संशय ) करने के बाद बाष्प ( माप, कुहरा ) देखने से अनुमान किया जाता हुआ भी ताप जनक अनल अग्नि जो व्यभिचरित गलत नहीं हुआ, यह श्चर्य की बात है-नहीं, नहीं भाश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि सखियों द्वारा धरणिधरभू ( राजपुत्री दमयन्ती) के विषय में विमर्श ( विचार ) करके बाष्प प्रभु देखने से अनुमान किया हुआ संताप-जनक नल व्यभिचरित ( गलत ) नहीं था / / 18 // टिप्पणी-यहाँ कवि ने न्यायशास्त्र की ओर संकेत किया है, जहाँ धूम से अग्नि-अनुमान की प्रक्रिया बताई जाती है। पर्वत पर अग्नि का संशय होने पर निरवच्छिन्न धूमलेखा देखने से पर्वत (धरणिधर-भू ) पर ( अग्नि ) का यों अनुमान किया जाता है। 'पर्वतो वह्निमान् धूमात्' किन्तु यदि पर्वत पर बाष्प ( भाप, कुहरा देखने से अग्नि का अनुमान करें तो यह सव्यभिचार हेत्वाभास बन जाता है, क्योंकि नदी-नालों के जल के ऊपर भी बाष्प ( माप ) उठती है, लेकिन वहाँ अग्नि नहीं होती। किन्तु यहाँ सखियों बाष्प से अनुमान करती हैं और उनका अनुमान गलत नहीं पड़ता-यह आश्चर्य नहीं तो क्या ? यह सरासर न्यायसिद्धान्त के विरुद्ध बात है, वास्तव में कवि ने यहाँ वाक छल का प्रयोग किया है। धरणिभृद्-भू, विमर्श वाष्प और अनल शब्द श्लिष्ट हैं। पहला अर्थ क्रमशः पर्वत-प्रदेश, संशय, माप और अग्नि है और दूसरा अर्थ है राजपुत्री दमयन्ती,