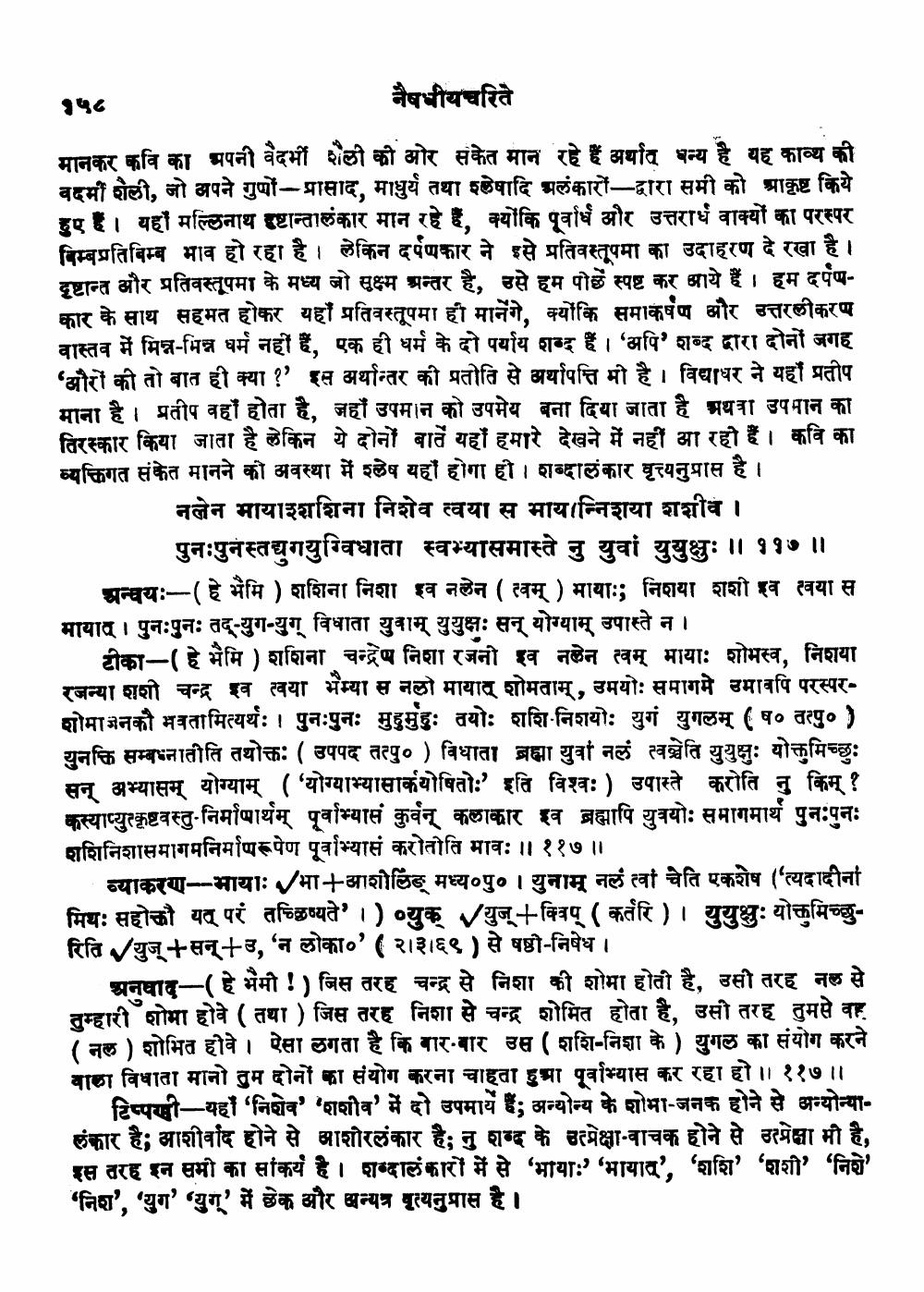________________ 150 नैषधीयचरिते मानकर कवि का अपनी वैदर्भी शैली की ओर संकेत मान रहे हैं अर्थात् धन्य है यह काव्य की वदमी शैली, जो अपने गुणों-प्रासाद, माधुर्य तथा श्लेषादि भलंकारों द्वारा समी को आकृष्ट किये हुए हैं। यहाँ मल्लिनाथ दृष्टान्तालंकार मान रहे हैं, क्योंकि पूर्वार्ध और उत्तरार्ध वाक्यों का परस्पर विम्बप्रतिबिम्ब भाव हो रहा है। लेकिन दर्पणकार ने इसे प्रतिवस्तूपमा का उदाहरण दे रखा है। दृष्टान्त और प्रतिवस्तूपमा के मध्य जो सूक्ष्म अन्तर है, उसे हम पोछे स्पष्ट कर आये हैं। हम दर्पणकार के साथ सहमत होकर यहाँ प्रतिवस्तूपमा ही मानेंगे, क्योंकि समाकर्षण और उत्तरलीकरण वास्तव में मिन्न-भिन्न धर्म नहीं हैं, एक ही धर्म के दो पर्याय शब्द हैं। 'अपि' शब्द द्वारा दोनों जगह 'औरों की तो बात ही क्या ?' इस अर्थान्तर की प्रतीति से अर्थापत्ति मी है। विद्याधर ने यहाँ प्रतीप माना है। प्रतीप वहाँ होता है, जहाँ उपमान को उपमेय बना दिया जाता है अथवा उपमान का तिरस्कार किया जाता है लेकिन ये दोनों बातें यहाँ हमारे देखने में नहीं आ रही हैं। कवि का व्यक्तिगत संकेत मानने को अवस्था में श्लेष यहाँ होगा ही। शब्दालंकार वृत्त्यनुप्रास है। नलेन मायाश्शशिना निशेव त्वया स मायान्निशया शशीव / पुनःपुनस्तद्युगयुग्विधाता स्वभ्यासमास्ते नु युवां युयुक्षुः / / 117 // अन्धयः-(हे भैमि ) शशिना निशा इव नलेन ( त्वम् ) मायाः; निशया शशी इव त्वया स मायाव / पुनःपुनः तद्-युग-युग विधाता युवाम् युयुक्षः सन् योग्याम् उपास्ते न / टीका-(हे भैमि ) शशिना चन्द्रेष निशा रजनी इव नलेन त्वम् मायाः शोमस्व, निशया रजन्या शशी चन्द्र इव त्वया भैम्या स नलो मायात् शोमताम् , उमयोः समागमे उमावपि परस्परशोमानको भवतामित्यर्थः / पुनःपुनः मुहुर्मुहुः तयोः शशि निशयोः युगं युगलम् (10 तत्पु०) युनक्ति सम्बनातीति तथोक्तः ( उपपद तत्पु० ) विधाता ब्रह्मा युवा नलं स्वच्चेति युयुक्षुः योक्तुमिच्छु: सन् अभ्यासम् योग्याम् ('योग्याभ्यासार्कयोषितोः' इति विश्वः) उपास्ते करोति नु किम् ? कस्याप्युत्कृष्टवस्तु-निर्मापार्थम् पूर्वाभ्यासं कुर्वन् कलाकार इव ब्रह्मापि युवयोः समागमार्थ पुनःपुनः शशिनिशासमागमनिर्माणरूपेण पूर्वाभ्यासं करोतोति मावः // 117 // व्याकरण-भायाः भा+आशोलिंङ् मध्यपु० / युनाम् नलं त्वां चेति एकशेष ('त्यदादीनां मिथः सहोलौ यत् परं तच्छिष्यते / ) ०युक युज्+विप् ( कर्तरि ) / युयुक्षुः योक्तुमिच्छुरिति युज्+सन्+3, 'न लोका०' (2 / 3 / 69 ) से षष्ठी-निषेध। अनवाद-(हे भैमी ! ) जिस तरह चन्द्र से निशा की शोमा होती है, उसी तरह नल से तुम्हारी शोमा होवे ( तथा ) जिस तरह निशा से चन्द्र शोमित होता है, उसी तरह तुमसे वह (नल ) शोभित होवे। ऐसा लगता है कि बार-बार उस ( शशि-निशा के ) युगल का संयोग करने वाला विधाता मानो तुम दोनों का संयोग करना चाहता हुमा पूर्वाभ्यास कर रहा हो। 117 / / टिप्पणी-यहाँ 'निशेव' शशीव' में दो उपमाय है; अन्योन्य के शोमा-जनक होने से अन्योन्यालंकार है; आशीर्वाद होने से आशीरलंकार है; नु शब्द के उत्प्रेक्षा-वाचक होने से उत्प्रेक्षा भी है, इस तरह इन सभी का सांकयं है। शब्दालंकारों में से 'भायाः' 'भायात्', 'शशि' 'शशी' 'निशे' 'निश', 'युग' 'युग' में छेक और अन्यत्र वृत्यनुप्रास है।