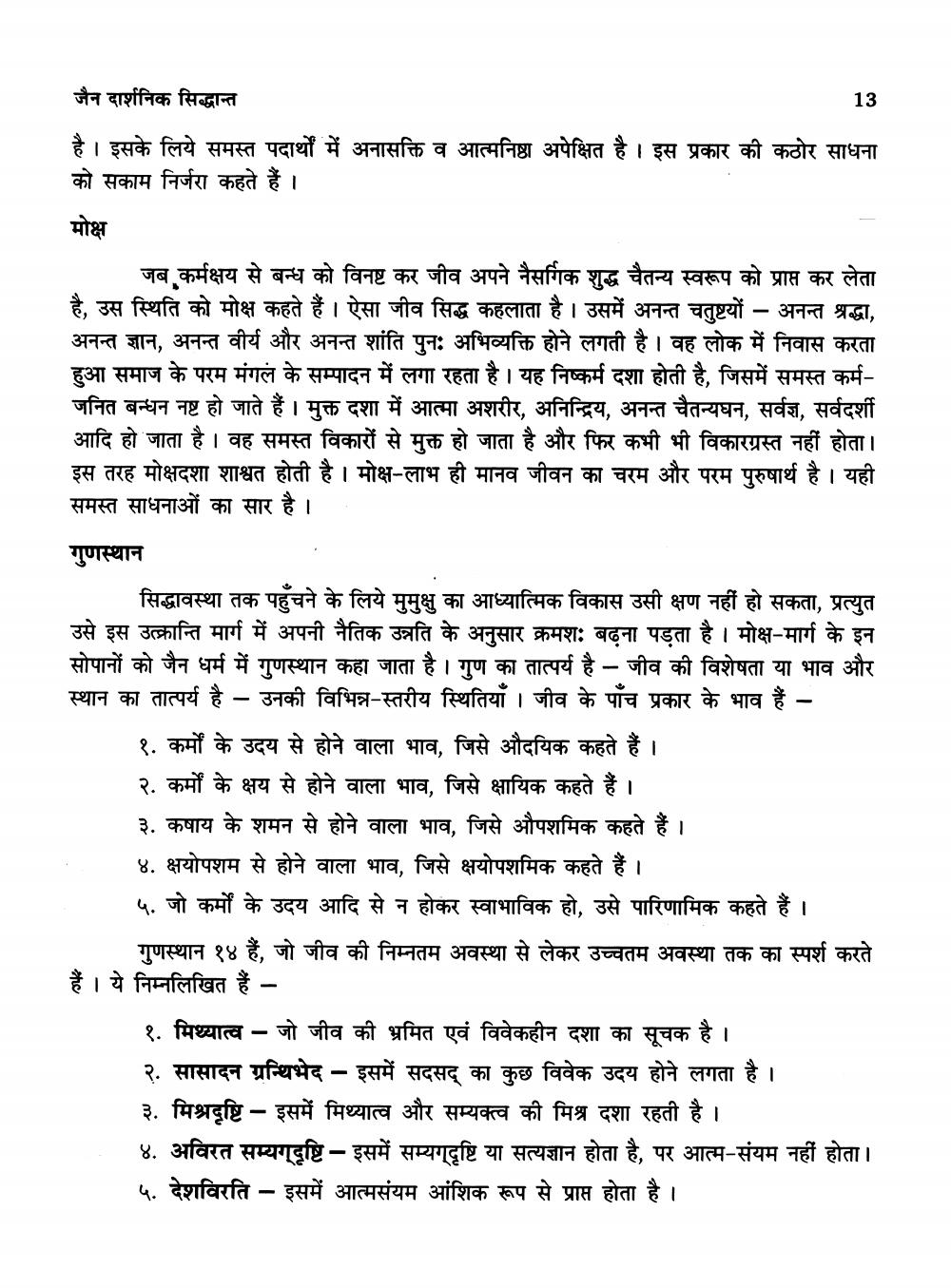________________ 13 जैन दार्शनिक सिद्धान्त है। इसके लिये समस्त पदार्थों में अनासक्ति व आत्मनिष्ठा अपेक्षित है। इस प्रकार की कठोर साधना को सकाम निर्जरा कहते हैं / मोक्ष जब कर्मक्षय से बन्ध को विनष्ट कर जीव अपने नैसर्गिक शुद्ध चैतन्य स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, उस स्थिति को मोक्ष कहते हैं / ऐसा जीव सिद्ध कहलाता है। उसमें अनन्त चतुष्टयों - अनन्त श्रद्धा, अनन्त ज्ञान, अनन्त वीर्य और अनन्त शांति पुनः अभिव्यक्ति होने लगती है। वह लोक में निवास करता हुआ समाज के परम मंगलं के सम्पादन में लगा रहता है। यह निष्कर्म दशा होती है, जिसमें समस्त कर्मजनित बन्धन नष्ट हो जाते हैं / मुक्त दशा में आत्मा अशरीर, अनिन्द्रिय, अनन्त चैतन्यघन, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी आदि हो जाता है / वह समस्त विकारों से मुक्त हो जाता है और फिर कभी भी विकारग्रस्त नहीं होता। इस तरह मोक्षदशा शाश्वत होती है / मोक्ष-लाभ ही मानव जीवन का चरम और परम पुरुषार्थ है / यही समस्त साधनाओं का सार है। गुणस्थान सिद्धावस्था तक पहुँचने के लिये मुमुक्षु का आध्यात्मिक विकास उसी क्षण नहीं हो सकता, प्रत्युत उसे इस उत्क्रान्ति मार्ग में अपनी नैतिक उन्नति के अनुसार क्रमशः बढ़ना पड़ता है / मोक्ष-मार्ग के इन सोपानों को जैन धर्म में गुणस्थान कहा जाता है। गुण का तात्पर्य है - जीव की विशेषता या भाव और स्थान का तात्पर्य है - उनकी विभिन्न-स्तरीय स्थितियाँ / जीव के पाँच प्रकार के भाव हैं - 1. कर्मों के उदय से होने वाला भाव, जिसे औदयिक कहते हैं / 2. कर्मों के क्षय से होने वाला भाव, जिसे क्षायिक कहते हैं / 3. कषाय के शमन से होने वाला भाव, जिसे औपशमिक कहते हैं / 4. क्षयोपशम से होने वाला भाव, जिसे क्षयोपशमिक कहते हैं / 5. जो कर्मों के उदय आदि से न होकर स्वाभाविक हो, उसे पारिणामिक कहते हैं / गुणस्थान 14 हैं, जो जीव की निम्नतम अवस्था से लेकर उच्चतम अवस्था तक का स्पर्श करते हैं / ये निम्नलिखित हैं - 1. मिथ्यात्व - जो जीव की भ्रमित एवं विवेकहीन दशा का सूचक है। 2. सासादन ग्रन्थिभेद - इसमें सदसद् का कुछ विवेक उदय होने लगता है / 3. मिश्रदृष्टि - इसमें मिथ्यात्व और सम्यक्त्व की मिश्र दशा रहती है / 4. अविरत सम्यग्दृष्टि - इसमें सम्यग्दृष्टि या सत्यज्ञान होता है, पर आत्म-संयम नहीं होता। 5. देशविरति - इसमें आत्मसंयम आंशिक रूप से प्राप्त होता है /