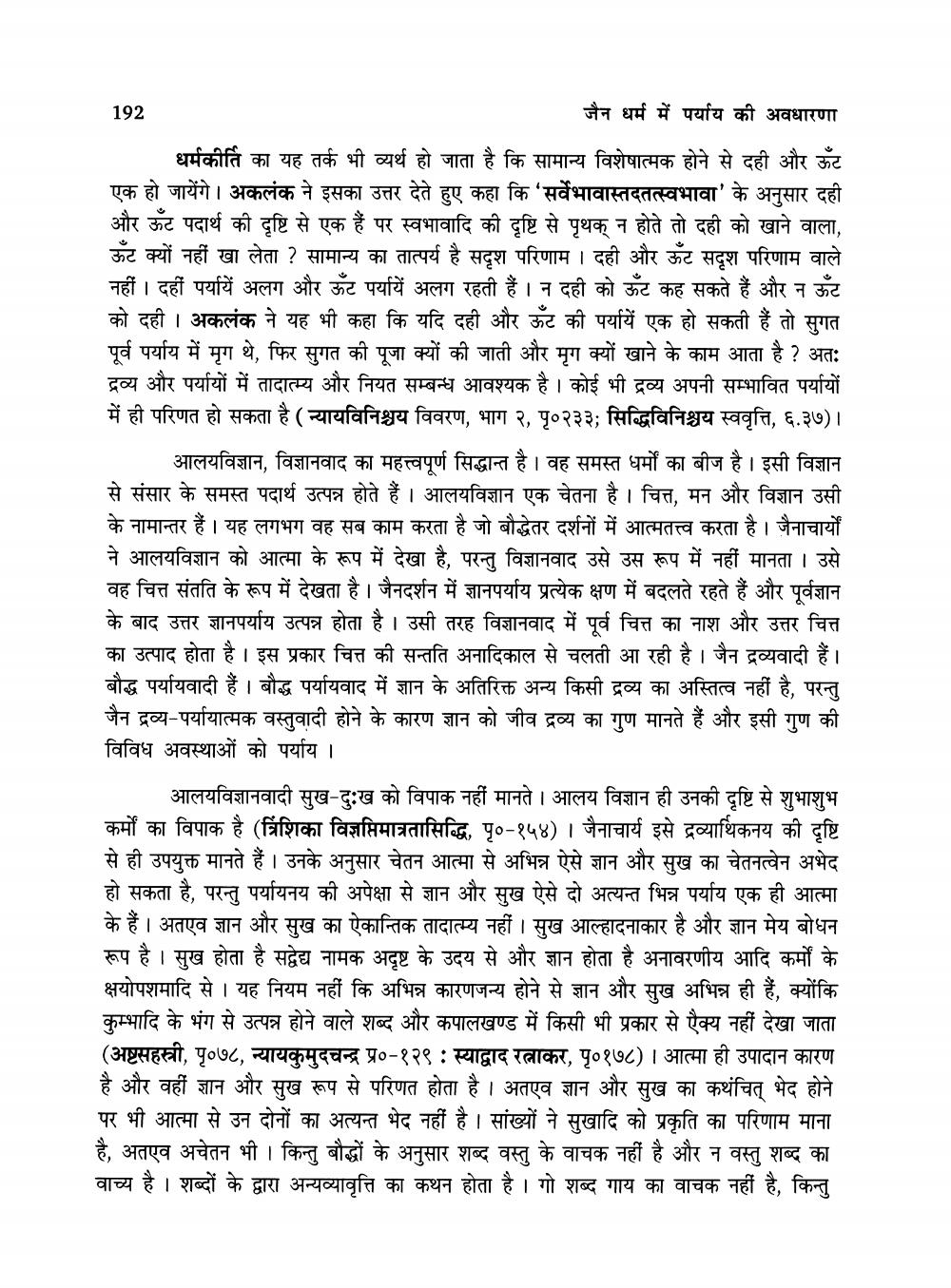________________ 192 जैन धर्म में पर्याय की अवधारणा धर्मकीर्ति का यह तर्क भी व्यर्थ हो जाता है कि सामान्य विशेषात्मक होने से दही और ऊँट एक हो जायेंगे। अकलंक ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि 'सर्वेभावास्तदतत्स्वभावा' के अनुसार दही और ऊँट पदार्थ की दृष्टि से एक हैं पर स्वभावादि की दृष्टि से पृथक् न होते तो दही को खाने वाला, ऊँट क्यों नहीं खा लेता ? सामान्य का तात्पर्य है सदृश परिणाम / दही और ऊँट सदृश परिणाम वाले नहीं / दही पर्यायें अलग और ऊँट पर्यायें अलग रहती हैं / न दही को ऊँट कह सकते हैं और न ऊँट को दही / अकलंक ने यह भी कहा कि यदि दही और ऊँट की पर्यायें एक हो सकती हैं तो सुगत पूर्व पर्याय में मृग थे, फिर सुगत की पूजा क्यों की जाती और मृग क्यों खाने के काम आता है ? अतः द्रव्य और पर्यायों में तादात्म्य और नियत सम्बन्ध आवश्यक है। कोई भी द्रव्य अपनी सम्भावित पर्यायों में ही परिणत हो सकता है (न्यायविनिश्चय विवरण, भाग 2, पृ०२३३; सिद्धिविनिश्चय स्ववृत्ति, 6.37) / आलयविज्ञान, विज्ञानवाद का महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है / वह समस्त धर्मों का बीज है। इसी विज्ञान से संसार के समस्त पदार्थ उत्पन्न होते हैं / आलयविज्ञान एक चेतना है / चित्त, मन और विज्ञान उसी के नामान्तर हैं / यह लगभग वह सब काम करता है जो बौद्धेतर दर्शनों में आत्मतत्त्व करता है। जैनाचार्यों ने आलयविज्ञान को आत्मा के रूप में देखा है, परन्तु विज्ञानवाद उसे उस रूप में नहीं मानता / उसे वह चित्त संतति के रूप में देखता है / जैनदर्शन में ज्ञानपर्याय प्रत्येक क्षण में बदलते रहते हैं और पूर्वज्ञान के बाद उत्तर ज्ञानपर्याय उत्पन्न होता है। उसी तरह विज्ञानवाद में पूर्व चित्त का नाश और उत्तर चित्त का उत्पाद होता है / इस प्रकार चित्त की सन्तति अनादिकाल से चलती आ रही है / जैन द्रव्यवादी हैं। बौद्ध पर्यायवादी हैं / बौद्ध पर्यायवाद में ज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी द्रव्य का अस्तित्व नहीं है, परन्तु जैन द्रव्य-पर्यायात्मक वस्तुवादी होने के कारण ज्ञान को जीव द्रव्य का गुण मानते हैं और इसी गुण की विविध अवस्थाओं को पर्याय / आलयविज्ञानवादी सुख-दुःख को विपाक नहीं मानते / आलय विज्ञान ही उनकी दृष्टि से शुभाशुभ कर्मों का विपाक है (त्रिंशिका विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि, पृ०-१५४) / जैनाचार्य इसे द्रव्यार्थिकनय की दृष्टि से ही उपयुक्त मानते हैं। उनके अनुसार चेतन आत्मा से अभिन्न ऐसे ज्ञान और सुख का चेतनत्वेन अभेद हो सकता है, परन्तु पर्यायनय की अपेक्षा से ज्ञान और सुख ऐसे दो अत्यन्त भिन्न पर्याय एक ही आत्मा के हैं / अतएव ज्ञान और सुख का ऐकान्तिक तादात्म्य नहीं / सुख आल्हादनाकार है और ज्ञान मेय बोधन रूप है / सुख होता है सवैद्य नामक अदृष्ट के उदय से और ज्ञान होता है अनावरणीय आदि कर्मों के क्षयोपशमादि से / यह नियम नहीं कि अभिन्न कारणजन्य होने से ज्ञान और सुख अभिन्न ही हैं, क्योंकि कुम्भादि के भंग से उत्पन्न होने वाले शब्द और कपालखण्ड में किसी भी प्रकार से ऐक्य नहीं देखा जाता (अष्टसहस्त्री, पृ०७८, न्यायकुमुदचन्द्र प्र०-१२९ : स्याद्वाद रत्नाकर, पृ०१७८) / आत्मा ही उपादान कारण है और वहीं ज्ञान और सख रूप से परिणत होता है। अतएव ज्ञान और सख का कथंचित भेद / पर भी आत्मा से उन दोनों का अत्यन्त भेद नहीं है / सांख्यों ने सुखादि को प्रकृति का परिणाम माना है, अतएव अचेतन भी / किन्तु बौद्धों के अनुसार शब्द वस्तु के वाचक नहीं है और न वस्तु शब्द का वाच्य है / शब्दों के द्वारा अन्यव्यावृत्ति का कथन होता है / गो शब्द गाय का वाचक नहीं है, किन्तु