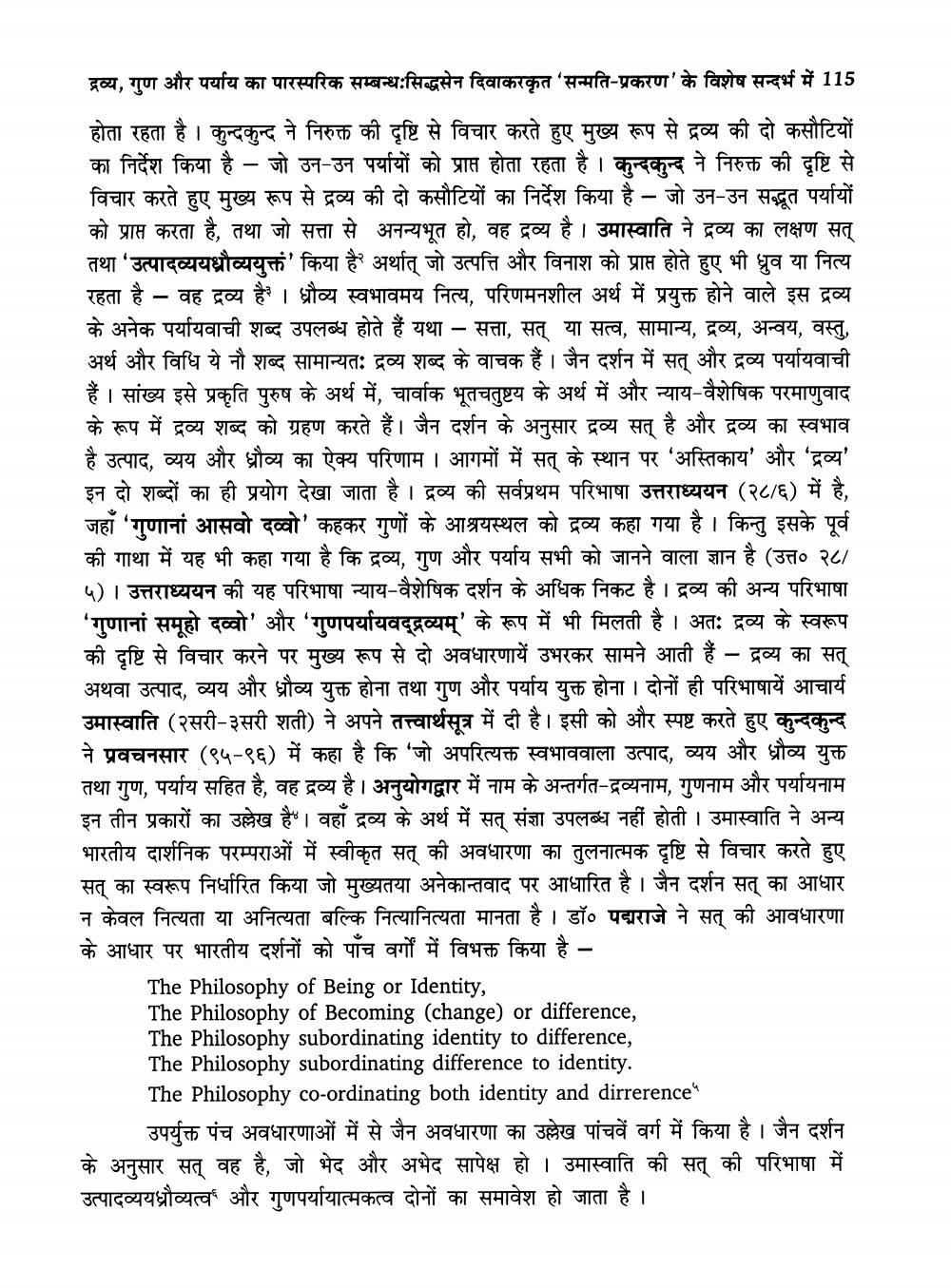________________ द्रव्य, गुण और पर्याय का पारस्परिक सम्बन्धःसिद्धसेन दिवाकरकृत 'सन्मति-प्रकरण' के विशेष सन्दर्भ में 115 होता रहता है / कुन्दकुन्द ने निरुक्त की दृष्टि से विचार करते हुए मुख्य रूप से द्रव्य की दो कसौटियों का निर्देश किया है - जो उन-उन पर्यायों को प्राप्त होता रहता है / कुन्दकुन्द ने निरुक्त की दृष्टि से विचार करते हुए मुख्य रूप से द्रव्य की दो कसौटियों का निर्देश किया है - जो उन-उन सद्भूत पर्यायों तथा 'उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं' किया है। अर्थात् जो उत्पत्ति और विनाश को प्राप्त होते हुए भी ध्रुव या नित्य रहता है - वह द्रव्य है / ध्रौव्य स्वभावमय नित्य, परिणमनशील अर्थ में प्रयुक्त होने वाले इस द्रव्य के अनेक पर्यायवाची शब्द उपलब्ध होते हैं यथा - सत्ता, सत् या सत्व, सामान्य, द्रव्य, अन्वय, वस्तु, अर्थ और विधि ये नौ शब्द सामान्यतः द्रव्य शब्द के वाचक हैं / जैन दर्शन में सत् और द्रव्य पर्यायवाची हैं / सांख्य इसे प्रकृति पुरुष के अर्थ में, चार्वाक भूतचतुष्टय के अर्थ में और न्याय-वैशेषिक परमाणुवाद के रूप में द्रव्य शब्द को ग्रहण करते हैं। जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य सत् है और द्रव्य का स्वभाव है उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य का ऐक्य परिणाम / आगमों में सत् के स्थान पर 'अस्तिकाय' और 'द्रव्य' इन दो शब्दों का ही प्रयोग देखा जाता है / द्रव्य की सर्वप्रथम परिभाषा उत्तराध्ययन (28/6) में है, जहाँ 'गुणानां आसवो दव्वो' कहकर गुणों के आश्रयस्थल को द्रव्य कहा गया है। किन्तु इसके पूर्व की गाथा में यह भी कहा गया है कि द्रव्य, गुण और पर्याय सभी को जानने वाला ज्ञान है (उत्त० 28/ 5) / उत्तराध्ययन की यह परिभाषा न्याय-वैशेषिक दर्शन के अधिक निकट है / द्रव्य की अन्य परिभाषा 'गुणानां समूहो दव्वो' और 'गुणपर्यायवद्रव्यम्' के रूप में भी मिलती है / अतः द्रव्य के स्वरूप की दृष्टि से विचार करने पर मुख्य रूप से दो अवधारणायें उभरकर सामने आती हैं - द्रव्य का सत् अथवा उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य युक्त होना तथा गुण और पर्याय युक्त होना / दोनों ही परिभाषायें आचार्य उमास्वाति (२सरी-३सरी शती) ने अपने तत्त्वार्थसूत्र में दी है। इसी को और स्पष्ट करते हुए कुन्दकुन्द ने प्रवचनसार (95-96) में कहा है कि 'जो अपरित्यक्त स्वभाववाला उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य युक्त तथा गुण, पर्याय सहित है, वह द्रव्य है। अनुयोगद्वार में नाम के अन्तर्गत-द्रव्यनाम, गुणनाम और पर्यायनाम इन तीन प्रकारों का उल्लेख है। वहाँ द्रव्य के अर्थ में सत् संज्ञा उपलब्ध नहीं होती / उमास्वाति ने अन्य भारतीय दार्शनिक परम्पराओं में स्वीकृत सत् की अवधारणा का तुलनात्मक दृष्टि से विचार करते हुए सत् का स्वरूप निर्धारित किया जो मुख्यतया अनेकान्तवाद पर आधारित है / जैन दर्शन सत् का आधार न केवल नित्यता या अनित्यता बल्कि नित्यानित्यता मानता है / डॉ० पद्मराजे ने सत् की आवधारणा के आधार पर भारतीय दर्शनों को पाँच वर्गों में विभक्त किया है - The Philosophy of Being or Identity, The Philosophy of Becoming (change) or difference, The Philosophy subordinating identity to difference, The Philosophy subordinating difference to identity. The Philosophy co-ordinating both identity and dirrerence उपर्युक्त पंच अवधारणाओं में से जैन अवधारणा का उल्लेख पांचवें वर्ग में किया है / जैन दर्शन के अनुसार सत् वह है, जो भेद और अभेद सापेक्ष हो / उमास्वाति की सत् की परिभाषा में उत्पादव्ययध्रौव्यत्व और गुणपर्यायात्मकत्व दोनों का समावेश हो जाता है।