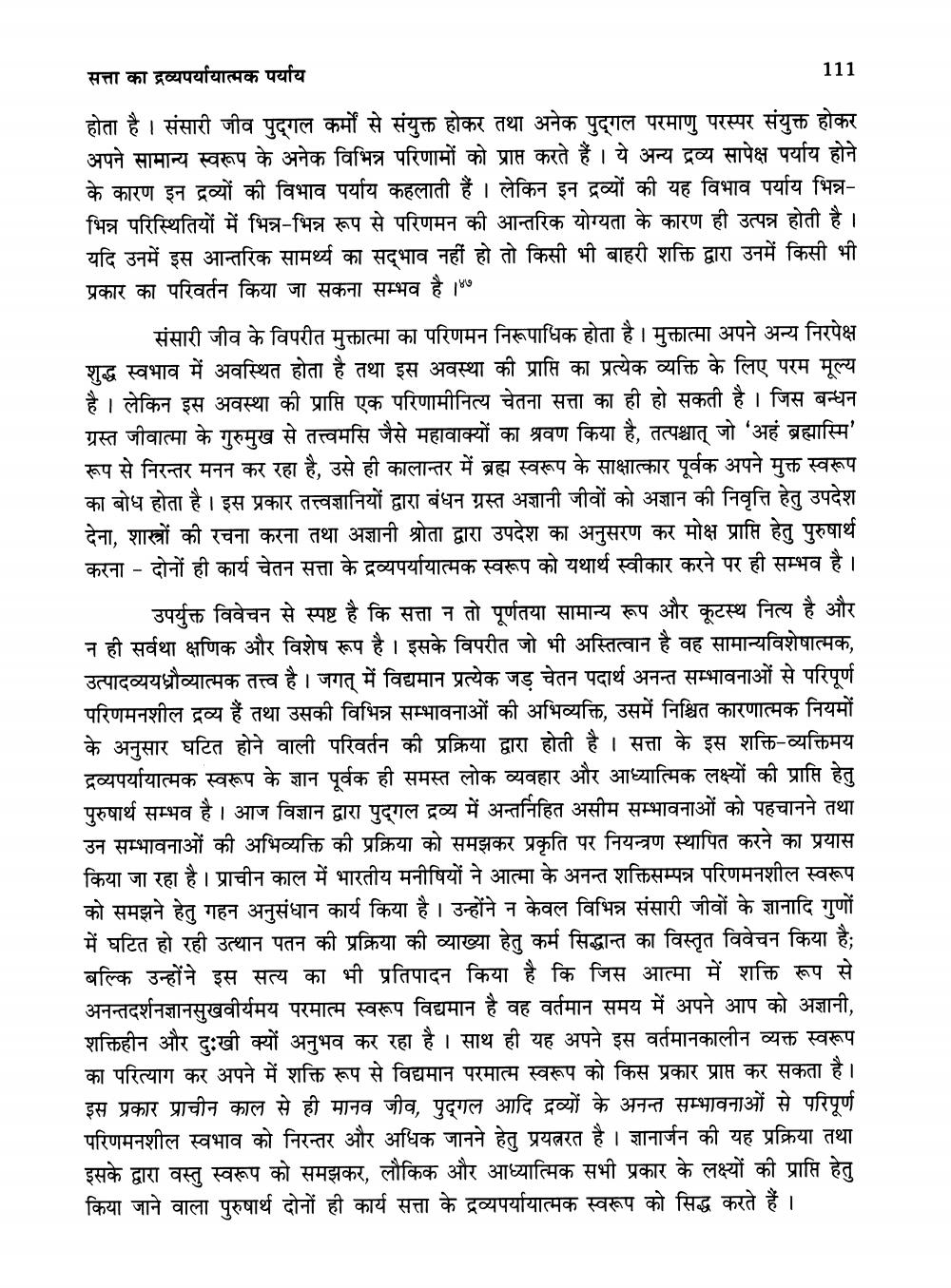________________ 111 सत्ता का द्रव्यपर्यायात्मक पर्याय होता है / संसारी जीव पुद्गल कर्मों से संयुक्त होकर तथा अनेक पुद्गल परमाणु परस्पर संयुक्त होकर अपने सामान्य स्वरूप के अनेक विभिन्न परिणामों को प्राप्त करते हैं / ये अन्य द्रव्य सापेक्ष पर्याय होने के कारण इन द्रव्यों की विभाव पर्याय कहलाती हैं / लेकिन इन द्रव्यों की यह विभाव पर्याय भिन्नभिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न रूप से परिणमन की आन्तरिक योग्यता के कारण ही उत्पन्न होती है / यदि उनमें इस आन्तरिक सामर्थ्य का सद्भाव नहीं हो तो किसी भी बाहरी शक्ति द्वारा उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकना सम्भव है / 40 संसारी जीव के विपरीत मुक्तात्मा का परिणमन निरूपाधिक होता है / मुक्तात्मा अपने अन्य निरपेक्ष शुद्ध स्वभाव में अवस्थित होता है तथा इस अवस्था की प्राप्ति का प्रत्येक व्यक्ति के लिए परम मूल्य है / लेकिन इस अवस्था की प्राप्ति एक परिणामीनित्य चेतना सत्ता का ही हो सकती है। जिस बन्धन ग्रस्त जीवात्मा के गुरुमुख से तत्त्वमसि जैसे महावाक्यों का श्रवण किया है, तत्पश्चात् जो 'अहं ब्रह्मास्मि' रूप से निरन्तर मनन कर रहा है, उसे ही कालान्तर में ब्रह्म स्वरूप के साक्षात्कार पूर्वक अपने मुक्त स्वरूप का बोध होता है / इस प्रकार तत्त्वज्ञानियों द्वारा बंधन ग्रस्त अज्ञानी जीवों को अज्ञान की निवृत्ति हेतु उपदेश देना, शास्त्रों की रचना करना तथा अज्ञानी श्रोता द्वारा उपदेश का अनुसरण कर मोक्ष प्राप्ति हेतु पुरुषार्थ करना - दोनों ही कार्य चेतन सत्ता के द्रव्यपर्यायात्मक स्वरूप को यथार्थ स्वीकार करने पर ही सम्भव है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सत्ता न तो पूर्णतया सामान्य रूप और कूटस्थ नित्य है और न ही सर्वथा क्षणिक और विशेष रूप है / इसके विपरीत जो भी अस्तित्वान है वह सामान्यविशेषात्मक, उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक तत्त्व है। जगत् में विद्यमान प्रत्येक जड़ चेतन पदार्थ अनन्त सम्भावनाओं से परिपूर्ण परिणमनशील द्रव्य हैं तथा उसकी विभिन्न सम्भावनाओं की अभिव्यक्ति, उसमें निश्चित कारणात्मक नियमों के अनुसार घटित होने वाली परिवर्तन की प्रक्रिया द्वारा होती है / सत्ता के इस शक्ति-व्यक्तिमय द्रव्यपर्यायात्मक स्वरूप के ज्ञान पूर्वक ही समस्त लोक व्यवहार और आध्यात्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पुरुषार्थ सम्भव है। आज विज्ञान द्वारा पुद्गल द्रव्य में अन्तर्निहित असीम सम्भावनाओं को पहचानने तथा उन सम्भावनाओं की अभिव्यक्ति की प्रक्रिया को समझकर प्रकृति पर नियन्त्रण स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्राचीन काल में भारतीय मनीषियों ने आत्मा के अनन्त शक्तिसम्पन्न परिणमनशील स्वरूप को समझने हेतु गहन अनुसंधान कार्य किया है। उन्होंने न केवल विभिन्न संसारी जीवों के ज्ञानादि गुणों में घटित हो रही उत्थान पतन की प्रक्रिया की व्याख्या हेतु कर्म सिद्धान्त का विस्तृत विवेचन किया है; बल्कि उन्होंने इस सत्य का भी प्रतिपादन किया है कि जिस आत्मा में शक्ति रूप से अनन्तदर्शनज्ञानसुखवीर्यमय परमात्म स्वरूप विद्यमान है वह वर्तमान समय में अपने आप को अज्ञानी, शक्तिहीन और दुःखी क्यों अनुभव कर रहा है। साथ ही यह अपने इस वर्तमानकालीन व्यक्त स्वरूप का परित्याग कर अपने में शक्ति रूप से विद्यमान परमात्म स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार प्राचीन काल से ही मानव जीव, पुद्गल आदि द्रव्यों के अनन्त सम्भावनाओं से परिपूर्ण परिणमनशील स्वभाव को निरन्तर और अधिक जानने हेतु प्रयत्नरत है। ज्ञानार्जन की यह प्रक्रिया तथा इसके द्वारा वस्तु स्वरूप को समझकर, लौकिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किया जाने वाला पुरुषार्थ दोनों ही कार्य सत्ता के द्रव्यपर्यायात्मक स्वरूप को सिद्ध करते हैं /