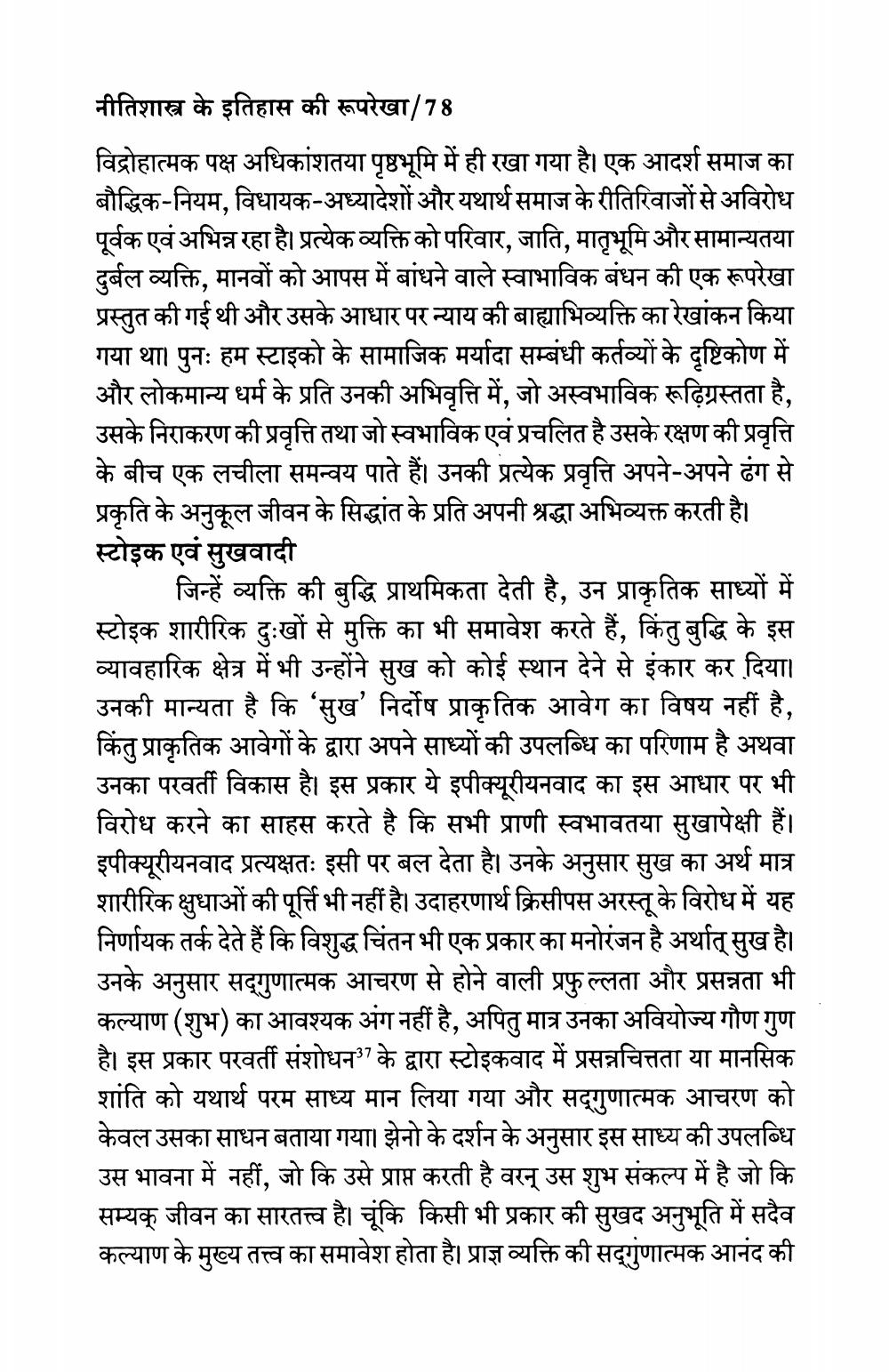________________
नीतिशास्त्र के इतिहास की रूपरेखा/78 विद्रोहात्मक पक्ष अधिकांशतया पृष्ठभूमि में ही रखा गया है। एक आदर्श समाज का बौद्धिक-नियम, विधायक-अध्यादेशों और यथार्थसमाज के रीतिरिवाजों से अविरोध पूर्वक एवं अभिन्न रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को परिवार, जाति, मातृभूमि और सामान्यतया दुर्बल व्यक्ति, मानवों को आपस में बांधने वाले स्वाभाविक बंधन की एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और उसके आधार पर न्याय की बाह्याभिव्यक्ति का रेखांकन किया गया था। पुनः हम स्टाइको के सामाजिक मर्यादा सम्बंधी कर्तव्यों के दृष्टिकोण में
और लोकमान्य धर्म के प्रति उनकी अभिवृत्ति में, जो अस्वभाविक रूढ़िग्रस्तता है, उसके निराकरण की प्रवृत्ति तथा जो स्वभाविक एवं प्रचलित है उसके रक्षण की प्रवृत्ति के बीच एक लचीला समन्वय पाते हैं। उनकी प्रत्येक प्रवृत्ति अपने-अपने ढंग से प्रकृति के अनुकूल जीवन के सिद्धांत के प्रति अपनी श्रद्धा अभिव्यक्त करती है। स्टोइक एवं सुखवादी
जिन्हें व्यक्ति की बुद्धि प्राथमिकता देती है, उन प्राकृतिक साध्यों में स्टोइक शारीरिक दुःखों से मुक्ति का भी समावेश करते हैं, किंतु बुद्धि के इस व्यावहारिक क्षेत्र में भी उन्होंने सुख को कोई स्थान देने से इंकार कर दिया। उनकी मान्यता है कि 'सुख' निर्दोष प्राकृतिक आवेग का विषय नहीं है, किंतु प्राकृतिक आवेगों के द्वारा अपने साध्यों की उपलब्धि का परिणाम है अथवा उनका परवर्ती विकास है। इस प्रकार ये इपीक्यूरीयनवाद का इस आधार पर भी विरोध करने का साहस करते है कि सभी प्राणी स्वभावतया सुखापेक्षी हैं। इपीक्यूरीयनवाद प्रत्यक्षतः इसी पर बल देता है। उनके अनुसार सुख का अर्थ मात्र शारीरिक क्षुधाओं की पूर्ति भी नहीं है। उदाहरणार्थ क्रिसीपस अरस्तू के विरोध में यह निर्णायक तर्क देते हैं कि विशुद्ध चिंतन भी एक प्रकार का मनोरंजन है अर्थात् सुख है। उनके अनुसार सद्गुणात्मक आचरण से होने वाली प्रफुल्लता और प्रसन्नता भी कल्याण (शुभ) का आवश्यक अंग नहीं है, अपितु मात्र उनका अवियोज्य गौण गुण है। इस प्रकार परवर्ती संशोधन के द्वारा स्टोइकवाद में प्रसन्नचित्तता या मानसिक शांति को यथार्थ परम साध्य मान लिया गया और सद्गुणात्मक आचरण को केवल उसका साधन बताया गया। झेनो के दर्शन के अनुसार इस साध्य की उपलब्धि उस भावना में नहीं, जो कि उसे प्राप्त करती है वरन् उस शुभ संकल्प में है जो कि सम्यक् जीवन का सारतत्त्व है। चूंकि किसी भी प्रकार की सुखद अनुभूति में सदैव कल्याण के मुख्य तत्त्व का समावेश होता है। प्राज्ञ व्यक्ति की सद्गुणात्मक आनंद की