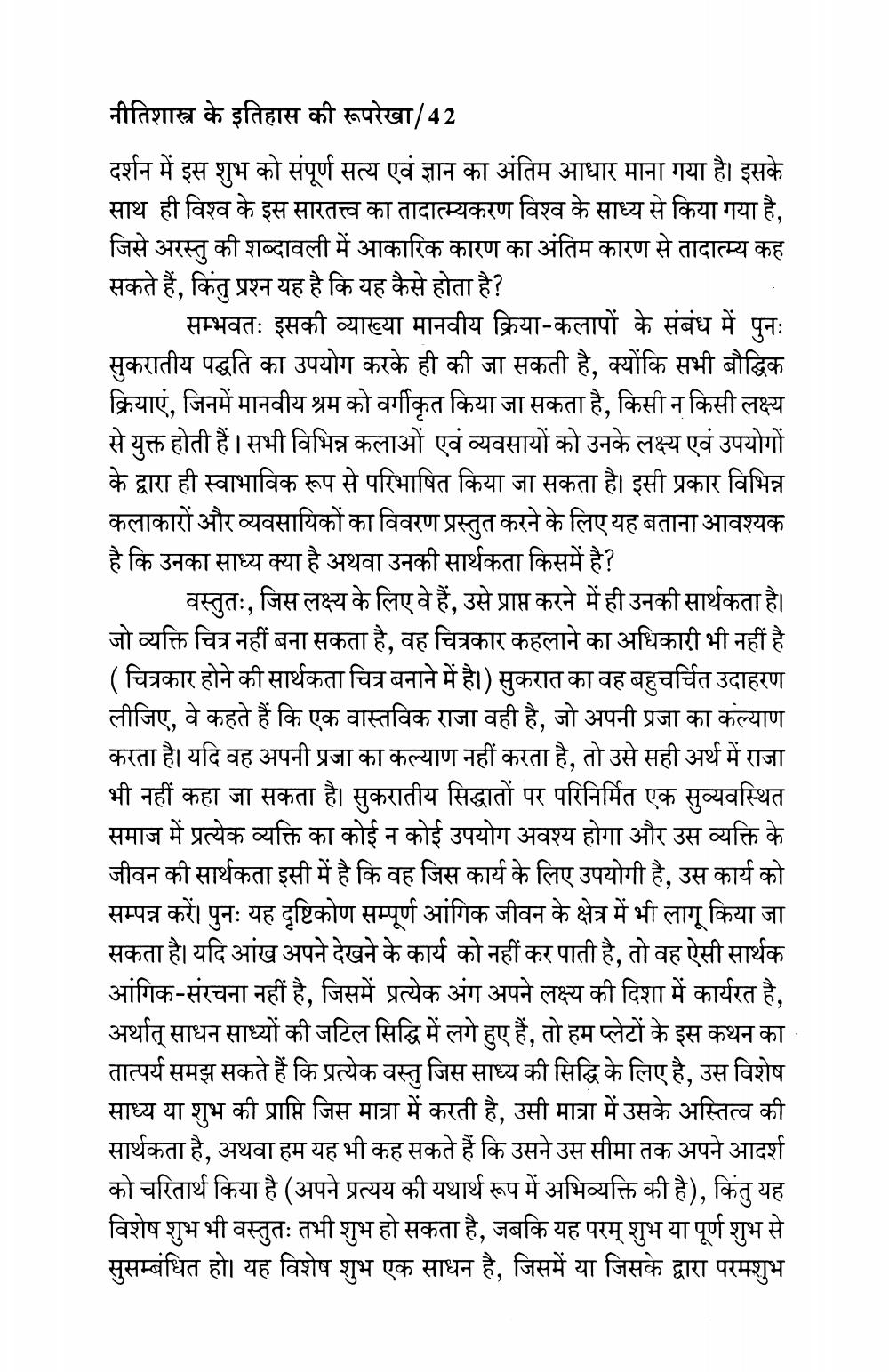________________
नीतिशास्त्र के इतिहास की रूपरेखा/42 दर्शन में इस शुभ को संपूर्ण सत्य एवं ज्ञान का अंतिम आधार माना गया है। इसके साथ ही विश्व के इस सारतत्त्व का तादात्म्यकरण विश्व के साध्य से किया गया है, जिसे अरस्तु की शब्दावली में आकारिक कारण का अंतिम कारण से तादात्म्य कह सकते हैं, किंतु प्रश्न यह है कि यह कैसे होता है?
___ सम्भवतः इसकी व्याख्या मानवीय क्रिया-कलापों के संबंध में पुनः सुकरातीय पद्धति का उपयोग करके ही की जा सकती है, क्योंकि सभी बौद्धिक क्रियाएं, जिनमें मानवीय श्रम को वर्गीकृत किया जा सकता है, किसी न किसी लक्ष्य से युक्त होती हैं। सभी विभिन्न कलाओं एवं व्यवसायों को उनके लक्ष्य एवं उपयोगों के द्वारा ही स्वाभाविक रूप से परिभाषित किया जा सकता है। इसी प्रकार विभिन्न कलाकारों और व्यवसायिकों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए यह बताना आवश्यक है कि उनका साध्य क्या है अथवा उनकी सार्थकता किसमें है?
वस्तुतः, जिस लक्ष्य के लिए वे हैं, उसे प्राप्त करने में ही उनकी सार्थकता है। जो व्यक्ति चित्र नहीं बना सकता है, वह चित्रकार कहलाने का अधिकारी भी नहीं है ( चित्रकार होने की सार्थकता चित्र बनाने में है।) सुकरात का वह बहुचर्चित उदाहरण लीजिए, वे कहते हैं कि एक वास्तविक राजा वही है, जो अपनी प्रजा का कल्याण करता है। यदि वह अपनी प्रजा का कल्याण नहीं करता है, तो उसे सही अर्थ में राजा भी नहीं कहा जा सकता है। सुकरातीय सिद्धातों पर परिनिर्मित एक सुव्यवस्थित समाज में प्रत्येक व्यक्ति का कोई न कोई उपयोग अवश्य होगा और उस व्यक्ति के जीवन की सार्थकता इसी में है कि वह जिस कार्य के लिए उपयोगी है, उस कार्य को सम्पन्न करें। पुनः यह दृष्टिकोण सम्पूर्ण आंगिक जीवन के क्षेत्र में भी लागू किया जा सकता है। यदि आंख अपने देखने के कार्य को नहीं कर पाती है, तो वह ऐसी सार्थक आंगिक-संरचना नहीं है, जिसमें प्रत्येक अंग अपने लक्ष्य की दिशा में कार्यरत है, अर्थात् साधन साध्यों की जटिल सिद्धि में लगे हुए हैं, तो हम प्लेटों के इस कथन का तात्पर्य समझ सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु जिस साध्य की सिद्धि के लिए है, उस विशेष साध्य या शुभ की प्राप्ति जिस मात्रा में करती है, उसी मात्रा में उसके अस्तित्व की सार्थकता है, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि उसने उस सीमा तक अपने आदर्श को चरितार्थ किया है (अपने प्रत्यय की यथार्थ रूप में अभिव्यक्ति की है), किंतु यह विशेष शुभ भी वस्तुतः तभी शुभ हो सकता है, जबकि यह परम् शुभ या पूर्ण शुभ से सुसम्बंधित हो। यह विशेष शुभ एक साधन है, जिसमें या जिसके द्वारा परमशुभ