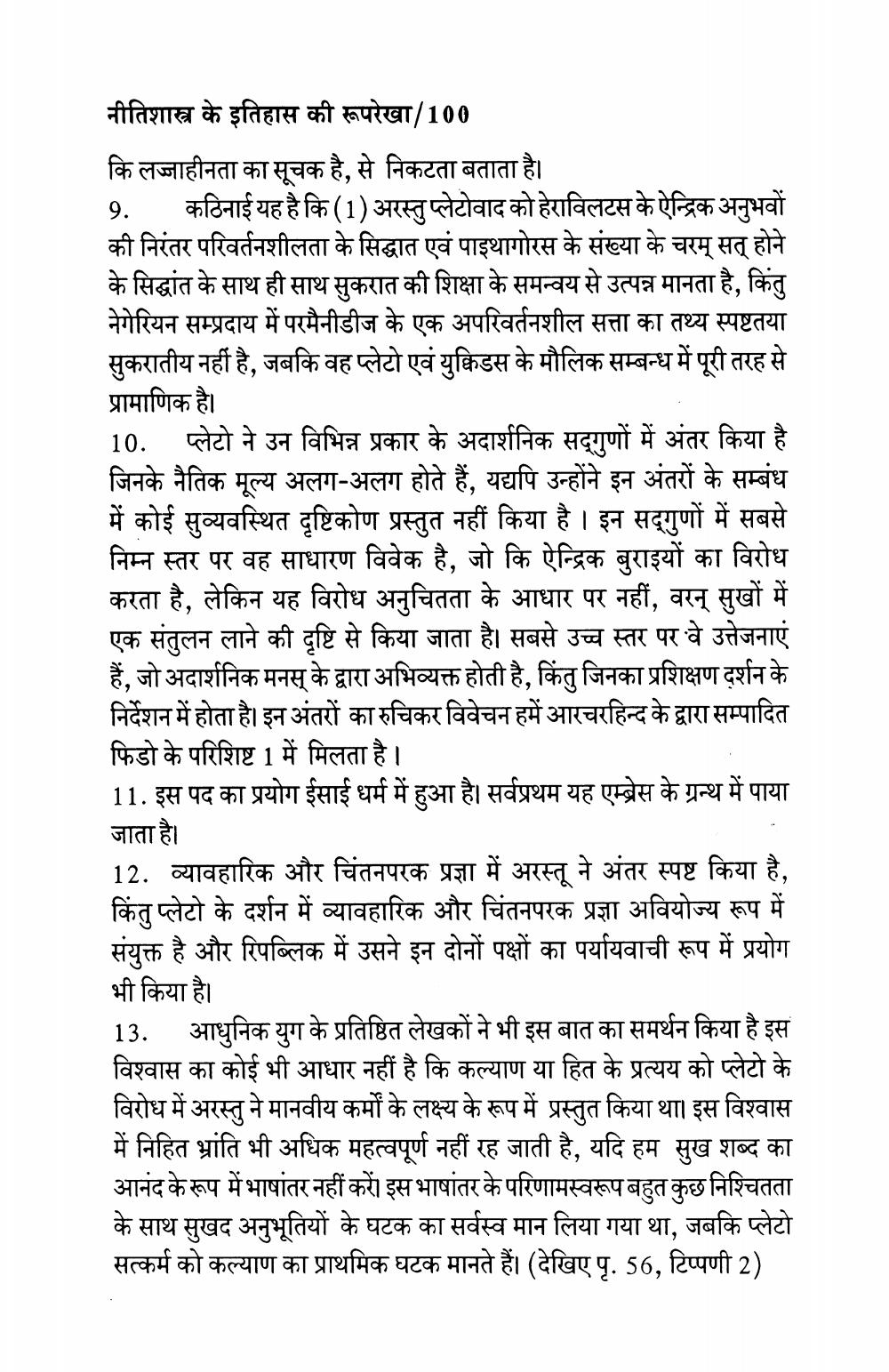________________
नीतिशास्त्र के इतिहास की रूपरेखा/100 कि लज्जाहीनता का सूचक है, से निकटता बताता है। 9. कठिनाई यह है कि (1) अरस्तुप्लेटोवाद को हेराविलटस के ऐन्द्रिक अनुभवों की निरंतर परिवर्तनशीलता के सिद्धात एवं पाइथागोरस के संख्या के चरम् सत् होने के सिद्धांत के साथ ही साथ सुकरात की शिक्षा के समन्वय से उत्पन्न मानता है, किंतु नेगेरियन सम्प्रदाय में परमैनीडीज के एक अपरिवर्तनशील सत्ता का तथ्य स्पष्टतया सुकरातीय नहीं है, जबकि वह प्लेटो एवं युक्विडस के मौलिक सम्बन्ध में पूरी तरह से प्रामाणिक है। 10. प्लेटो ने उन विभिन्न प्रकार के अदार्शनिक सद्गुणों में अंतर किया है जिनके नैतिक मूल्य अलग-अलग होते हैं, यद्यपि उन्होंने इन अंतरों के सम्बंध में कोई सुव्यवस्थित दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं किया है। इन सद्गुणों में सबसे निम्न स्तर पर वह साधारण विवेक है, जो कि ऐन्द्रिक बुराइयों का विरोध करता है, लेकिन यह विरोध अनुचितता के आधार पर नहीं, वरन् सुखों में एक संतुलन लाने की दृष्टि से किया जाता है। सबसे उच्च स्तर पर वे उत्तेजनाएं हैं, जो अदार्शनिक मनस् के द्वारा अभिव्यक्त होती है, किंतु जिनका प्रशिक्षण दर्शन के निर्देशन में होता है। इन अंतरों का रुचिकर विवेचन हमें आरचरहिन्द के द्वारा सम्पादित फिडो के परिशिष्ट 1 में मिलता है। 11. इस पद का प्रयोग ईसाई धर्म में हुआ है। सर्वप्रथम यह एम्ब्रेस के ग्रन्थ में पाया जाता है। 12. व्यावहारिक और चिंतनपरक प्रज्ञा में अरस्तू ने अंतर स्पष्ट किया है, किंतु प्लेटो के दर्शन में व्यावहारिक और चिंतनपरक प्रज्ञा अवियोज्य रूप में संयुक्त है और रिपब्लिक में उसने इन दोनों पक्षों का पर्यायवाची रूप में प्रयोग भी किया है। 13. आधुनिक युग के प्रतिष्ठित लेखकों ने भी इस बात का समर्थन किया है इस विश्वास का कोई भी आधार नहीं है कि कल्याण या हित के प्रत्यय को प्लेटो के विरोध में अरस्तु ने मानवीय कर्मों के लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया था। इस विश्वास में निहित भ्रांति भी अधिक महत्वपूर्ण नहीं रह जाती है, यदि हम सुख शब्द का आनंद के रूप में भाषांतर नहीं करें। इस भाषांतर के परिणामस्वरूप बहुत कुछ निश्चितता के साथ सुखद अनुभूतियों के घटक का सर्वस्व मान लिया गया था, जबकि प्लेटो सत्कर्म को कल्याण का प्राथमिक घटक मानते हैं। (देखिए पृ. 56, टिप्पणी 2)