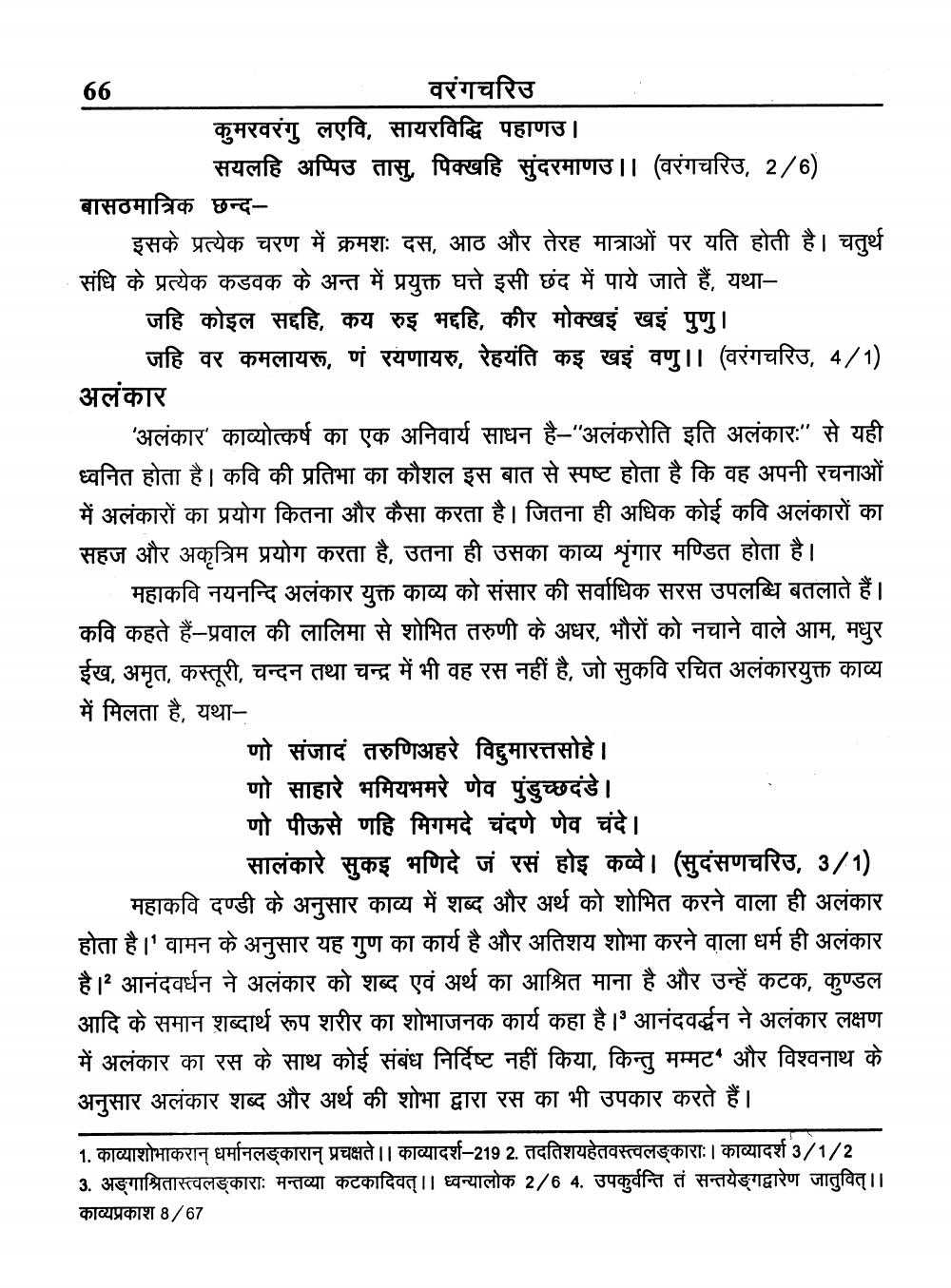________________
66
वरंगचरिउ
कुमरवरंगु लएवि, सायरविद्धि पहाणउ ।
सयलहि अप्पिउ तासु, पिक्खहि सुंदरमाणउ ।। (वरंगचरिउ, 2/6)
बासठमात्रिक छन्द
इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः दस, आठ और तेरह मात्राओं पर यति होती है। चतुर्थ संधि के प्रत्येक कडवक के अन्त में प्रयुक्त घत्ते इसी छंद में पाये जाते हैं, यथा
जहि कोइल सद्दहि, कय रुइ भद्दहि, कीर मोक्खइं खरं पुणु ।
जहि वर कमलायरू, णं रयणायरु, रेहयंति कइ खइं वणु ।। (वरंगचरिउ, 4 / 1) अलंकार
'अलंकार' काव्योत्कर्ष का एक अनिवार्य साधन है - "अलंकरोति इति अलंकार:" से यही ध्वनित होता है । कवि की प्रतिभा का कौशल इस बात से स्पष्ट होता है कि वह अपनी रचनाओं में अलंकारों का प्रयोग कितना और कैसा करता है। जितना ही अधिक कोई कवि अलंकारों का सहज और अकृत्रिम प्रयोग करता है, उतना ही उसका काव्य शृंगार मण्डित होता है ।
महाकवि नयनन्दि अलंकार युक्त काव्य को संसार की सर्वाधिक सरस उपलब्धि बतलाते हैं । कवि कहते हैं-प्रवाल की लालिमा से शोभित तरुणी के अधर, भौरों को नचाने वाले आम, मधुर ईख, अमृत, कस्तूरी, चन्दन तथा चन्द्र में भी वह रस नहीं है, जो सुकवि रचित अलंकारयुक्त काव्य में मिलता है, यथा-
णो संजादं तरुणिअहरे विद्दुमारत्तसोहे । णो साहारे भमियभमरे णेव पुंडुच्छदंडे |
णो पीऊसे णहि मिगमदे चंदणे णेव चंदे |
सालंकारे सुकइ भणिदे जं रसं होइ कव्वे । (सुदंसणचरिउ, 3 / 1 )
महाकवि दण्डी के अनुसार काव्य में शब्द और अर्थ को शोभित करने वाला ही अलंकार होता है।' वामन के अनुसार यह गुण का कार्य है और अतिशय शोभा करने वाला धर्म ही अलंकार है।± आनंदवर्धन ने अलंकार को शब्द एवं अर्थ का आश्रित माना है और उन्हें कटक, कुण्डल आदि के समान शब्दार्थ रूप शरीर का शोभाजनक कार्य कहा है। आनंदवर्द्धन ने अलंकार लक्षण में अलंकार का रस के साथ कोई संबंध निर्दिष्ट नहीं किया, किन्तु मम्मट' और विश्वनाथ के अनुसार अलंकार शब्द और अर्थ की शोभा द्वारा रस का भी उपकार करते हैं।
1. काव्याशोभाकरान् धर्मानलङ्कारान् प्रचक्षते ।। काव्यादर्श - 219 2. तदतिशयहेतवस्त्वलङ्काराः । काव्यादर्श 3/1/2 3. अङ्गाश्रितास्त्वलङ्काराः मन्तव्या कटकादिवत् । । ध्वन्यालोक 2 / 6 4 उपकुर्वन्ति तं सन्तयेङ्गद्वारेण जातुवित् ।।
काव्यप्रकाश 8 / 67