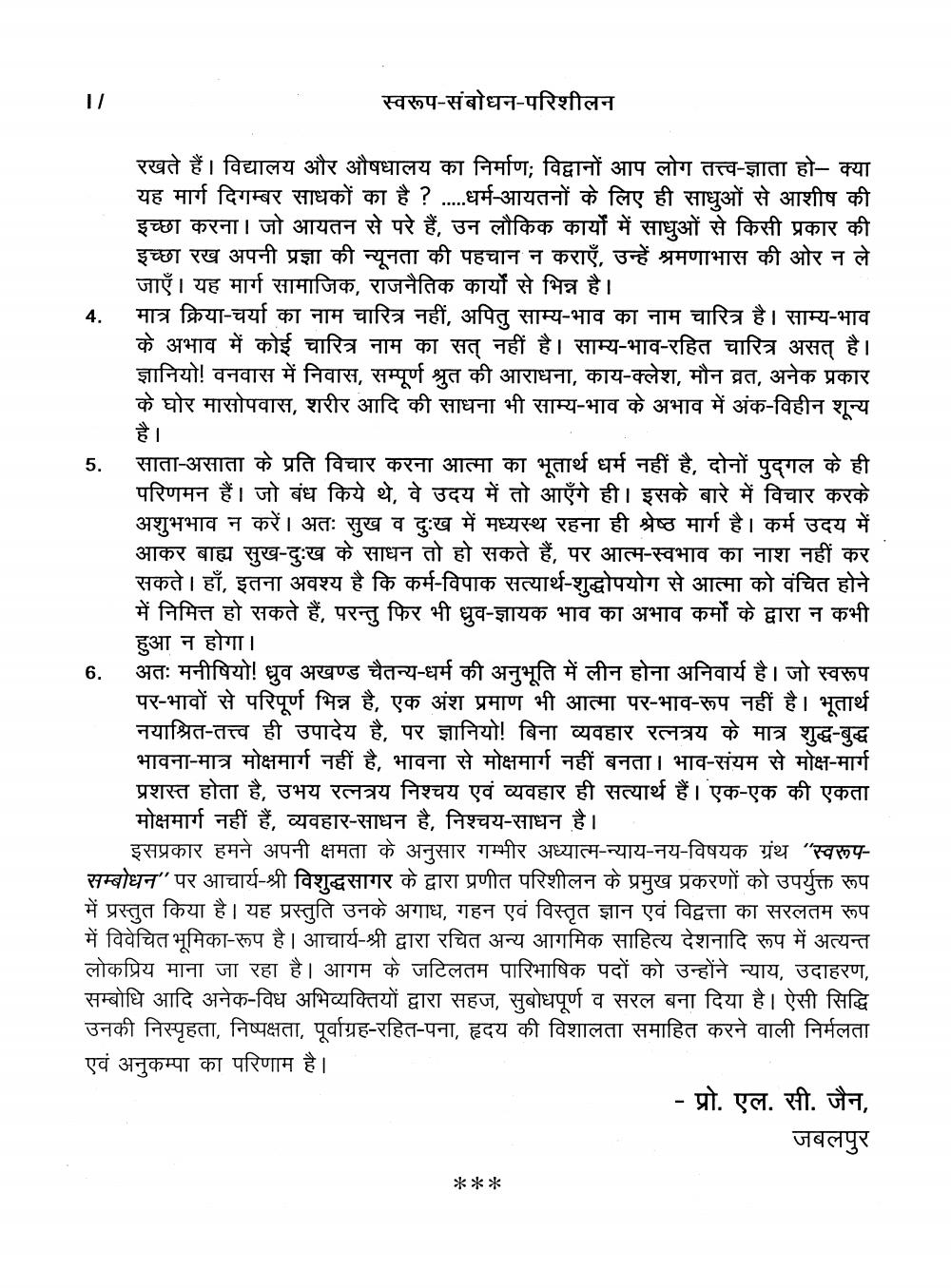________________
1/
4.
5.
6.
स्वरूप-संबोधन-परिशीलन
रखते हैं। विद्यालय और औषधालय का निर्माण; विद्वानों आप लोग तत्त्व - ज्ञाता हो- क्या यह मार्ग दिगम्बर साधकों का है ? .....धर्म - आयतनों के लिए ही साधुओं से आशीष की इच्छा करना। जो आयतन से परे हैं, उन लौकिक कार्यों में साधुओं से किसी प्रकार की इच्छा रख अपनी प्रज्ञा की न्यूनता की पहचान न कराएँ, उन्हें श्रमणाभास की ओर न ले जाएँ। यह मार्ग सामाजिक, राजनैतिक कार्यों से भिन्न है ।
मात्र क्रिया-चर्या का नाम चारित्र नहीं, अपितु साम्य-भाव का नाम चारित्र है । साम्य-भाव के अभाव कोई चारित्र नाम का सत् नहीं है। साम्य-भाव रहित चारित्र असत् है । ज्ञानियो! वनवास में निवास, सम्पूर्ण श्रुत की आराधना, काय-क्लेश, मौन व्रत, अनेक प्रकार के घोर मासोपवास, शरीर आदि की साधना भी साम्य-भाव के अभाव में अंक -विहीन शून्य है ।
साता-असाता के प्रति विचार करना आत्मा का भूतार्थ धर्म नहीं है, दोनों पुद्गल के ही परिणमन हैं । जो बंध किये थे, वे उदय में तो आएँगे ही। इसके बारे में विचार करके अशुभभाव न करें। अतः सुख व दुःख में मध्यस्थ रहना ही श्रेष्ठ मार्ग है। कर्म उदय में आकर बाह्य सुख-दुःख के साधन तो हो सकते हैं, पर आत्म-स्वभाव का नाश नहीं कर सकते। हाँ, इतना अवश्य है कि कर्म विपाक सत्यार्थ- शुद्धोपयोग से आत्मा को वंचित होने में निमित्त हो सकते हैं, परन्तु फिर भी ध्रुव-ज्ञायक भाव का अभाव कर्मों के द्वारा न कभी हुआ न होगा।
अतः मनीषियो! ध्रुव अखण्ड चैतन्य-धर्म की अनुभूति में लीन होना अनिवार्य है। जो स्वरूप पर-भावों से परिपूर्ण भिन्न है, एक अंश प्रमाण भी आत्मा पर - भाव-रूप नहीं है । भूतार्थ नयाश्रित-तत्त्व ही उपादेय है, पर ज्ञानियो ! बिना व्यवहार रत्नत्रय के मात्र शुद्ध - बुद्ध भावना-मात्र मोक्षमार्ग नहीं है, भावना से मोक्षमार्ग नहीं बनता । भाव- संयम से मोक्ष - मार्ग प्रशस्त होता है, उभय रत्नत्रय निश्चय एवं व्यवहार ही सत्यार्थ हैं। एक-एक की एकता मोक्षमार्ग नहीं हैं, व्यवहार - साधन है, निश्चय - साधन है ।
इसप्रकार हमने अपनी क्षमता के अनुसार गम्भीर अध्यात्म - न्याय-नय- विषयक ग्रंथ "स्वरूपसम्बोधन” पर आचार्य श्री विशुद्धसागर के द्वारा प्रणीत परिशीलन के प्रमुख प्रकरणों को उपर्युक्त रूप
प्रस्तुत किया है। यह प्रस्तुति उनके अगाध, गहन एवं विस्तृत ज्ञान एवं विद्वत्ता का सरलतम रूप में विवेचित भूमिका रूप है। आचार्य श्री द्वारा रचित अन्य आगमिक साहित्य देशनादि रूप में अत्यन्त लोकप्रिय माना जा रहा है। आगम के जटिलतम पारिभाषिक पदों को उन्होंने न्याय, उदाहरण, सम्बोधि आदि अनेक-विध अभिव्यक्तियों द्वारा सहज, सुबोधपूर्ण व सरल बना दिया है। ऐसी सिद्धि उनकी निस्पृहता, निष्पक्षता, पूर्वाग्रह - रहित - पना, हृदय की विशालता समाहित करने वाली निर्मलता एवं अनुकम्पा का परिणाम है।
***
- प्रो. एल. सी. जैन,
जबलपुर