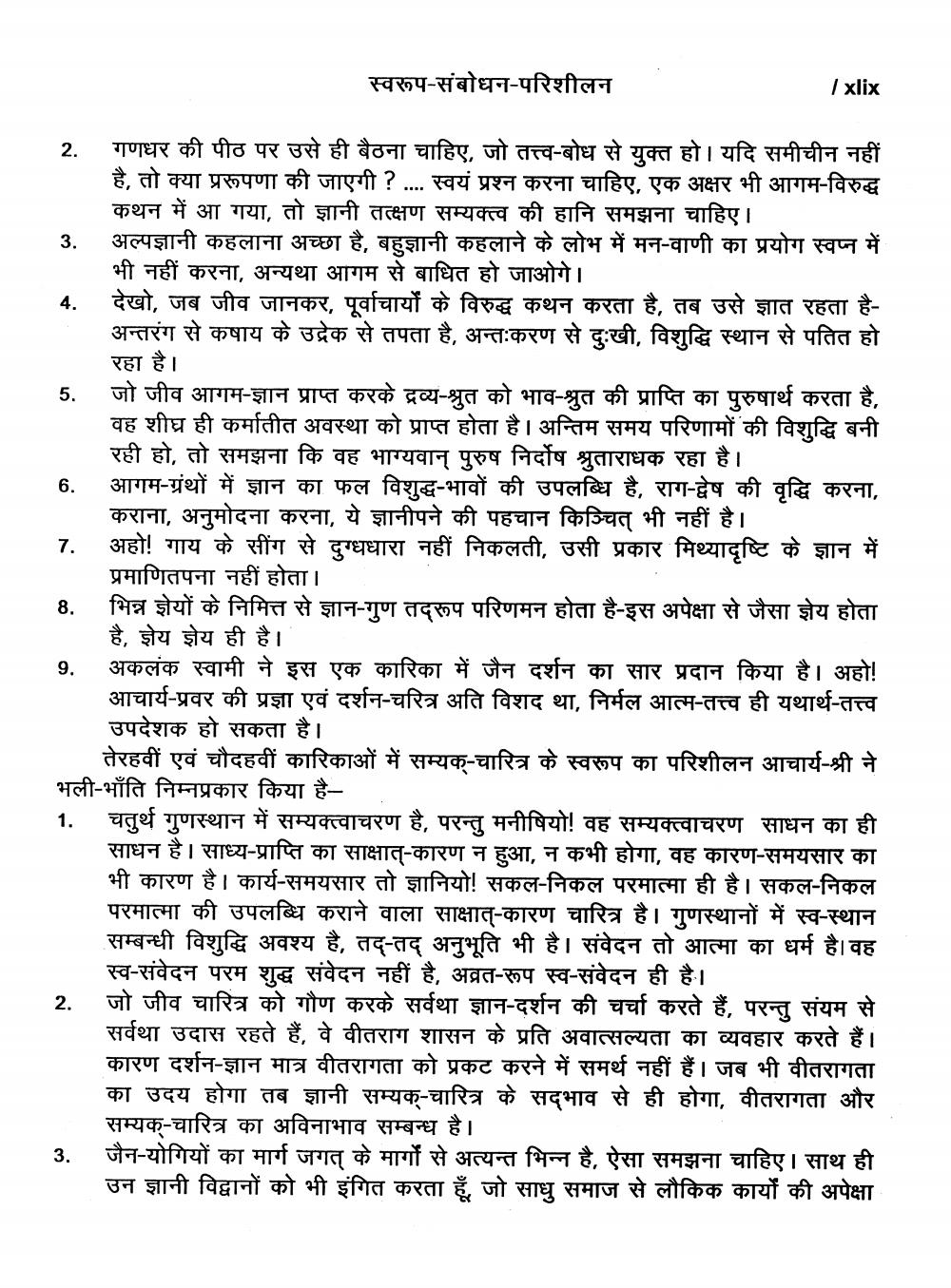________________
स्वरूप-संबोधन-परिशीलन
1 xlix
2. गणधर की पीठ पर उसे ही बैठना चाहिए, जो तत्त्व-बोध से युक्त हो। यदि समीचीन नहीं
है, तो क्या प्ररूपणा की जाएगी? .... स्वयं प्रश्न करना चाहिए, एक अक्षर भी आगम-विरुद्ध
कथन में आ गया, तो ज्ञानी तत्क्षण सम्यक्त्व की हानि समझना चाहिए। 3. अल्पज्ञानी कहलाना अच्छा है, बहुज्ञानी कहलाने के लोभ में मन-वाणी का प्रयोग स्वप्न में
भी नहीं करना, अन्यथा आगम से बाधित हो जाओगे। 4. देखो, जब जीव जानकर, पूर्वाचार्यों के विरुद्ध कथन करता है, तब उसे ज्ञात रहता है
अन्तरंग से कषाय के उद्रेक से तपता है, अन्तःकरण से दुःखी, विशुद्धि स्थान से पतित हो
रहा है। 5. जो जीव आगम-ज्ञान प्राप्त करके द्रव्य-श्रुत को भाव-श्रुत की प्राप्ति का पुरुषार्थ करता है,
वह शीघ्र ही कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होता है। अन्तिम समय परिणामों की विशुद्धि बनी
रही हो, तो समझना कि वह भाग्यवान् पुरुष निर्दोष श्रुताराधक रहा है। 6. आगम-ग्रंथों में ज्ञान का फल विशुद्ध-भावों की उपलब्धि है, राग-द्वेष की वृद्धि करना,
कराना, अनुमोदना करना, ये ज्ञानीपने की पहचान किञ्चित् भी नहीं है। 7. अहो! गाय के सींग से दुग्धधारा नहीं निकलती, उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि के ज्ञान में
प्रमाणितपना नहीं होता।। 8. भिन्न ज्ञेयों के निमित्त से ज्ञान-गुण तद्रूप परिणमन होता है-इस अपेक्षा से जैसा ज्ञेय होता
है, ज्ञेय ज्ञेय ही है। 9. अकलंक स्वामी ने इस एक कारिका में जैन दर्शन का सार प्रदान किया है। अहो!
आचार्य-प्रवर की प्रज्ञा एवं दर्शन-चरित्र अति विशद था, निर्मल आत्म-तत्त्व ही यथार्थ-तत्त्व उपदेशक हो सकता है।
तेरहवीं एवं चौदहवीं कारिकाओं में सम्यक्-चारित्र के स्वरूप का परिशीलन आचार्य-श्री ने भली-भाँति निम्नप्रकार किया है1. चतुर्थ गुणस्थान में सम्यक्त्वाचरण है, परन्तु मनीषियो! वह सम्यक्त्वाचरण साधन का ही
साधन है। साध्य-प्राप्ति का साक्षात्-कारण न हुआ, न कभी होगा, वह कारण-समयसार का भी कारण है। कार्य-समयसार तो ज्ञानियो! सकल-निकल परमात्मा ही है। सकल-निकल परमात्मा की उपलब्धि कराने वाला साक्षात्-कारण चारित्र है। गुणस्थानों में स्व-स्थान सम्बन्धी विशुद्धि अवश्य है, तद्-तद् अनुभूति भी है। संवेदन तो आत्मा का धर्म है। वह
स्व-संवेदन परम शुद्ध संवेदन नहीं है, अव्रत-रूप स्व-संवेदन ही है। 2. जो जीव चारित्र को गौण करके सर्वथा ज्ञान-दर्शन की चर्चा करते हैं, परन्तु संयम से
सर्वथा उदास रहते हैं, वे वीतराग शासन के प्रति अवात्सल्यता का व्यवहार करते हैं। कारण दर्शन-ज्ञान मात्र वीतरागता को प्रकट करने में समर्थ नहीं हैं। जब भी वीतरागता का उदय होगा तब ज्ञानी सम्यक्-चारित्र के सद्भाव से ही होगा, वीतरागता और
सम्यक्-चारित्र का अविनाभाव सम्बन्ध है। 3. जैन-योगियों का मार्ग जगत् के मार्गों से अत्यन्त भिन्न है, ऐसा समझना चाहिए। साथ ही
उन ज्ञानी विद्वानों को भी इंगित करता हूँ, जो साधु समाज से लौकिक कार्यों की अपेक्षा