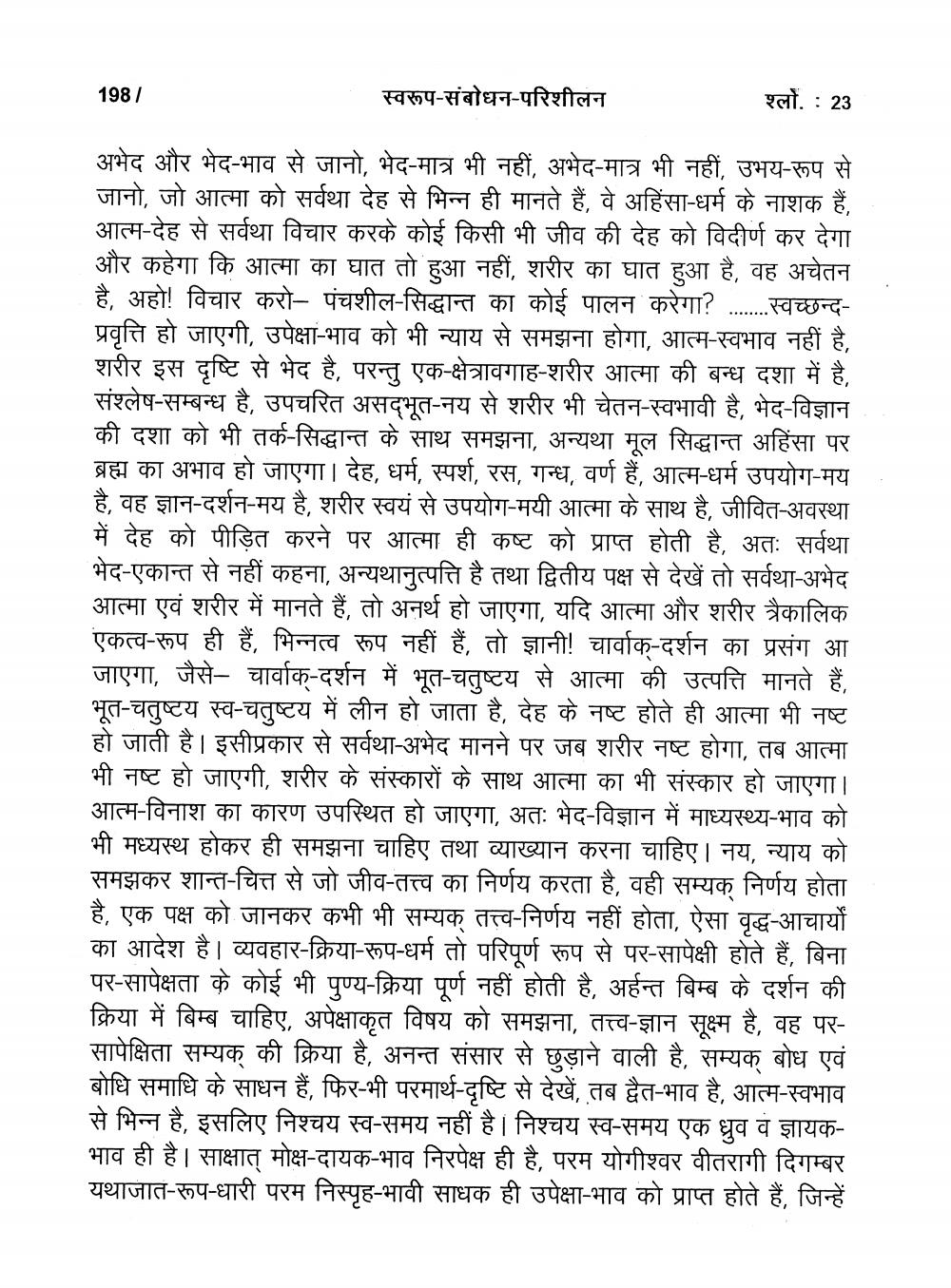________________
1981
स्वरूप-संबोधन-परिशीलन
श्लो. : 23
अभेद और भेद-भाव से जानो, भेद-मात्र भी नहीं, अभेद-मात्र भी नहीं, उभय-रूप से जानो, जो आत्मा को सर्वथा देह से भिन्न ही मानते हैं, वे अहिंसा-धर्म के नाशक हैं, आत्म-देह से सर्वथा विचार करके कोई किसी भी जीव की देह को विदीर्ण कर देगा और कहेगा कि आत्मा का घात तो हुआ नहीं, शरीर का घात हुआ है, वह अचेतन है, अहो! विचार करो- पंचशील-सिद्धान्त का कोई पालन करेगा? .....स्वच्छन्दप्रवृत्ति हो जाएगी, उपेक्षा-भाव को भी न्याय से समझना होगा, आत्म-स्वभाव नहीं है, शरीर इस दृष्टि से भेद है, परन्तु एक-क्षेत्रावगाह-शरीर आत्मा की बन्ध दशा में है, संश्लेष-सम्बन्ध है, उपचरित असद्भूत-नय से शरीर भी चेतन-स्वभावी है, भेद-विज्ञान की दशा को भी तर्क-सिद्धान्त के साथ समझना, अन्यथा मूल सिद्धान्त अहिंसा पर ब्रह्म का अभाव हो जाएगा। देह, धर्म, स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण हैं, आत्म-धर्म उपयोग-मय है, वह ज्ञान-दर्शन-मय है, शरीर स्वयं से उपयोग-मयी आत्मा के साथ है, जीवित-अवस्था में देह को पीड़ित करने पर आत्मा ही कष्ट को प्राप्त होती है, अतः सर्वथा भेद-एकान्त से नहीं कहना, अन्यथानुत्पत्ति है तथा द्वितीय पक्ष से देखें तो सर्वथा-अभेद आत्मा एवं शरीर में मानते हैं, तो अनर्थ हो जाएगा, यदि आत्मा और शरीर त्रैकालिक एकत्व-रूप ही हैं, भिन्नत्व रूप नहीं हैं, तो ज्ञानी! चार्वाक्-दर्शन का प्रसंग आ जाएगा. जैसे- चार्वाक-दर्शन में भत-चतष्टय से आत्मा की उत्पत्ति मानते हैं भूत-चतुष्टय स्व-चतुष्टय में लीन हो जाता है, देह के नष्ट होते ही आत्मा भी नष्ट हो जाती है। इसीप्रकार से सर्वथा अभेद मानने पर जब शरीर नष्ट होगा, तब आत्मा भी नष्ट हो जाएगी, शरीर के संस्कारों के साथ आत्मा का भी संस्कार हो जाएगा। आत्म-विनाश का कारण उपस्थित हो जाएगा, अतः भेद-विज्ञान में माध्यस्थ्य-भाव को भी मध्यस्थ होकर ही समझना चाहिए तथा व्याख्यान करना चाहिए। नय, न्याय को समझकर शान्त-चित्त से जो जीव-तत्त्व का निर्णय करता है, वही सम्यक् निर्णय होता है, एक पक्ष को जानकर कभी भी सम्यक तत्त्व-निर्णय नहीं होता, ऐसा वृद्ध-आचार्यों का आदेश है। व्यवहार-क्रिया-रूप-धर्म तो परिपूर्ण रूप से पर-सापेक्षी होते हैं, बिना पर-सापेक्षता के कोई भी पुण्य-क्रिया पूर्ण नहीं होती है, अर्हन्त बिम्ब के दर्शन की क्रिया में बिम्ब चाहिए, अपेक्षाकृत विषय को समझना, तत्त्व-ज्ञान सूक्ष्म है, वह परसापेक्षिता सम्यक् की क्रिया है, अनन्त संसार से छुड़ाने वाली है, सम्यक् बोध एवं बोधि समाधि के साधन हैं, फिर भी परमार्थ-दृष्टि से देखें, तब द्वैत-भाव है, आत्म-स्वभाव से भिन्न है, इसलिए निश्चय स्व-समय नहीं है। निश्चय स्व-समय एक ध्रुव व ज्ञायकभाव ही है। साक्षात् मोक्ष-दायक-भाव निरपेक्ष ही है, परम योगीश्वर वीतरागी दिगम्बर यथाजात-रूप-धारी परम निस्पृह-भावी साधक ही उपेक्षा-भाव को प्राप्त होते हैं, जिन्हें