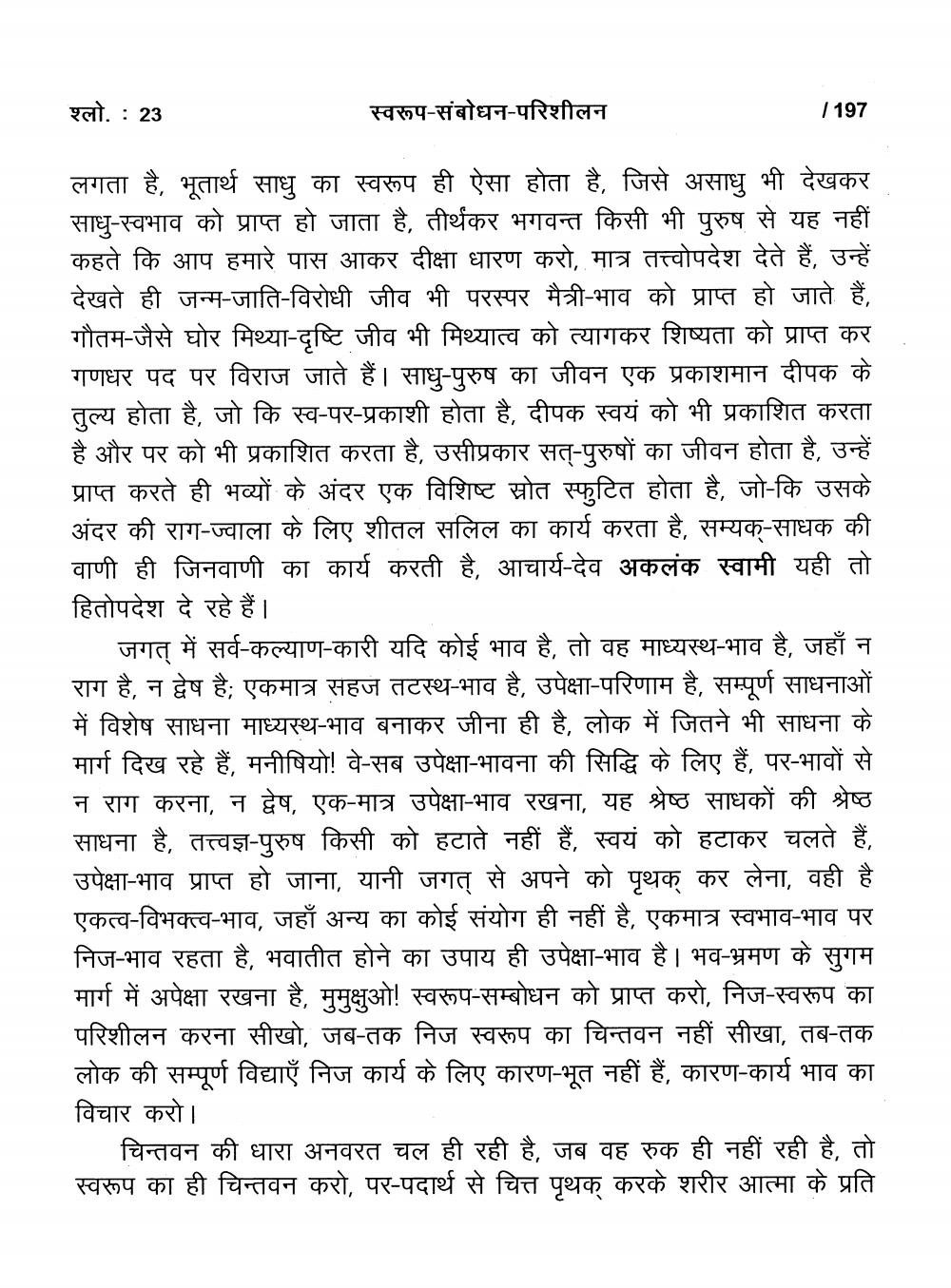________________
श्लो . : 23
स्वरूप-संबोधन-परिशीलन
1197
लगता है, भूतार्थ साधु का स्वरूप ही ऐसा होता है, जिसे असाधु भी देखकर साधु-स्वभाव को प्राप्त हो जाता है, तीर्थंकर भगवन्त किसी भी पुरुष से यह नहीं कहते कि आप हमारे पास आकर दीक्षा धारण करो, मात्र तत्त्वोपदेश देते हैं, उन्हें देखते ही जन्म-जाति-विरोधी जीव भी परस्पर मैत्री-भाव को प्राप्त हो जाते हैं, गौतम-जैसे घोर मिथ्या-दृष्टि जीव भी मिथ्यात्व को त्यागकर शिष्यता को प्राप्त कर गणधर पद पर विराज जाते हैं। साधु-पुरुष का जीवन एक प्रकाशमान दीपक के तुल्य होता है, जो कि स्व-पर-प्रकाशी होता है, दीपक स्वयं को भी प्रकाशित करता है और पर को भी प्रकाशित करता है, उसीप्रकार सत्-पुरुषों का जीवन होता है, उन्हें प्राप्त करते ही भव्यों के अंदर एक विशिष्ट स्रोत स्फुटित होता है, जो-कि उसके अंदर की राग-ज्वाला के लिए शीतल सलिल का कार्य करता है, सम्यक्-साधक की वाणी ही जिनवाणी का कार्य करती है, आचार्य-देव अकलंक स्वामी यही तो हितोपदेश दे रहे हैं।
जगत् में सर्व-कल्याण-कारी यदि कोई भाव है, तो वह माध्यस्थ-भाव है, जहाँ न राग है, न द्वेष है; एकमात्र सहज तटस्थ-भाव है, उपेक्षा परिणाम है, सम्पूर्ण साधनाओं में विशेष साधना माध्यस्थ-भाव बनाकर जीना ही है, लोक में जितने भी साधना के मार्ग दिख रहे हैं, मनीषियो! वे-सब उपेक्षा-भावना की सिद्धि के लिए हैं, पर-भावों से न राग करना, न द्वेष, एक-मात्र उपेक्षा-भाव रखना, यह श्रेष्ठ साधकों की श्रेष्ठ साधना है, तत्त्वज्ञ-पुरुष किसी को हटाते नहीं हैं, स्वयं को हटाकर चलते हैं, उपेक्षा-भाव प्राप्त हो जाना, यानी जगत् से अपने को पृथक् कर लेना, वही है एकत्व-विभक्त्व-भाव, जहाँ अन्य का कोई संयोग ही नहीं है, एकमात्र स्वभाव-भाव पर निज-भाव रहता है, भवातीत होने का उपाय ही उपेक्षा-भाव है। भव-भ्रमण के सुगम मार्ग में अपेक्षा रखना है, मुमुक्षुओ! स्वरूप-सम्बोधन को प्राप्त करो, निज-स्वरूप का परिशीलन करना सीखो, जब-तक निज स्वरूप का चिन्तवन नहीं सीखा, तब-तक लोक की सम्पूर्ण विद्याएँ निज कार्य के लिए कारण-भूत नहीं हैं, कारण-कार्य भाव का विचार करो।
चिन्तवन की धारा अनवरत चल ही रही है, जब वह रुक ही नहीं रही है, तो स्वरूप का ही चिन्तवन करो, पर-पदार्थ से चित्त पृथक् करके शरीर आत्मा के प्रति