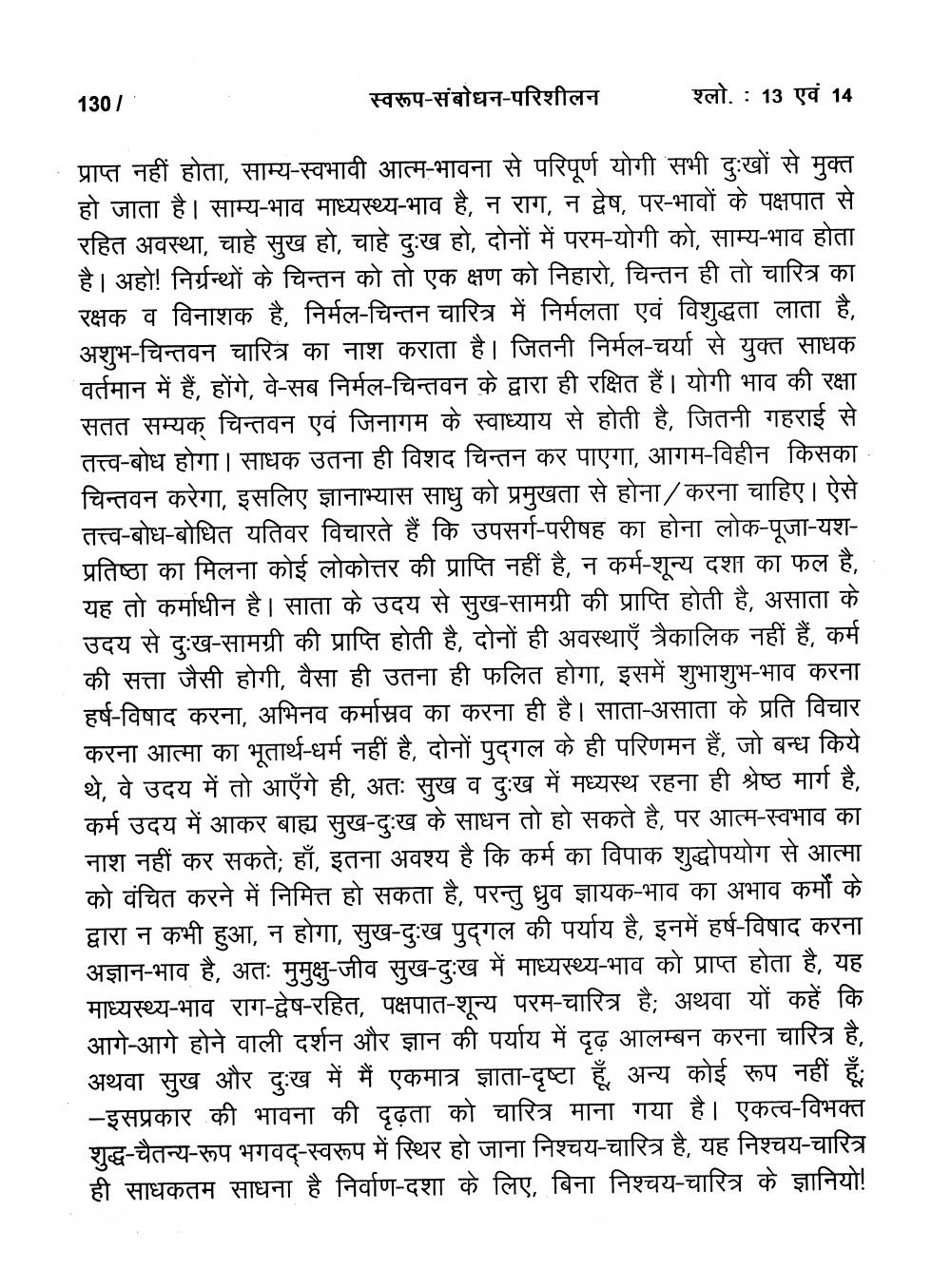________________
1301
स्वरूप-संबोधन-परिशीलन
श्लो. : 13 एवं 14
प्राप्त नहीं होता, साम्य-स्वभावी आत्म-भावना से परिपूर्ण योगी सभी दुःखों से मुक्त हो जाता है। साम्य-भाव माध्यस्थ्य-भाव है, न राग, न द्वेष, पर-भावों के पक्षपात से रहित अवस्था, चाहे सुख हो, चाहे दुःख हो, दोनों में परम-योगी को, साम्य-भाव होता है। अहो! निर्ग्रन्थों के चिन्तन को तो एक क्षण को निहारो, चिन्तन ही तो चारित्र का रक्षक व विनाशक है, निर्मल-चिन्तन चारित्र में निर्मलता एवं विशुद्धता लाता है, अशुभ-चिन्तवन चारित्र का नाश कराता है। जितनी निर्मल-चर्या से युक्त साधक वर्तमान में हैं, होंगे, वे-सब निर्मल-चिन्तवन के द्वारा ही रक्षित हैं। योगी भाव की रक्षा सतत सम्यक् चिन्तवन एवं जिनागम के स्वाध्याय से होती है, जितनी गहराई से तत्त्व-बोध होगा। साधक उतना ही विशद चिन्तन कर पाएगा, आगम-विहीन किसका चिन्तवन करेगा, इसलिए ज्ञानाभ्यास साधु को प्रमुखता से होना/करना चाहिए। ऐसे तत्त्व-बोध-बोधित यतिवर विचारते हैं कि उपसर्ग-परीषह का होना लोक-पूजा-यशप्रतिष्ठा का मिलना कोई लोकोत्तर की प्राप्ति नहीं है, न कर्म-शून्य दशा का फल है, यह तो कर्माधीन है। साता के उदय से सुख-सामग्री की प्राप्ति होती है, असाता के उदय से दुःख-सामग्री की प्राप्ति होती है, दोनों ही अवस्थाएँ त्रैकालिक नहीं हैं, कर्म की सत्ता जैसी होगी, वैसा ही उतना ही फलित होगा, इसमें शुभाशुभ-भाव करना हर्ष-विषाद करना, अभिनव कर्मास्रव का करना ही है। साता-असाता के प्रति विचार करना आत्मा का भूतार्थ-धर्म नहीं है, दोनों पुदगल के ही परिणमन हैं, जो बन्ध किये थे, वे उदय में तो आएँगे ही, अतः सुख व दुःख में मध्यस्थ रहना ही श्रेष्ठ मार्ग है, कर्म उदय में आकर बाह्य सुख-दुःख के साधन तो हो सकते है, पर आत्म-स्वभाव का नाश नहीं कर सकते; हाँ, इतना अवश्य है कि कर्म का विपाक शुद्धोपयोग से आत्मा को वंचित करने में निमित्त हो सकता है, परन्तु ध्रुव ज्ञायक-भाव का अभाव कर्मों के द्वारा न कभी हुआ, न होगा, सुख-दुःख पुद्गल की पर्याय है, इनमें हर्ष-विषाद करना अज्ञान-भाव है, अतः मुमुक्षु-जीव सुख-दुःख में माध्यस्थ्य-भाव को प्राप्त होता है, यह माध्यस्थ्य-भाव राग-द्वेष-रहित, पक्षपात-शून्य परम-चारित्र है; अथवा यों कहें कि आगे-आगे होने वाली दर्शन और ज्ञान की पर्याय में दृढ़ आलम्बन करना चारित्र है, अथवा सुख और दुःख में मैं एकमात्र ज्ञाता-दृष्टा हूँ, अन्य कोई रूप नहीं हूँ; -इसप्रकार की भावना की दृढ़ता को चारित्र माना गया है। एकत्व-विभक्त शुद्ध-चैतन्य-रूप भगवद्-स्वरूप में स्थिर हो जाना निश्चय-चारित्र है, यह निश्चय-चारित्र ही साधकतम साधना है निर्वाण-दशा के लिए, बिना निश्चय-चारित्र के ज्ञानियो!