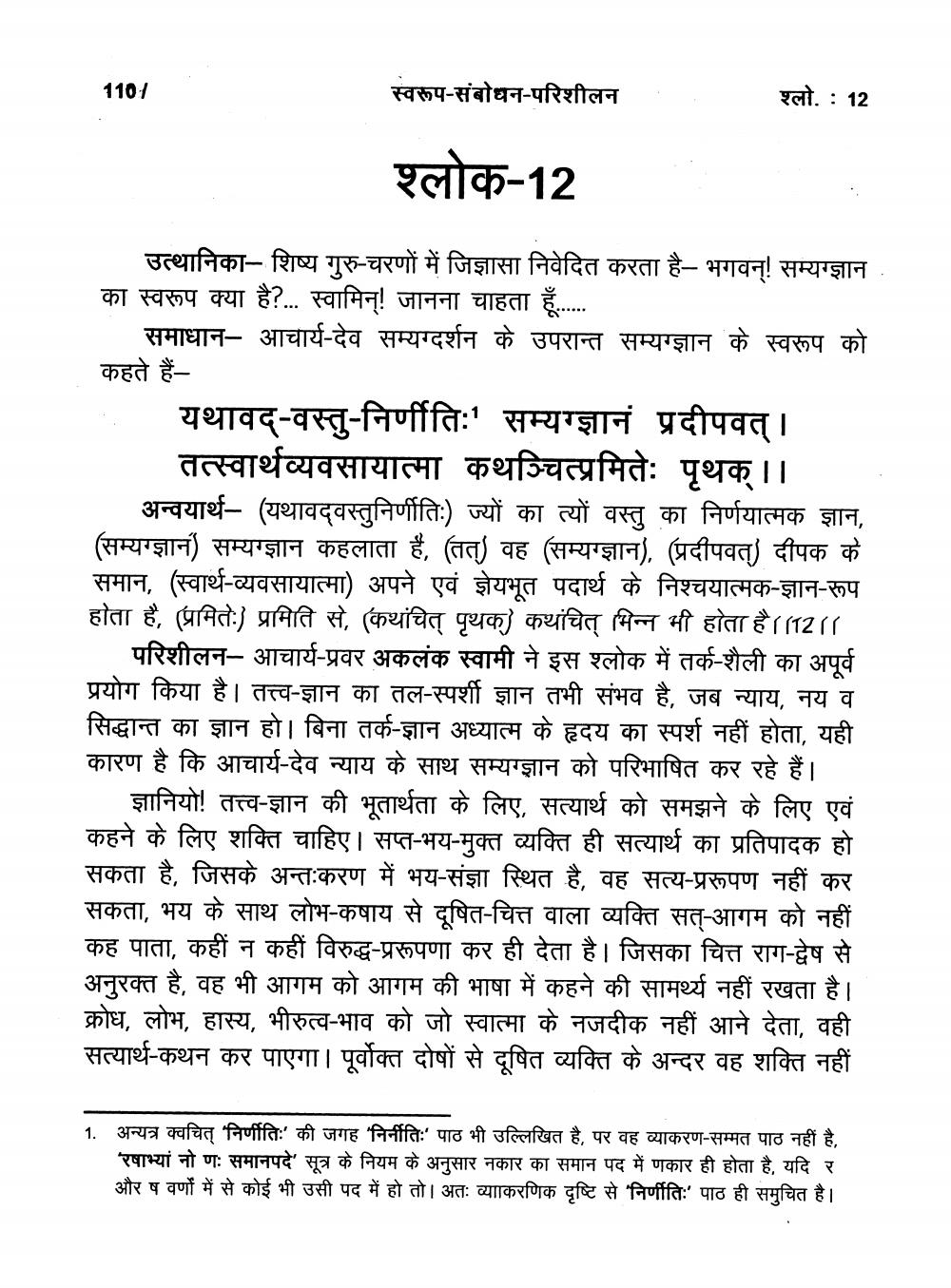________________
1101
स्वरूप-संबोधन-परिशीलन
श्लो. : 12
श्लोक-12
उत्थानिका- शिष्य गुरु-चरणों में जिज्ञासा निवेदित करता है- भगवन्! सम्यग्ज्ञान . का स्वरूप क्या है?... स्वामिन्! जानना चाहता हूँ.......
समाधान- आचार्य-देव सम्यग्दर्शन के उपरान्त सम्यग्ज्ञान के स्वरूप को कहते हैं
यथावद्-वस्तु-निर्णीतिः' सम्यग्ज्ञानं प्रदीपवत् ।
तत्स्वार्थव्यवसायात्मा कथञ्चित्प्रमितेः पृथक् ।। अन्वयार्थ- (यथावद्वस्तुनिर्णीतिः) ज्यों का त्यों वस्तु का निर्णयात्मक ज्ञान, (सम्यग्ज्ञान) सम्यग्ज्ञान कहलाता है, (तत्) वह (सम्यग्ज्ञान), (प्रदीपवत्) दीपक के समान, (स्वार्थ-व्यवसायात्मा) अपने एवं ज्ञेयभूत पदार्थ के निश्चयात्मक-ज्ञान-रूप होता है, (प्रमिते.) प्रमिति से, (कथांचत् पृथक) कथांचत् मिन्न भी होता है। [1200
परिशीलन- आचार्य-प्रवर अकलंक स्वामी ने इस श्लोक में तर्क-शैली का अपूर्व प्रयोग किया है। तत्त्व-ज्ञान का तल-स्पर्शी ज्ञान तभी संभव है, जब न्याय, नय व सिद्धान्त का ज्ञान हो। बिना तर्क-ज्ञान अध्यात्म के हृदय का स्पर्श नहीं होता, यही कारण है कि आचार्य-देव न्याय के साथ सम्यग्ज्ञान को परिभाषित कर रहे हैं।
ज्ञानियो! तत्त्व-ज्ञान की भूतार्थता के लिए, सत्यार्थ को समझने के लिए एवं कहने के लिए शक्ति चाहिए। सप्त-भय-मुक्त व्यक्ति ही सत्यार्थ का प्रतिपादक हो सकता है, जिसके अन्तःकरण में भय-संज्ञा स्थित है, वह सत्य-प्ररूपण नहीं कर सकता, भय के साथ लोभ-कषाय से दूषित-चित्त वाला व्यक्ति सत्-आगम को नहीं कह पाता, कहीं न कहीं विरुद्ध-प्ररूपणा कर ही देता है। जिसका चित्त राग-द्वेष से अनुरक्त है, वह भी आगम को आगम की भाषा में कहने की सामर्थ्य नहीं रखता है। क्रोध, लोभ, हास्य, भीरुत्व-भाव को जो स्वात्मा के नजदीक नहीं आने देता, वही सत्यार्थ-कथन कर पाएगा। पूर्वोक्त दोषों से दूषित व्यक्ति के अन्दर वह शक्ति नहीं
अन्यत्र क्वचित् 'निर्णीतिः' की जगह निर्नीतिः' पाठ भी उल्लिखित है, पर वह व्याकरण-सम्मत पाठ नहीं है, 'रषाभ्यां नो णः समानपदे' सूत्र के नियम के अनुसार नकार का समान पद में णकार ही होता है, यदि र और ष वर्गों में से कोई भी उसी पद में हो तो। अतः व्याकरणिक दृष्टि से 'निर्णीतिः' पाठ ही समुचित है।