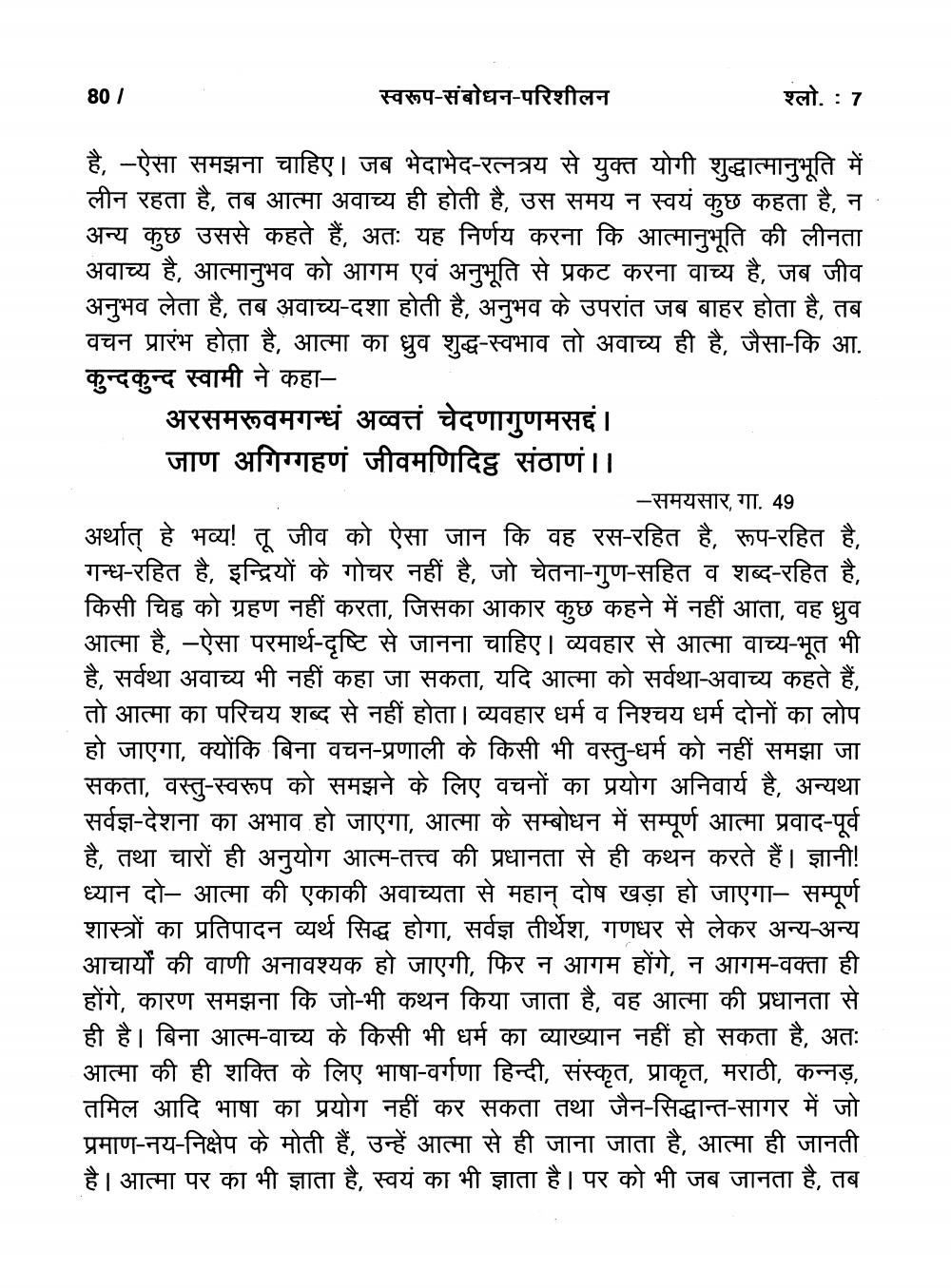________________
80/
स्वरूप-संबोधन-परिशीलन
श्लो. : 7
है, -ऐसा समझना चाहिए। जब भेदाभेद-रत्नत्रय से युक्त योगी शुद्धात्मानुभूति में लीन रहता है, तब आत्मा अवाच्य ही होती है, उस समय न स्वयं कुछ कहता है, न अन्य कुछ उससे कहते हैं, अतः यह निर्णय करना कि आत्मानुभूति की लीनता अवाच्य है, आत्मानुभव को आगम एवं अनुभूति से प्रकट करना वाच्य है, जब जीव अनुभव लेता है, तब अवाच्य-दशा होती है, अनुभव के उपरांत जब बाहर होता है, तब वचन प्रारंभ होता है, आत्मा का ध्रुव शुद्ध-स्वभाव तो अवाच्य ही है, जैसा कि आ. कुन्दकुन्द स्वामी ने कहा
अरसमरूवमगन्धं अव्वत्तं चेदणागुणमसदं । जाण अगिग्गहणं जीवमणिदिट्ठ संठाणं।।
-समयसार गा. 49 अर्थात् हे भव्य! तू जीव को ऐसा जान कि वह रस-रहित है, रूप-रहित है, गन्ध-रहित है, इन्द्रियों के गोचर नहीं है, जो चेतना-गुण-सहित व शब्द-रहित है, किसी चिह को ग्रहण नहीं करता, जिसका आकार कुछ कहने में नहीं आता, वह ध्रुव
आत्मा है, -ऐसा परमार्थ-दृष्टि से जानना चाहिए। व्यवहार से आत्मा वाच्य-भूत भी है, सर्वथा अवाच्य भी नहीं कहा जा सकता, यदि आत्मा को सर्वथा-अवाच्य कहते हैं, तो आत्मा का परिचय शब्द से नहीं होता। व्यवहार धर्म व निश्चय धर्म दोनों का लोप हो जाएगा, क्योंकि बिना वचन-प्रणाली के किसी भी वस्तु-धर्म को नहीं समझा जा सकता, वस्तु-स्वरूप को समझने के लिए वचनों का प्रयोग अनिवार्य है, अन्यथा सर्वज्ञ-देशना का अभाव हो जाएगा, आत्मा के सम्बोधन में सम्पूर्ण आत्मा प्रवाद-पूर्व है, तथा चारों ही अनुयोग आत्म-तत्त्व की प्रधानता से ही कथन करते हैं। ज्ञानी! ध्यान दो- आत्मा की एकाकी अवाच्यता से महान् दोष खड़ा हो जाएगा- सम्पूर्ण शास्त्रों का प्रतिपादन व्यर्थ सिद्ध होगा, सर्वज्ञ तीर्थेश, गणधर से लेकर अन्य अन्य आचार्यों की वाणी अनावश्यक हो जाएगी, फिर न आगम होंगे, न आगम-वक्ता ही होंगे, कारण समझना कि जो भी कथन किया जाता है, वह आत्मा की प्रधानता से ही है। बिना आत्म-वाच्य के किसी भी धर्म का व्याख्यान नहीं हो सकता है, अतः आत्मा की ही शक्ति के लिए भाषा-वर्गणा हिन्दी, संस्कृत, प्राकृत, मराठी, कन्नड़, तमिल आदि भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता तथा जैन-सिद्धान्त-सागर में जो प्रमाण-नय-निक्षेप के मोती हैं, उन्हें आत्मा से ही जाना जाता है, आत्मा ही जानती है। आत्मा पर का भी ज्ञाता है, स्वयं का भी ज्ञाता है। पर को भी जब जानता है, तब