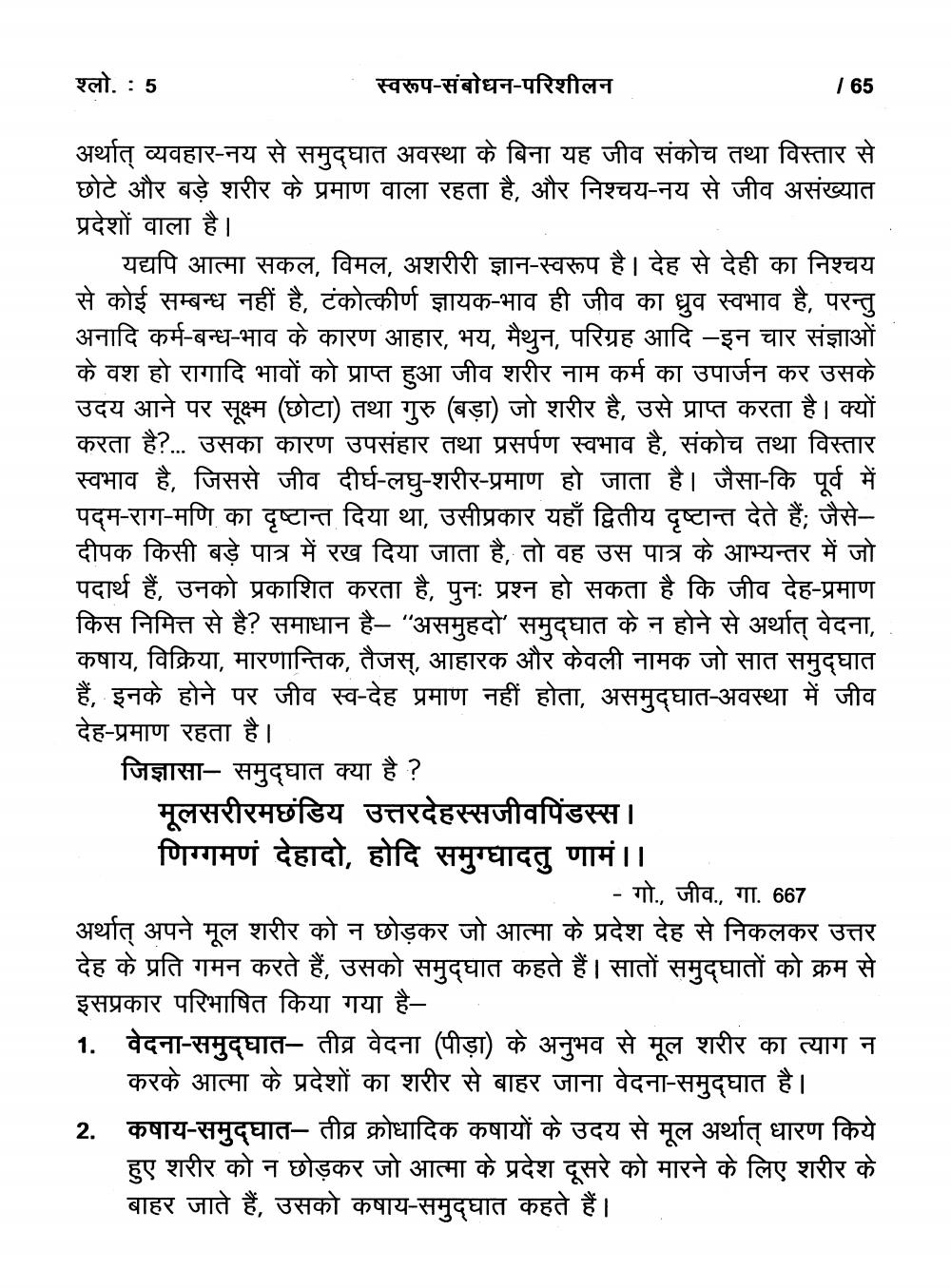________________
श्लो. : 5
स्वरूप-संबोधन-परिशीलन
165
अर्थात् व्यवहार-नय से समुद्घात अवस्था के बिना यह जीव संकोच तथा विस्तार से छोटे और बड़े शरीर के प्रमाण वाला रहता है, और निश्चय-नय से जीव असंख्यात प्रदेशों वाला है।
यद्यपि आत्मा सकल, विमल, अशरीरी ज्ञान-स्वरूप है। देह से देही का निश्चय से कोई सम्बन्ध नहीं है, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक-भाव ही जीव का ध्रुव स्वभाव है, परन्तु अनादि कर्म-बन्ध-भाव के कारण आहार, भय, मैथुन, परिग्रह आदि -इन चार संज्ञाओं के वश हो रागादि भावों को प्राप्त हुआ जीव शरीर नाम कर्म का उपार्जन कर उसके उदय आने पर सूक्ष्म (छोटा) तथा गुरु (बड़ा) जो शरीर है, उसे प्राप्त करता है। क्यों करता है?... उसका कारण उपसंहार तथा प्रसर्पण स्वभाव है, संकोच तथा विस्तार स्वभाव है, जिससे जीव दीर्घ-लघु-शरीर-प्रमाण हो जाता है। जैसा कि पूर्व में पद्म-राग-मणि का दृष्टान्त दिया था, उसीप्रकार यहाँ द्वितीय दृष्टान्त देते हैं; जैसेदीपक किसी बड़े पात्र में रख दिया जाता है, तो वह उस पात्र के आभ्यन्तर में जो पदार्थ हैं, उनको प्रकाशित करता है, पुनः प्रश्न हो सकता है कि जीव देह-प्रमाण किस निमित्त से है? समाधान है- "असमुहदो समुद्घात के न होने से अर्थात् वेदना, कषाय, विक्रिया, मारणान्तिक, तैजस्, आहारक और केवली नामक जो सात समुद्घात हैं, इनके होने पर जीव स्व-देह प्रमाण नहीं होता, असमुद्घात-अवस्था में जीव देह-प्रमाण रहता है। जिज्ञासा- समुद्घात क्या है ?
मूलसरीरमछंडिय उत्तरदेहस्सजीवपिंडस्स। णिग्गमणं देहादो, होदि समुग्घादतु णाम।।
- गो., जीव., गा. 667 अर्थात् अपने मूल शरीर को न छोड़कर जो आत्मा के प्रदेश देह से निकलकर उत्तर देह के प्रति गमन करते हैं, उसको समुद्घात कहते हैं। सातों समुद्घातों को क्रम से इसप्रकार परिभाषित किया गया है1. वेदना-समुद्घात- तीव्र वेदना (पीड़ा) के अनुभव से मूल शरीर का त्याग न
करके आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर जाना वेदना-समुद्घात है। 2. कषाय-समुद्घात- तीव्र क्रोधादिक कषायों के उदय से मूल अर्थात् धारण किये
हुए शरीर को न छोड़कर जो आत्मा के प्रदेश दूसरे को मारने के लिए शरीर के बाहर जाते हैं, उसको कषाय-समुद्घात कहते हैं।