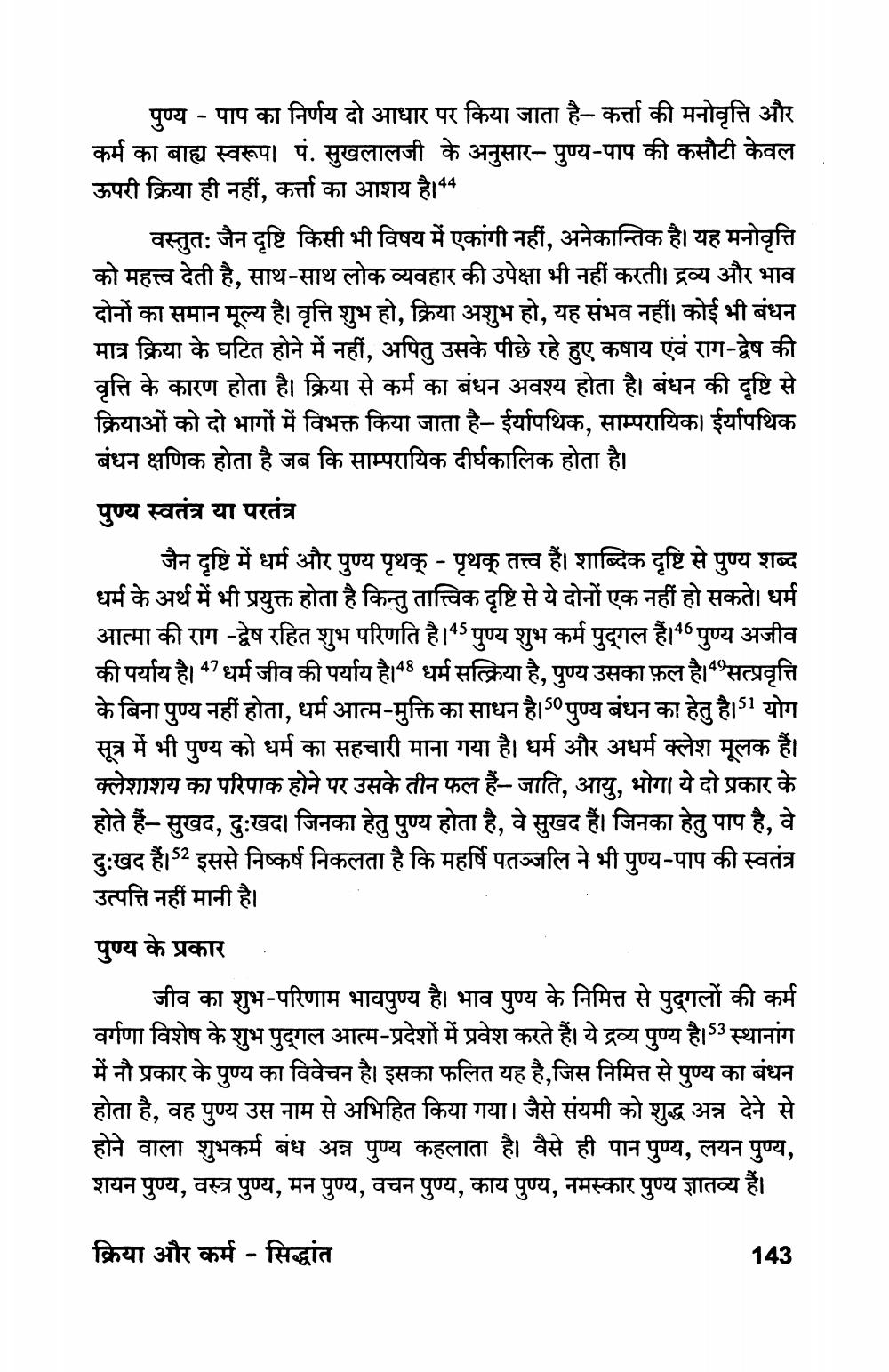________________
पुण्य - पाप का निर्णय दो आधार पर किया जाता है- कर्ता की मनोवृत्ति और कर्म का बाह्य स्वरूप। पं. सुखलालजी के अनुसार- पुण्य-पाप की कसौटी केवल ऊपरी क्रिया ही नहीं, कर्ता का आशय है।44
वस्तुत: जैन दृष्टि किसी भी विषय में एकांगी नहीं, अनेकान्तिक है। यह मनोवृत्ति को महत्त्व देती है, साथ-साथ लोक व्यवहार की उपेक्षा भी नहीं करती। द्रव्य और भाव दोनों का समान मूल्य है। वृत्ति शुभ हो, क्रिया अशुभ हो, यह संभव नहीं। कोई भी बंधन मात्र क्रिया के घटित होने में नहीं, अपितु उसके पीछे रहे हुए कषाय एवं राग-द्वेष की वृत्ति के कारण होता है। क्रिया से कर्म का बंधन अवश्य होता है। बंधन की दृष्टि से क्रियाओं को दो भागों में विभक्त किया जाता है- ईर्यापथिक, साम्परायिक। ईर्यापथिक बंधन क्षणिक होता है जब कि साम्परायिक दीर्घकालिक होता है। पुण्य स्वतंत्र या परतंत्र
जैन दृष्टि में धर्म और पुण्य पृथक् - पृथक् तत्त्व हैं। शाब्दिक दृष्टि से पुण्य शब्द धर्म के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है किन्तु तात्त्विक दृष्टि से ये दोनों एक नहीं हो सकते। धर्म आत्मा की राग -द्वेष रहित शुभ परिणति है।45 पुण्य शुभ कर्म पुद्गल हैं। पुण्य अजीव की पर्याय है। 47 धर्म जीव की पर्याय है।48 धर्म सत्क्रिया है, पुण्य उसका फ़ल है।4"सत्प्रवृत्ति के बिना पुण्य नहीं होता, धर्म आत्म-मुक्ति का साधन है। पुण्य बंधन का हेतु है।51 योग सूत्र में भी पुण्य को धर्म का सहचारी माना गया है। धर्म और अधर्म क्लेश मूलक हैं। क्लेशाशय का परिपाक होने पर उसके तीन फल हैं- जाति, आयु, भोग। ये दो प्रकार के होते हैं- सुखद, दुःखद। जिनका हेतु पुण्य होता है, वे सुखद हैं। जिनका हेतु पाप है, वे दुःखद हैं।52 इससे निष्कर्ष निकलता है कि महर्षि पतञ्जलि ने भी पुण्य-पाप की स्वतंत्र उत्पत्ति नहीं मानी है। पुण्य के प्रकार
जीव का शुभ-परिणाम भावपुण्य है। भाव पुण्य के निमित्त से पुद्गलों की कर्म वर्गणा विशेष के शुभ पुद्गल आत्म-प्रदेशों में प्रवेश करते हैं। ये द्रव्य पुण्य है। स्थानांग में नौ प्रकार के पुण्य का विवेचन है। इसका फलित यह है,जिस निमित्त से पुण्य का बंधन होता है, वह पुण्य उस नाम से अभिहित किया गया। जैसे संयमी को शुद्ध अन्न देने से होने वाला शुभकर्म बंध अन्न पुण्य कहलाता है। वैसे ही पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य, नमस्कार पुण्य ज्ञातव्य हैं।
क्रिया और कर्म - सिद्धांत
143