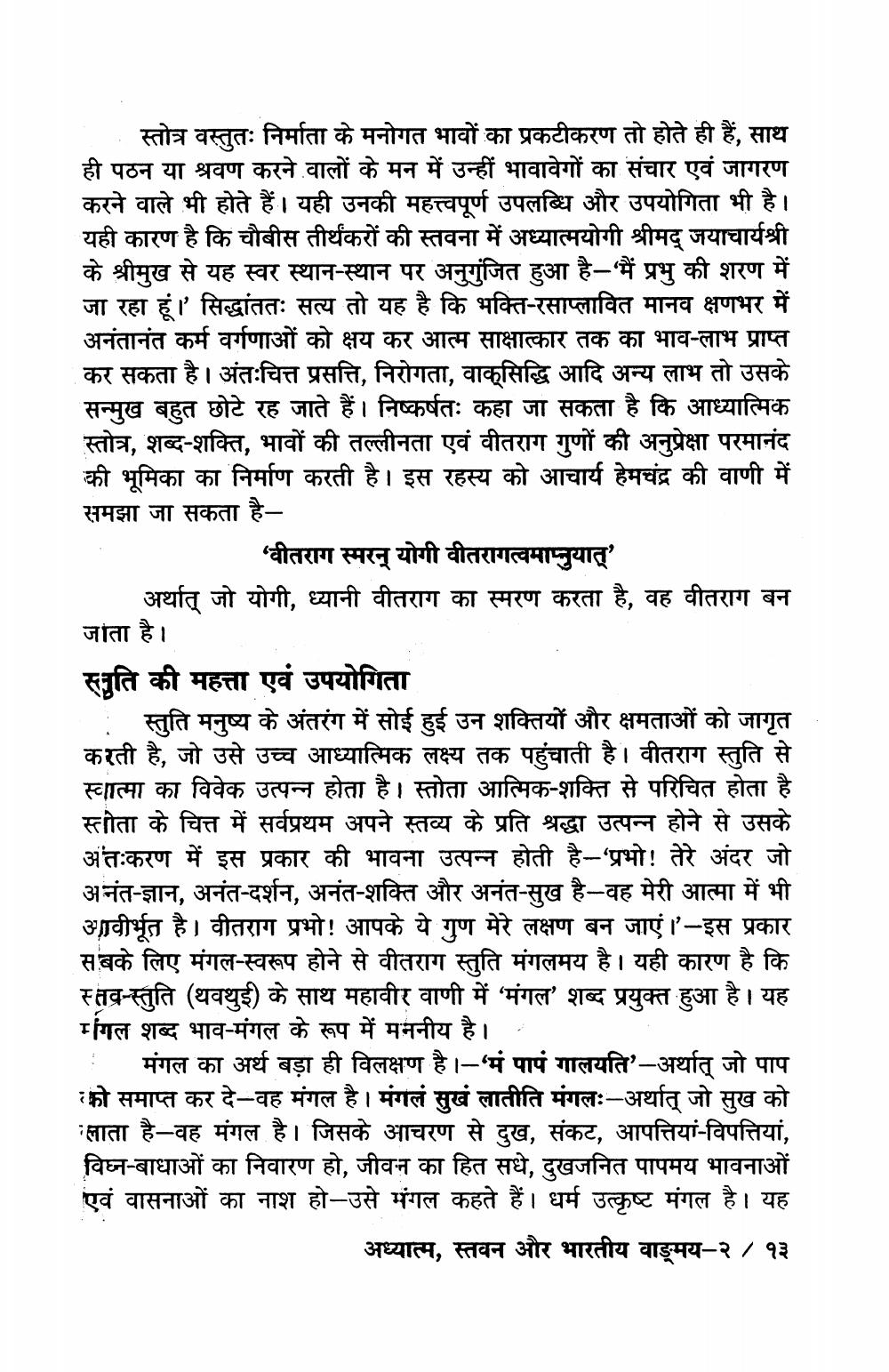________________
__स्तोत्र वस्तुतः निर्माता के मनोगत भावों का प्रकटीकरण तो होते ही हैं, साथ ही पठन या श्रवण करने वालों के मन में उन्हीं भावावेगों का संचार एवं जागरण करने वाले भी होते हैं। यही उनकी महत्त्वपूर्ण उपलब्धि और उपयोगिता भी है। यही कारण है कि चौबीस तीर्थंकरों की स्तवना में अध्यात्मयोगी श्रीमद् जयाचार्यश्री के श्रीमुख से यह स्वर स्थान-स्थान पर अनुगुंजित हुआ है-“मैं प्रभु की शरण में जा रहा हूं।' सिद्धांततः सत्य तो यह है कि भक्ति-रसाप्लावित मानव क्षणभर में अनंतानंत कर्म वर्गणाओं को क्षय कर आत्म साक्षात्कार तक का भाव-लाभ प्राप्त कर सकता है। अंतःचित्त प्रसत्ति, निरोगता, वाक्सिद्धि आदि अन्य लाभ तो उसके सन्मुख बहुत छोटे रह जाते हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आध्यात्मिक स्तोत्र, शब्द-शक्ति, भावों की तल्लीनता एवं वीतराग गुणों की अनुप्रेक्षा परमानंद की भूमिका का निर्माण करती है। इस रहस्य को आचार्य हेमचंद्र की वाणी में समझा जा सकता है
_ 'वीतराग स्मरन् योगी वीतरागत्वमाप्नुयात्' ___ अर्थात् जो योगी, ध्यानी वीतराग का स्मरण करता है, वह वीतराग बन जाता है। स्तुति की महत्ता एवं उपयोगिता
. स्तुति मनुष्य के अंतरंग में सोई हुई उन शक्तियों और क्षमताओं को जागृत करती है, जो उसे उच्च आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुंचाती है। वीतराग स्तुति से स्वात्मा का विवेक उत्पन्न होता है। स्तोता आत्मिक-शक्ति से परिचित होता है स्तोता के चित्त में सर्वप्रथम अपने स्तव्य के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होने से उसके अंतःकरण में इस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है-'प्रभो! तेरे अंदर जो अनंत-ज्ञान, अनंत-दर्शन, अनंत-शक्ति और अनंत-सुख है-वह मेरी आत्मा में भी
आवीभूत है। वीतराग प्रभो! आपके ये गुण मेरे लक्षण बन जाएं।'-इस प्रकार सबके लिए मंगल-स्वरूप होने से वीतराग स्तुति मंगलमय है। यही कारण है कि स्तव-स्तुति (थवथुई) के साथ महावीर वाणी में ‘मंगल' शब्द प्रयुक्त हुआ है। यह मंगल शब्द भाव-मंगल के रूप में मननीय है। : मंगल का अर्थ बड़ा ही विलक्षण है।-'मं पापं गालयति' अर्थात् जो पाप को समाप्त कर दे-वह मंगल है। मंगलं सुखं लातीति मंगलः-अर्थात् जो सुख को लाता है-वह मंगल है। जिसके आचरण से दुख, संकट, आपत्तियां-विपत्तियां, विघ्न-बाधाओं का निवारण हो, जीवन का हित सधे, दुखजनित पापमय भावनाओं एवं वासनाओं का नाश हो-उसे मंगल कहते हैं। धर्म उत्कृष्ट मंगल है। यह
अध्यात्म, स्तवन और भारतीय वाङ्मय-२ / १३