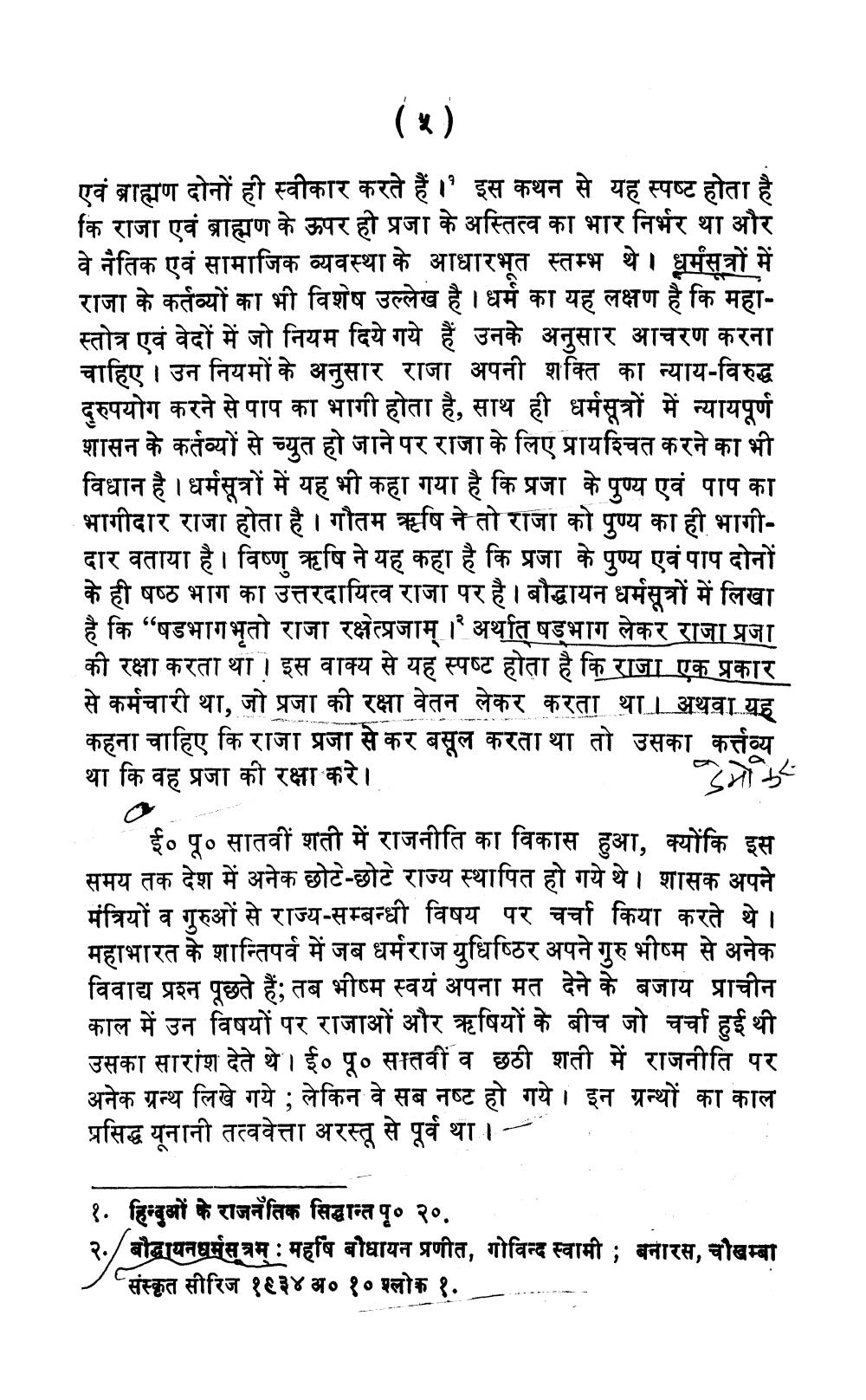________________
एवं ब्राह्मण दोनों ही स्वीकार करते हैं।' इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि राजा एवं ब्राह्मण के ऊपर हो प्रजा के अस्तित्व का भार निर्भर था और वे नैतिक एवं सामाजिक व्यवस्था के आधारभूत स्तम्भ थे। धर्मसत्रों में राजा के कर्तव्यों का भी विशेष उल्लेख है। धर्म का यह लक्षण है कि महास्तोत्र एवं वेदों में जो नियम दिये गये हैं उनके अनुसार आचरण करना चाहिए। उन नियमों के अनुसार राजा अपनी शक्ति का न्याय-विरुद्ध दुरुपयोग करने से पाप का भागी होता है, साथ ही धर्मसूत्रों में न्यायपूर्ण शासन के कर्तव्यों से च्युत हो जाने पर राजा के लिए प्रायश्चित करने का भी विधान है । धर्मसूत्रों में यह भी कहा गया है कि प्रजा के पुण्य एवं पाप का भागीदार राजा होता है । गौतम ऋषि ने तो राजा को पूण्य का ही भागीदार वताया है। विष्णु ऋषि ने यह कहा है कि प्रजा के पुण्य एवं पाप दोनों के ही षष्ठ भाग का उत्तरदायित्व राजा पर है। बौद्धायन धर्मसूत्रों में लिखा है कि “षडभागभतो राजा रक्षेत्प्रजाम् । अर्थात षड्भाग लेकर राजा प्रजा की रक्षा करता था। इस वाक्य से यह स्पष्ट होता है कि राजा एक प्रकार से कर्मचारी था, जो प्रजा की रक्षा वेतन लेकर करता था। अथवा यह कहना चाहिए कि राजा प्रजा से कर बसूल करता था तो उसका कर्तव्य था कि वह प्रजा की रक्षा करे।
- ई० पू० सातवीं शती में राजनीति का विकास हुआ, क्योंकि इस समय तक देश में अनेक छोटे-छोटे राज्य स्थापित हो गये थे। शासक अपने मंत्रियों व गुरुओं से राज्य-सम्बन्धी विषय पर चर्चा किया करते थे। महाभारत के शान्तिपर्व में जब धर्मराज युधिष्ठिर अपने गुरु भीष्म से अनेक विवाद्य प्रश्न पूछते हैं; तब भीष्म स्वयं अपना मत देने के बजाय प्राचीन काल में उन विषयों पर राजाओं और ऋषियों के बीच जो चर्चा हुई थी उसका सारांश देते थे। ई० पू० सातवीं व छठी शती में राजनीति पर अनेक ग्रन्थ लिखे गये ; लेकिन वे सब नष्ट हो गये। इन ग्रन्थों का काल प्रसिद्ध यूनानी तत्ववेत्ता अरस्तू से पूर्व था।
१. हिन्दुओं के राजनैतिक सिद्धान्त पृ० २०. २./बौद्धायनधर्मसूत्रम् : महर्षि बोधायन प्रणीत, गोविन्द स्वामी ; बनारस, चौखम्बा / संस्कृत सीरिज १९३४ अ० १० श्लोक १. ..