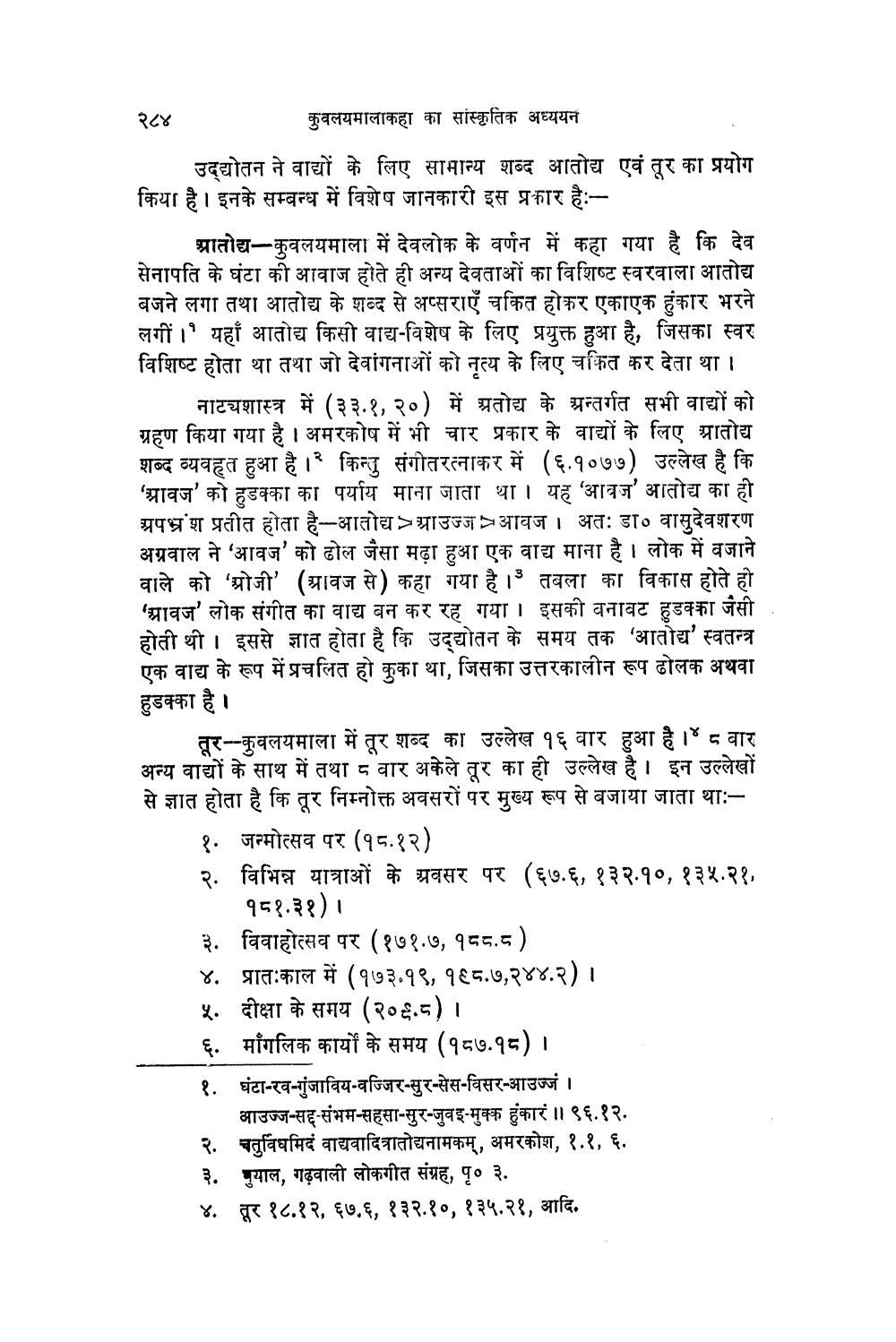________________
२८४
कुवलयमालाकहा का सांस्कृतिक अध्ययन
उद्द्योतन ने वाद्यों के लिए सामान्य शब्द आतोद्य एवं तूर का प्रयोग किया है। इनके सम्बन्ध में विशेष जानकारी इस प्रकार है:
प्रातोद्य-कुवलयमाला में देवलोक के वर्णन में कहा गया है कि देव सेनापति के घंटा की आवाज होते ही अन्य देवताओं का विशिष्ट स्वरवाला आतोद्य बजने लगा तथा आतोद्य के शब्द से अप्सराएँ चकित होकर एकाएक हुंकार भरने लगीं।' यहाँ आतोद्य किसी वाद्य-विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिसका स्वर विशिष्ट होता था तथा जो देवांगनाओं को नृत्य के लिए चकित कर देता था।
नाट्यशास्त्र में (३३.१, २०) में अतोद्य के अन्तर्गत सभी वाद्यों को ग्रहण किया गया है । अमरकोष में भी चार प्रकार के वाद्यों के लिए पातोद्य शब्द व्यवहृत हुआ है। किन्तु संगीतरत्नाकर में (६.१०७७) उल्लेख है कि 'पावज' को हुडक्का का पर्याय माना जाता था। यह 'आवज' आतोद्य का ही अपभ्रंश प्रतीत होता है-आतोद्य आउज्ज आवज। अतः डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने 'आवज' को ढोल जैसा मढ़ा हुआ एक वाद्य माना है । लोक में बजाने वाले को 'प्रोजी' (आवज से) कहा गया है। तबला का विकास होते हो 'आवज' लोक संगीत का वाद्य बन कर रह गया। इसकी वनावट हुडक्का जैसी होती थी। इससे ज्ञात होता है कि उद्द्योतन के समय तक 'आतोद्य' स्वतन्त्र एक वाद्य के रूप में प्रचलित हो कुका था, जिसका उत्तरकालीन रूप ढोलक अथवा हुडक्का है।
तूर-कुवलयमाला में तूर शब्द का उल्लेख १६ वार हुआ है । ८ वार अन्य वाद्यों के साथ में तथा ८ बार अकेले तूर का ही उल्लेख है। इन उल्लेखों से ज्ञात होता है कि तूर निम्नोक्त अवसरों पर मुख्य रूप से बजाया जाता था:
१. जन्मोत्सव पर (१८.१२) २. विभिन्न यात्राओं के अवसर पर (६७.६, १३२.१०, १३५.२१,
१८१.३१)। ३. विवाहोत्सव पर (१७१.७, १८८.८) ४. प्रातःकाल में (१७३.१९, १६८.७,२४४.२) । ५. दीक्षा के समय (२०६.८) । ६. मांगलिक कार्यों के समय (१८७.१८)। १. घंटा-रव-गुंजाविय-वज्जिर-सुर-सेस-विसर-आउज्ज ।
आउज्ज-सद्द-संभम-सहसा-सुर-जुवइ-मुक्क हुंकारं ॥ ९६.१२. २. चतुर्विधमिदं वाद्यवादित्रातोद्यनामकम् , अमरकोश, १.१, ६. ३. भुयाल, गढ़वाली लोकगीत संग्रह, पृ० ३. ४. तूर १८.१२, ६७.६, १३२.१०, १३५.२१, आदि.