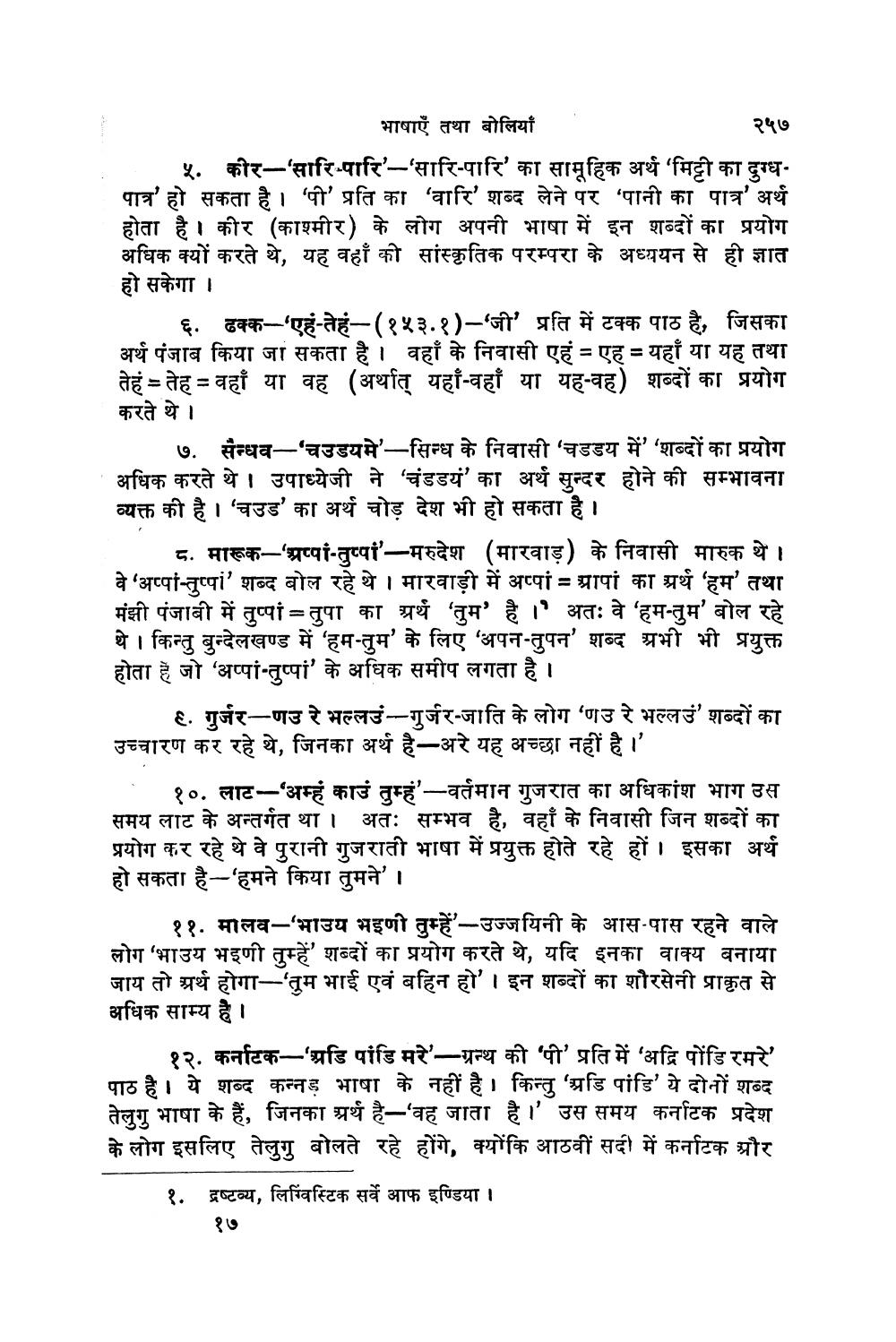________________
भाषाएँ तथा बोलियाँ
२५७
५. कीर - ' सारि पारि - ' सारि-पारि' का सामूहिक अर्थ 'मिट्टी का दुग्ध
पात्र' हो सकता है । 'पी' प्रति का 'वारि' शब्द लेने पर 'पानी का पात्र' अर्थ होता है । कीर (काश्मीर) के लोग अपनी भाषा में इन शब्दों का प्रयोग अधिक क्यों करते थे, यह वहाँ की सांस्कृतिक परम्परा के अध्ययन से ही ज्ञात हो सकेगा ।
६. ढक्क - - 'एहं- तेहं - (१५३.१ ) - 'जी' प्रति में टक्क पाठ है, जिसका अर्थ पंजाब किया जा सकता है । वहाँ के निवासी एहं = एह= यहाँ या यह तथा तेहं = तेह = वहाँ या वह ( अर्थात् यहाँ-वहाँ या यह वह ) शब्दों का प्रयोग करते थे ।
७. सैन्धव - 'चउडयमे' - सिन्ध के निवासी 'चडडय में' 'शब्दों का प्रयोग अधिक करते थे । उपाध्येजी ने 'चंडडयं' का अर्थ सुन्दर होने की सम्भावना व्यक्त की है । 'चउड' का अर्थ चोड़ देश भी हो सकता है ।
1
८. मारूक - 'प-तुप्पा' - मरुदेश ( मारवाड़) के निवासी मारुक थे । वे 'अप्पां-तुप्पां' शब्द बोल रहे थे । मारवाड़ी में अप्पां = प्रापां का अर्थ 'हम' तथा मंझी पंजाबी में तुप्पां = तुपा का अर्थ 'तुम' है ।' अतः वे 'हम-तुम' बोल रहे थे । किन्तु बुन्देलखण्ड में 'हम तुम' के लिए 'अपन-तुपन' शब्द अभी भी प्रयुक्त होता है जो 'अप्पां-तुप्पां' के अधिक समीप लगता है ।
६. गुर्जर - उ रे भल्लउं - गुर्जर जाति के लोग 'णउ रे भल्लउं' शब्दों का उच्चारण कर रहे थे, जिनका अर्थ है - अरे यह अच्छा नहीं है ।'
१०. लाट - ' अहं काउं तुम्हें' - वर्तमान गुजरात का अधिकांश भाग उस समय लाट के अन्तर्गत था । अतः सम्भव है, वहाँ के निवासी जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे थे वे पुरानी गुजराती भाषा में प्रयुक्त होते रहे हों । इसका अर्थ हो सकता है - 'हमने किया तुमने ' ।
११. मालव - ' भाउय भइणी तुम्हें' - उज्जयिनी के आस-पास रहने वाले लोग 'भाउय भइणी तुम्हें' शब्दों का प्रयोग करते थे, यदि इनका वाक्य बनाया जाय तो अर्थ होगा- 'तुम भाई एवं बहिन हो' । इन शब्दों का शौरसेनी प्राकृत अधिक साम्य है |
१२. कर्नाटक - 'डि पांडि मरे ' - ग्रन्थ की 'पी' प्रति में 'अद्रि पोंडि रमरे ' पाठ है । ये शब्द कन्नड़ भाषा के नहीं है । किन्तु 'डि पांडि' ये दोनों शब्द तेलुगु भाषा के हैं, जिनका अर्थ है - 'वह जाता है ।' उस समय कर्नाटक प्रदेश लोग इसलिए तेलुगु बोलते रहे होंगे, क्योंकि आठवीं सदी में कर्नाटक और
लिग्विस्टिक सर्वे आफ इण्डिया ।
१.
द्रष्टव्य,
१७