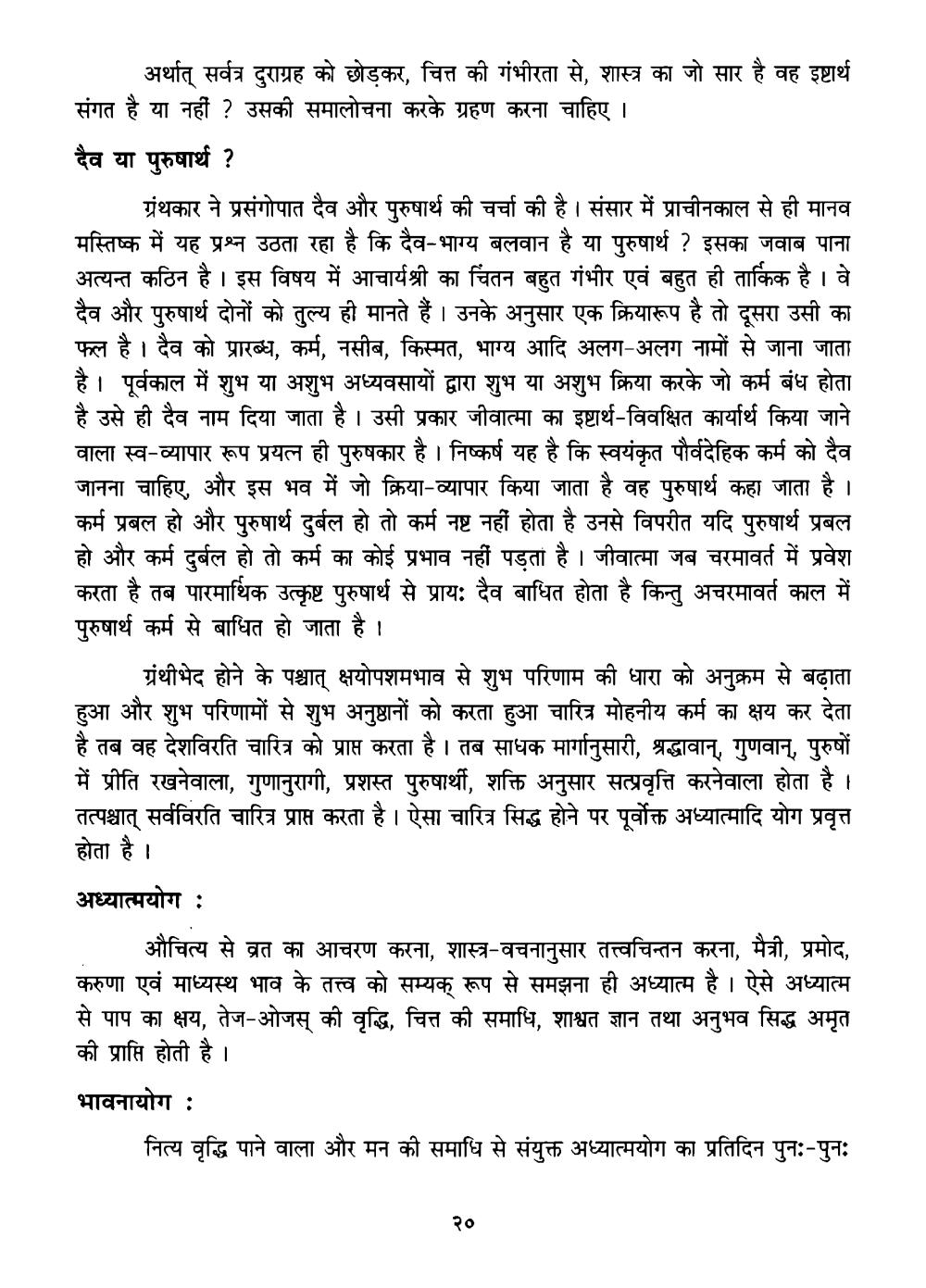________________
अर्थात् सर्वत्र दुराग्रह को छोड़कर, चित्त की गंभीरता से, शास्त्र का जो सार है वह इष्टार्थ संगत है या नहीं ? उसकी समालोचना करके ग्रहण करना चाहिए । दैव या पुरुषार्थ ?
ग्रंथकार ने प्रसंगोपात दैव और पुरुषार्थ की चर्चा की है। संसार में प्राचीनकाल से ही मानव मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता रहा है कि दैव-भाग्य बलवान है या पुरुषार्थ ? इसका जवाब पाना अत्यन्त कठिन है । इस विषय में आचार्यश्री का चिंतन बहुत गंभीर एवं बहुत ही ताकिक है । वे दैव और पुरुषार्थ दोनों को तुल्य ही मानते हैं। उनके अनुसार एक क्रियारूप है तो दूसरा उसी का फल है। दैव को प्रारब्ध, कर्म, नसीब, किस्मत, भाग्य आदि अलग-अलग नामों से जाना जाता है। पूर्वकाल में शुभ या अशुभ अध्यवसायों द्वारा शुभ या अशुभ क्रिया करके जो कर्म बंध होता है उसे ही दैव नाम दिया जाता है । उसी प्रकार जीवात्मा का इष्टार्थ-विवक्षित कार्यार्थ किया जाने वाला स्व-व्यापार रूप प्रयत्न ही पुरुषकार है। निष्कर्ष यह है कि स्वयंकृत पौर्वदेहिक कर्म को दैव जानना चाहिए, और इस भव में जो क्रिया-व्यापार किया जाता है वह पुरुषार्थ कहा जाता है । कर्म प्रबल हो और पुरुषार्थ दुर्बल हो तो कर्म नष्ट नहीं होता है उनसे विपरीत यदि पुरुषार्थ प्रबल हो और कर्म दुर्बल हो तो कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । जीवात्मा जब चरमावर्त में प्रवेश करता है तब पारमार्थिक उत्कृष्ट पुरुषार्थ से प्रायः दैव बाधित होता है किन्तु अचरमावर्त काल में पुरुषार्थ कर्म से बाधित हो जाता है ।
___ग्रंथीभेद होने के पश्चात् क्षयोपशमभाव से शुभ परिणाम की धारा को अनुक्रम से बढ़ाता हुआ और शुभ परिणामों से शुभ अनुष्ठानों को करता हुआ चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय कर देता है तब वह देशविरति चारित्र को प्राप्त करता है । तब साधक मार्गानुसारी, श्रद्धावान्, गुणवान्, पुरुषों में प्रीति रखनेवाला, गुणानुरागी, प्रशस्त पुरुषार्थी, शक्ति अनुसार सत्प्रवृत्ति करनेवाला होता है । तत्पश्चात् सर्वविरति चारित्र प्राप्त करता है। ऐसा चारित्र सिद्ध होने पर पूर्वोक्त अध्यात्मादि योग प्रवृत्त होता है। अध्यात्मयोग :
औचित्य से व्रत का आचरण करना, शास्त्र-वचनानुसार तत्त्वचिन्तन करना, मैत्री, प्रमोद, करुणा एवं माध्यस्थ भाव के तत्त्व को सम्यक् रूप से समझना ही अध्यात्म है । ऐसे अध्यात्म से पाप का क्षय, तेज-ओजस् की वृद्धि, चित्त की समाधि, शाश्वत ज्ञान तथा अनुभव सिद्ध अमृत की प्राप्ति होती है। भावनायोग :
नित्य वृद्धि पाने वाला और मन की समाधि से संयुक्त अध्यात्मयोग का प्रतिदिन पुनः पुनः