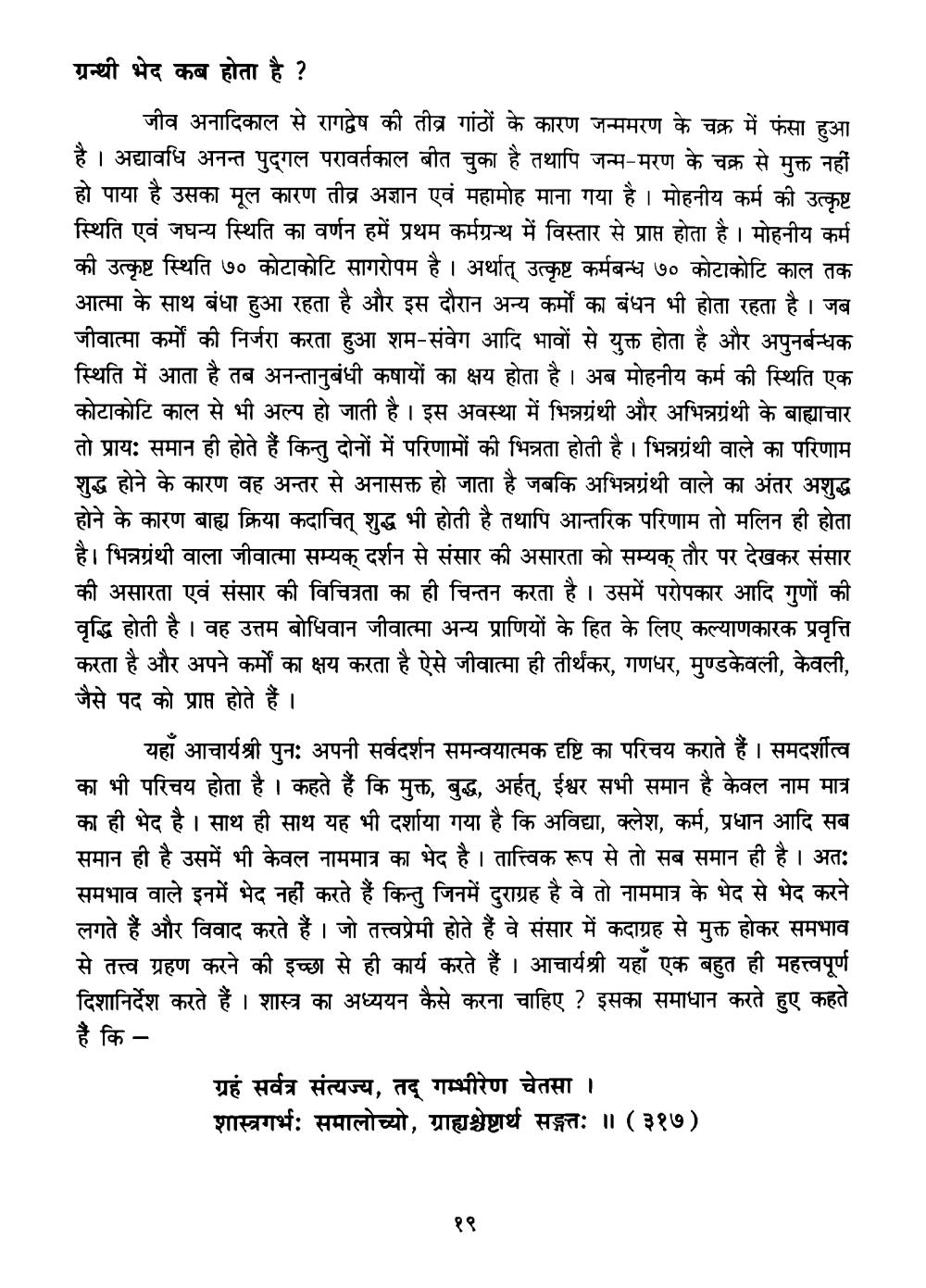________________
ग्रन्थी भेद कब होता है ?
जीव अनादिकाल से रागद्वेष की तीव्र गांठों के कारण जन्ममरण के चक्र में फंसा हुआ है। अद्यावधि अनन्त पुद्गल परावर्तकाल बीत चुका है तथापि जन्म-मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो पाया है उसका मूल कारण तीव्र अज्ञान एवं महामोह माना गया है । मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति एवं जघन्य स्थिति का वर्णन हमें प्रथम कर्मग्रन्थ में विस्तार से प्राप्त होता है। मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति ७० कोटाकोटि सागरोपम है । अर्थात् उत्कृष्ट कर्मबन्ध ७० कोटाकोटि काल तक आत्मा के साथ बंधा हुआ रहता है और इस दौरान अन्य कर्मों का बंधन भी होता रहता है । जब जीवात्मा कर्मों की निर्जरा करता हुआ शम-संवेग आदि भावों से युक्त होता है और अपुनर्बन्धक स्थिति में आता है तब अनन्तानुबंधी कषायों का क्षय होता है । अब मोहनीय कर्म की स्थिति एक कोटाकोटि काल से भी अल्प हो जाती है । इस अवस्था में भिन्नग्रंथी और अभिन्नग्रंथी के बाह्याचार तो प्रायः समान ही होते हैं किन्तु दोनों में परिणामों की भिन्नता होती है। भिन्नग्रंथी वाले का परिणाम शुद्ध होने के कारण वह अन्तर से अनासक्त हो जाता है जबकि अभिन्नग्रंथी वाले का अंतर अशुद्ध होने के कारण बाह्य क्रिया कदाचित् शुद्ध भी होती है तथापि आन्तरिक परिणाम तो मलिन ही होता है। भिन्नग्रंथी वाला जीवात्मा सम्यक् दर्शन से संसार की असारता को सम्यक् तौर पर देखकर संसार की असारता एवं संसार की विचित्रता का ही चिन्तन करता है। उसमें परोपकार आदि गुणों की वृद्धि होती है । वह उत्तम बोधिवान जीवात्मा अन्य प्राणियों के हित के लिए कल्याणकारक प्रवृत्ति करता है और अपने कर्मों का क्षय करता है ऐसे जीवात्मा ही तीर्थंकर, गणधर, मुण्डकेवली, केवली, जैसे पद को प्राप्त होते हैं।
___ यहाँ आचार्यश्री पुनः अपनी सर्वदर्शन समन्वयात्मक दृष्टि का परिचय कराते हैं । समदर्शीत्व का भी परिचय होता है । कहते हैं कि मुक्त, बुद्ध, अर्हत्, ईश्वर सभी समान है केवल नाम मात्र का ही भेद है । साथ ही साथ यह भी दर्शाया गया है कि अविद्या, क्लेश, कर्म, प्रधान आदि सब समान ही है उसमें भी केवल नाममात्र का भेद है । तात्त्विक रूप से तो सब समान ही है। अतः समभाव वाले इनमें भेद नहीं करते हैं किन्तु जिनमें दुराग्रह है वे तो नाममात्र के भेद से भेद करने लगते हैं और विवाद करते हैं । जो तत्त्वप्रेमी होते हैं वे संसार में कदाग्रह से मुक्त होकर समभाव से तत्त्व ग्रहण करने की इच्छा से ही कार्य करते हैं । आचार्यश्री यहाँ एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण दिशानिर्देश करते हैं । शास्त्र का अध्ययन कैसे करना चाहिए ? इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि -
ग्रहं सर्वत्र संत्यज्य, तद् गम्भीरेण चेतसा । शास्त्रगर्भः समालोच्यो, ग्राह्यचेष्टार्थ सङ्गतः ॥ (३१७)