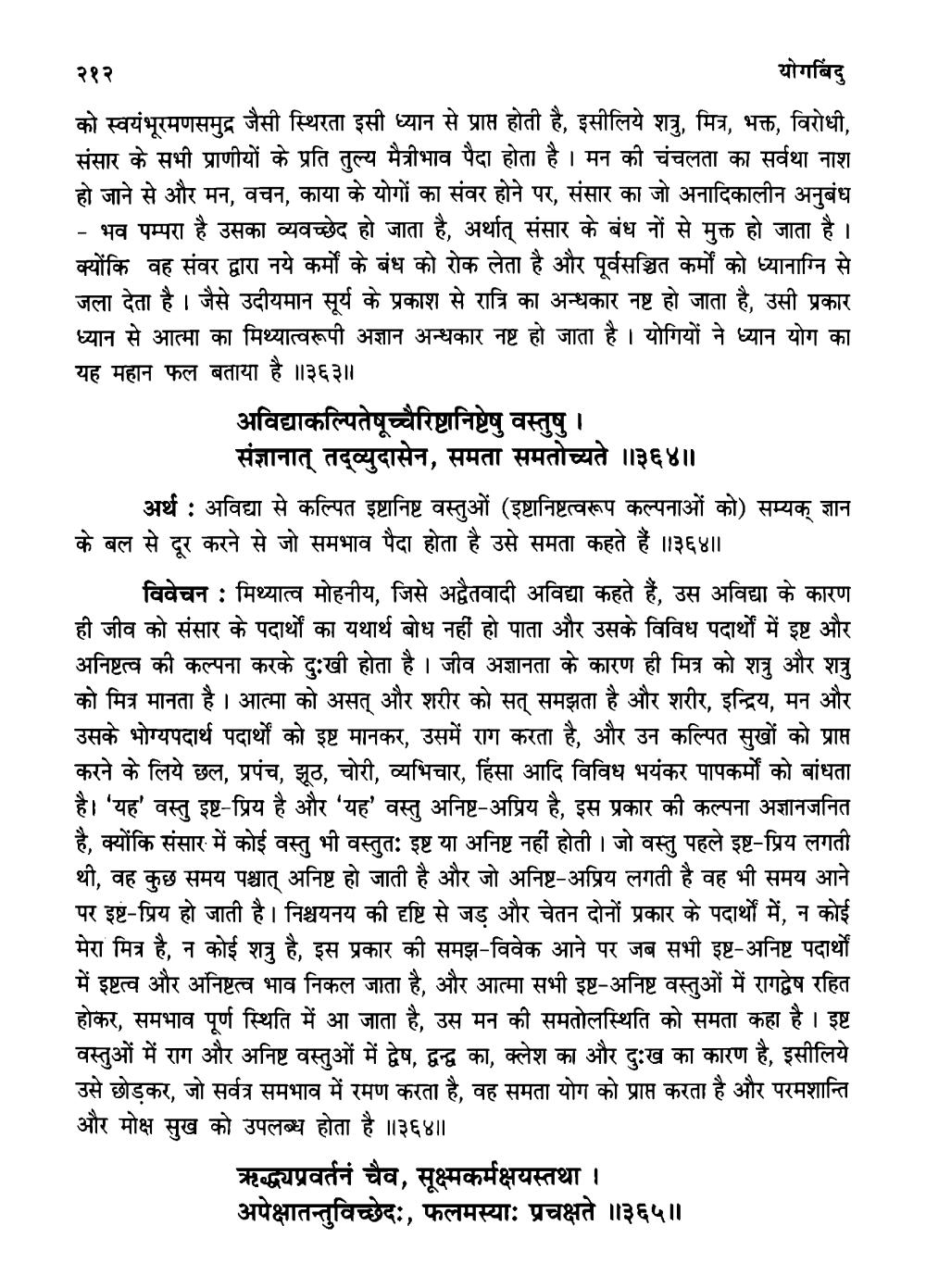________________ योगबिंदु 212 को स्वयंभूरमणसमुद्र जैसी स्थिरता इसी ध्यान से प्राप्त होती है, इसीलिये शत्रु, मित्र, भक्त, विरोधी, संसार के सभी प्राणीयों के प्रति तुल्य मैत्रीभाव पैदा होता है। मन की चंचलता का सर्वथा नाश हो जाने से और मन, वचन, काया के योगों का संवर होने पर, संसार का जो अनादिकालीन अनुबंध - भव पम्परा है उसका व्यवच्छेद हो जाता है, अर्थात् संसार के बंध नों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि वह संवर द्वारा नये कर्मों के बंध को रोक लेता है और पूर्वसञ्चित कर्मों को ध्यानाग्नि से जला देता है / जैसे उदीयमान सूर्य के प्रकाश से रात्रि का अन्धकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ध्यान से आत्मा का मिथ्यात्वरूपी अज्ञान अन्धकार नष्ट हो जाता है। योगियों ने ध्यान योग का यह महान फल बताया है // 363 // अविद्याकल्पितेषूच्चैरिष्टानिष्टेषु वस्तुषु / संज्ञानात् तद्व्युदासेन, समता समतोच्यते // 364 // अर्थ : अविद्या से कल्पित इष्टानिष्ट वस्तुओं (इष्टानिष्टत्वरूप कल्पनाओं को) सम्यक् ज्ञान के बल से दूर करने से जो समभाव पैदा होता है उसे समता कहते हैं // 364 / / विवेचन : मिथ्यात्व मोहनीय, जिसे अद्वैतवादी अविद्या कहते हैं, उस अविद्या के कारण ही जीव को संसार के पदार्थों का यथार्थ बोध नहीं हो पाता और उसके विविध पदार्थों में इष्ट और अनिष्टत्व की कल्पना करके दुःखी होता है / जीव अज्ञानता के कारण ही मित्र को शत्रु और शत्रु को मित्र मानता है। आत्मा को असत् और शरीर को सत् समझता है और शरीर, इन्द्रिय, मन और उसके भोग्यपदार्थ पदार्थों को इष्ट मानकर, उसमें राग करता है, और उन कल्पित सुखों को प्राप्त करने के लिये छल, प्रपंच, झूठ, चोरी, व्यभिचार, हिंसा आदि विविध भयंकर पापकर्मों को बांधता है। 'यह' वस्तु इष्ट-प्रिय है और 'यह' वस्तु अनिष्ट-अप्रिय है, इस प्रकार की कल्पना अज्ञानजनित है, क्योंकि संसार में कोई वस्तु भी वस्तुतः इष्ट या अनिष्ट नहीं होती। जो वस्तु पहले इष्ट-प्रिय लगती थी, वह कुछ समय पश्चात् अनिष्ट हो जाती है और जो अनिष्ट-अप्रिय लगती है वह भी समय आने पर इष्ट-प्रिय हो जाती है। निश्चयनय की दृष्टि से जड़ और चेतन दोनों प्रकार के पदार्थों में, न कोई मेरा मित्र है, न कोई शत्रु है, इस प्रकार की समझ-विवेक आने पर जब सभी इष्ट-अनिष्ट पदार्थों में इष्टत्व और अनिष्टत्व भाव निकल जाता है, और आत्मा सभी इष्ट-अनिष्ट वस्तुओं में रागद्वेष रहित होकर, समभाव पूर्ण स्थिति में आ जाता है, उस मन की समतोलस्थिति को समता कहा है / इष्ट वस्तुओं में राग और अनिष्ट वस्तुओं में द्वेष, द्वन्द्व का, क्लेश का और दुःख का कारण है, इसीलिये उसे छोड़कर, जो सर्वत्र समभाव में रमण करता है, वह समता योग को प्राप्त करता है और परमशान्ति और मोक्ष सुख को उपलब्ध होता है // 364 / / ऋद्ध्यप्रवर्तनं चैव, सूक्ष्मकर्मक्षयस्तथा / अपेक्षातन्तुविच्छेदः, फलमस्याः प्रचक्षते // 365 //