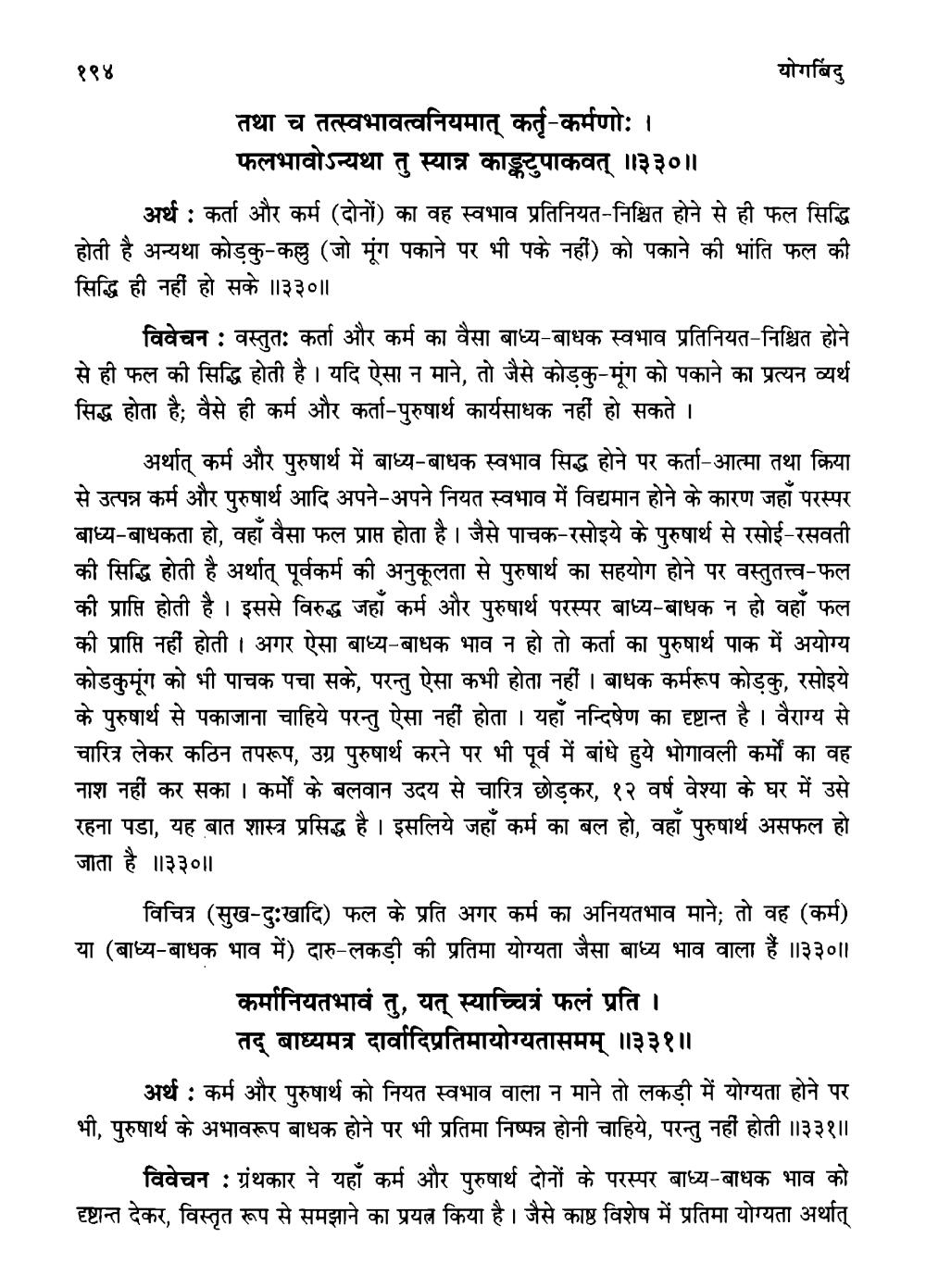________________ 194 योगबिंदु तथा च तत्स्वभावत्वनियमात् कर्तृ-कर्मणोः / फलभावोऽन्यथा तु स्यान्न काङ्कटुपाकवत् // 330 // अर्थ : कर्ता और कर्म (दोनों) का वह स्वभाव प्रतिनियत-निश्चित होने से ही फल सिद्धि होती है अन्यथा कोड़कु-कल्लु (जो मूंग पकाने पर भी पके नहीं) को पकाने की भांति फल की सिद्धि ही नहीं हो सके // 330 // विवेचन : वस्तुतः कर्ता और कर्म का वैसा बाध्य-बाधक स्वभाव प्रतिनियत-निश्चित होने से ही फल की सिद्धि होती है। यदि ऐसा न माने, तो जैसे कोड़कु-मूंग को पकाने का प्रत्यन व्यर्थ सिद्ध होता है; वैसे ही कर्म और कर्ता-पुरुषार्थ कार्यसाधक नहीं हो सकते / ___ अर्थात् कर्म और पुरुषार्थ में बाध्य-बाधक स्वभाव सिद्ध होने पर कर्ता-आत्मा तथा क्रिया से उत्पन्न कर्म और पुरुषार्थ आदि अपने-अपने नियत स्वभाव में विद्यमान होने के कारण जहाँ परस्पर बाध्य-बाधकता हो, वहाँ वैसा फल प्राप्त होता है। जैसे पाचक-रसोइये के पुरुषार्थ से रसोई-रसवती की सिद्धि होती है अर्थात् पूर्वकर्म की अनुकूलता से पुरुषार्थ का सहयोग होने पर वस्तुतत्त्व-फल की प्राप्ति होती है / इससे विरुद्ध जहाँ कर्म और पुरुषार्थ परस्पर बाध्य-बाधक न हो वहाँ फल की प्राप्ति नहीं होती। अगर ऐसा बाध्य-बाधक भाव न हो तो कर्ता का पुरुषार्थ पाक में अयोग्य कोडकुमूंग को भी पाचक पचा सके, परन्तु ऐसा कभी होता नहीं / बाधक कर्मरूप कोड़कु, रसोइये के पुरुषार्थ से पकाजाना चाहिये परन्तु ऐसा नहीं होता / यहा नन्दिषेण का दृष्टान्त है। वैराग्य से चारित्र लेकर कठिन तपरूप, उग्र पुरुषार्थ करने पर भी पूर्व में बांधे हुये भोगावली कर्मों का वह नाश नहीं कर सका / कर्मों के बलवान उदय से चारित्र छोड़कर, 12 वर्ष वेश्या के घर में उसे रहना पडा, यह बात शास्त्र प्रसिद्ध है / इसलिये जहाँ कर्म का बल हो, वहाँ पुरुषार्थ असफल हो जाता है // 330 // विचित्र (सुख-दुःखादि) फल के प्रति अगर कर्म का अनियतभाव माने; तो वह (कर्म) या (बाध्य-बाधक भाव में) दारु-लकड़ी की प्रतिमा योग्यता जैसा बाध्य भाव वाला हैं // 330 // कर्मानियतभावं तु, यत् स्याच्चित्रं फलं प्रति / तद् बाध्यमत्र दादिप्रतिमायोग्यतासमम् // 331 // अर्थ : कर्म और पुरुषार्थ को नियत स्वभाव वाला न माने तो लकड़ी में योग्यता होने पर भी, पुरुषार्थ के अभावरूप बाधक होने पर भी प्रतिमा निष्पन्न होनी चाहिये, परन्तु नहीं होती // 331 / / विवेचन : ग्रंथकार ने यहाँ कर्म और पुरुषार्थ दोनों के परस्पर बाध्य-बाधक भाव को दृष्टान्त देकर, विस्तृत रूप से समझाने का प्रयत्न किया है। जैसे काष्ठ विशेष में प्रतिमा योग्यता अर्थात्