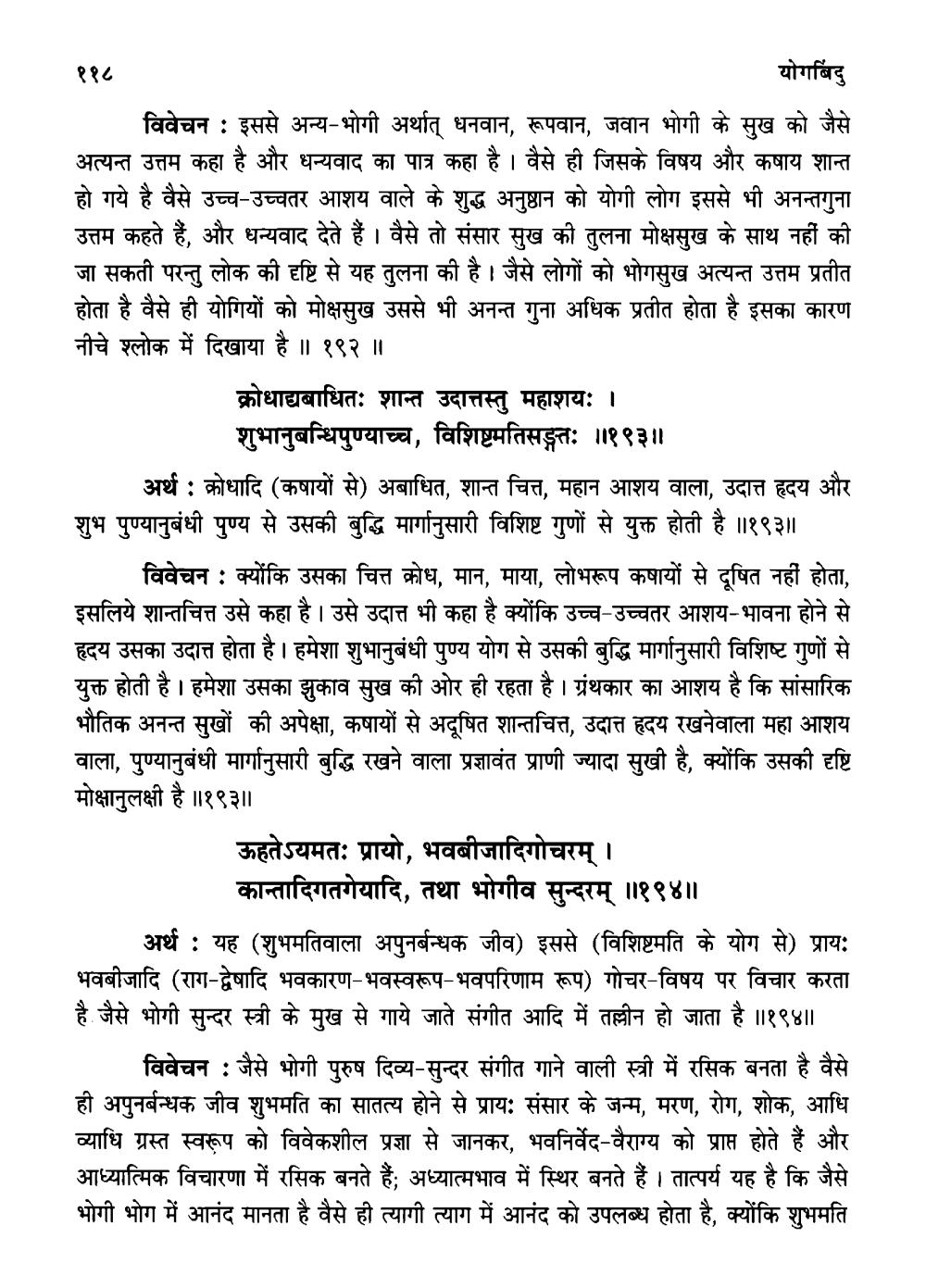________________ 118 योगबिंदु विवेचन : इससे अन्य-भोगी अर्थात् धनवान, रूपवान, जवान भोगी के सुख को जैसे अत्यन्त उत्तम कहा है और धन्यवाद का पात्र कहा है / वैसे ही जिसके विषय और कषाय शान्त हो गये है वैसे उच्च-उच्चतर आशय वाले के शुद्ध अनुष्ठान को योगी लोग इससे भी अनन्तगुना उत्तम कहते हैं, और धन्यवाद देते हैं। वैसे तो संसार सुख की तुलना मोक्षसुख के साथ नहीं की जा सकती परन्तु लोक की दृष्टि से यह तुलना की है। जैसे लोगों को भोगसुख अत्यन्त उत्तम प्रतीत होता है वैसे ही योगियों को मोक्षसुख उससे भी अनन्त गुना अधिक प्रतीत होता है इसका कारण नीचे श्लोक में दिखाया है || 192 / / क्रोधाद्यबाधितः शान्त उदात्तस्तु महाशयः / शुभानुबन्धिपुण्याच्च, विशिष्टमतिसङ्गतः // 193 // अर्थ : क्रोधादि (कषायों से) अबाधित, शान्त चित्त, महान आशय वाला, उदात्त हृदय और शुभ पुण्यानुबंधी पुण्य से उसकी बुद्धि मार्गानुसारी विशिष्ट गुणों से युक्त होती है // 193 // विवेचन : क्योंकि उसका चित्त क्रोध, मान, माया, लोभरूप कषायों से दूषित नहीं होता, इसलिये शान्तचित्त उसे कहा है। उसे उदात्त भी कहा है क्योंकि उच्च-उच्चतर आशय-भावना होने से हृदय उसका उदात्त होता है। हमेशा शुभानुबंधी पुण्य योग से उसकी बुद्धि मार्गानुसारी विशिष्ट गुणों से युक्त होती है। हमेशा उसका झुकाव सुख की ओर ही रहता है / ग्रंथकार का आशय है कि सांसारिक भौतिक अनन्त सुखों की अपेक्षा, कषायों से अदूषित शान्तचित्त, उदात्त हृदय रखनेवाला महा आशय वाला, पुण्यानुबंधी मार्गानुसारी बुद्धि रखने वाला प्रज्ञावंत प्राणी ज्यादा सुखी है, क्योंकि उसकी दृष्टि मोक्षानुलक्षी है // 193 // ऊहतेऽयमतः प्रायो, भवबीजादिगोचरम् / कान्तादिगतगेयादि, तथा भोगीव सुन्दरम् // 194 // अर्थ : यह (शुभमतिवाला अपुनर्बन्धक जीव) इससे (विशिष्टमति के योग से) प्रायः भवबीजादि (राग-द्वेषादि भवकारण-भवस्वरूप-भवपरिणाम रूप) गोचर-विषय पर विचार करता है जैसे भोगी सुन्दर स्त्री के मुख से गाये जाते संगीत आदि में तल्लीन हो जाता है ||194|| विवेचन : जैसे भोगी पुरुष दिव्य-सुन्दर संगीत गाने वाली स्त्री में रसिक बनता है वैसे ही अपुनर्बन्धक जीव शुभमति का सातत्य होने से प्रायः संसार के जन्म, मरण, रोग, शोक, आधि व्याधि ग्रस्त स्वरूप को विवेकशील प्रज्ञा से जानकर, भवनिर्वेद-वैराग्य को प्राप्त होते हैं और आध्यात्मिक विचारणा में रसिक बनते हैं; अध्यात्मभाव में स्थिर बनते हैं। तात्पर्य यह है कि जैसे भोगी भोग में आनंद मानता है वैसे ही त्यागी त्याग में आनंद को उपलब्ध होता है, क्योंकि शुभमति