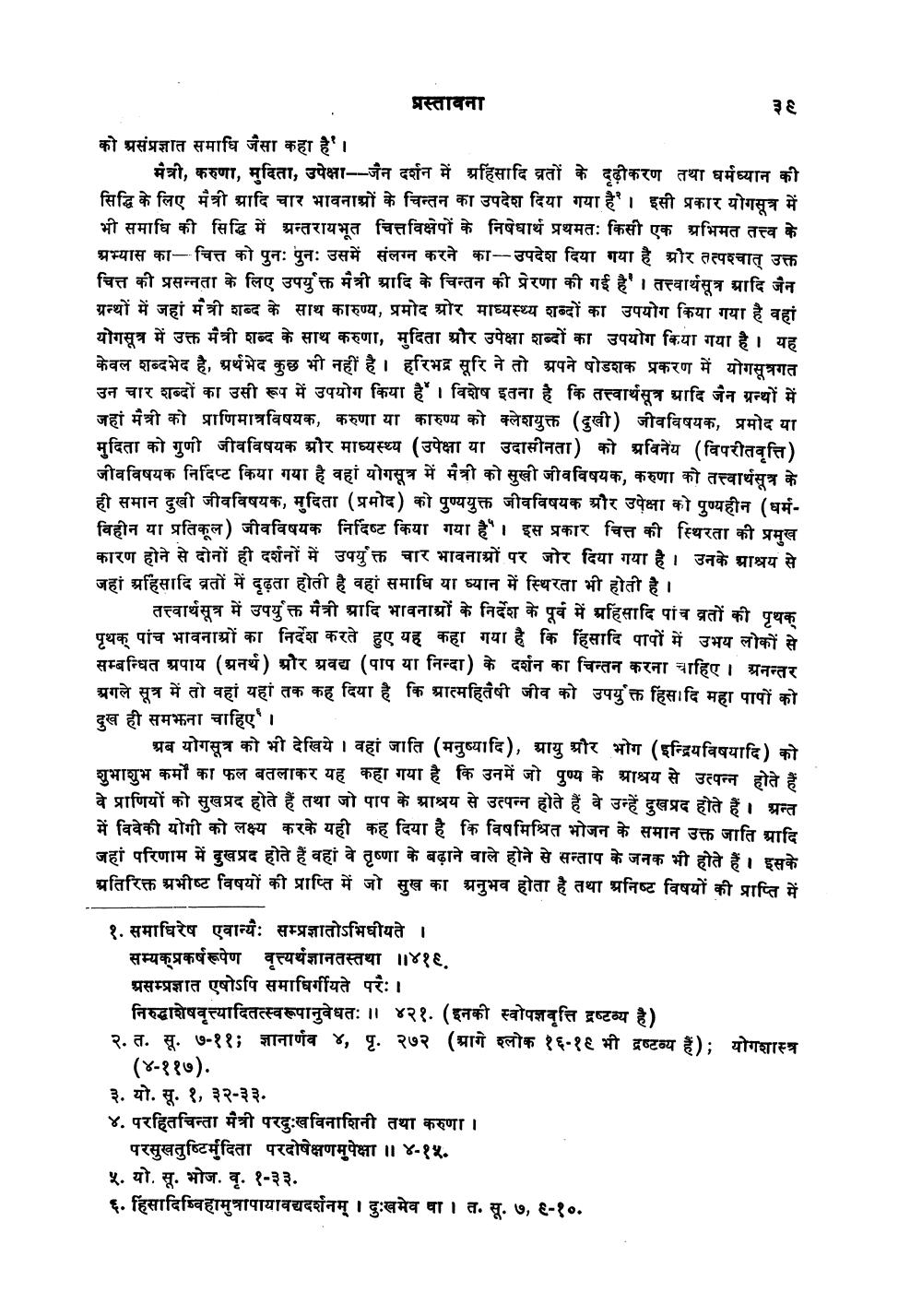________________
प्रस्तावना
को प्रसंप्रज्ञात समाधि जैसा कहा है ' ।
मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा -- जैन दर्शन में अहिंसादि व्रतों के दृढ़ीकरण तथा धर्मध्यान की सिद्धि के लिए मंत्री आदि चार भावनाओं के चिन्तन का उपदेश दिया गया है। इसी प्रकार योगसूत्र में भी समाधि की सिद्धि में अन्तरायभूत चित्तविक्षेपों के निषेधार्थ प्रथमतः किसी एक अभिमत तत्त्व के अभ्यास का — चित्त को पुनः पुनः उसमें संलग्न करने का उपदेश दिया गया है और तत्पश्चात् उक्त चित्त की प्रसन्नता के लिए उपर्युक्त मंत्री प्रादि के चिन्तन की प्रेरणा की गई है ' । तत्त्वार्थसूत्र प्रादि जैन ग्रन्थों में जहां मंत्री शब्द के साथ कारुण्य, प्रमोद र माध्यस्थ्य शब्दों का उपयोग किया गया है वहां योगसूत्र में उक्त मैत्री शब्द के साथ करुणा, मुदिता और उपेक्षा शब्दों का उपयोग किया गया है । यह केवल शब्दभेद है, अर्थभेद कुछ भी नहीं है । हरिभद्र सूरि ने तो अपने षोडशक प्रकरण में योगसूत्रगत उन चार शब्दों का उसी रूप में उपयोग किया है। विशेष इतना है कि तत्त्वार्थसूत्र आदि जैन ग्रन्थों में जहां मंत्री को प्राणिमात्रविषयक, करुणा या कारुण्य को क्लेशयुक्त (दुखी) जीवविषयक, प्रमोद या मुदिता को गुणी जीवविषयक और माध्यस्थ्य ( उपेक्षा या उदासीनता) को अविनेय (विपरीतवृत्ति ) जीवविषयक निर्दिष्ट किया गया है वहां योगसूत्र में मैत्री को सुखी जीवविषयक, करुणा को तत्त्वार्थसूत्र के ही समान दुखी जीवविषयक, मुदिता ( प्रमोद) को पुण्ययुक्त जीवविषयक और उपेक्षा को पुण्यहीन ( धर्म - विहीन या प्रतिकूल ) जीवविषयक निर्दिष्ट किया गया है। इस प्रकार चित्त की स्थिरता की प्रमुख कारण होने से दोनों ही दर्शनों में उपर्युक्त चार भावनाओं पर जोर दिया गया है। उनके प्रश्रय से जहां अहिंसादि व्रतों में दृढ़ता होती है वहां समाधि या ध्यान में स्थिरता भी होती है ।
तत्त्वार्थसूत्र में उपर्युक्त मैत्री आदि भावनाओं के निर्देश के पूर्व में अहिंसादि पांच व्रतों की पृथक् पृथक् पांच भावनाओं का निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि हिंसादि पापों में उभय लोकों से सम्बन्धित अपाय ( अनर्थ ) और अवद्य ( पाप या निन्दा ) के दर्शन का चिन्तन करना चाहिए। अनन्तर अगले सूत्र में तो वहां यहां तक कह दिया है कि श्रात्महितैषी जीव को उपर्युक्त हिंसादि महा पापों को दुख ही समझना चाहिए' ।
अब योगसूत्र को भी देखिये । वहां जाति ( मनुष्यादि), आयु और भोग (इन्द्रियविषयादि) को कहा गया है कि उनमें जो पुण्य के आश्रय से उत्पन्न होते हैं पाप के श्राश्रय से उत्पन्न होते हैं वे उन्हें दुखप्रद होते हैं । अन्त कह दिया है कि विषमिश्रित भोजन के समान उक्त जाति आदि वाले होने से सन्ताप के जनक भी होते हैं । इसके अनुभव होता है तथा अनिष्ट विषयों की प्राप्ति में
शुभाशुभ कर्मों का फल बतलाकर यह वे प्राणियों को सुखप्रद होते हैं तथा जो में विवेकी योगी को लक्ष्य करके यही जहां परिणाम में दुखप्रद होते हैं वहां वे तृष्णा के बढ़ाने अतिरिक्त अभीष्ट विषयों की प्राप्ति में जो सुख का
(४-११७).
३. यो. सू. १, ३२-३३.
१. समाधिरेष एवान्यैः सम्प्रज्ञातोऽभिधीयते । सम्यक्प्रकर्षरूपेण वृत्त्यर्थज्ञानतस्तथा ॥४१६. सम्प्रज्ञात एषोऽपि समाधिर्गीयते परैः ।
निरुद्धाशेषवृत्त्यादितत्स्वरूपानुवेधतः ।। ४२१. ( इनकी स्वोपज्ञवृत्ति द्रष्टव्य है )
२. त. सू. ७-११; ज्ञानार्णव ४, पृ. २७२ (आगे श्लोक १६-१६ भी द्रष्टव्य हैं ) ; योगशास्त्र
३६
४. परहितचिन्ता मंत्री परदुःखविनाशिनी तथा करुणा ।
परसुखतुष्टिर्मुदिता परदोषेक्षणमुपेक्षा । ४- १५.
५. यो. सू. भोज. वृ. १-३३.
६. हिंसादिष्विहामुत्रापायावद्यदर्शनम् । दुःखमेव वा । त. सू. ७, ६ १०.