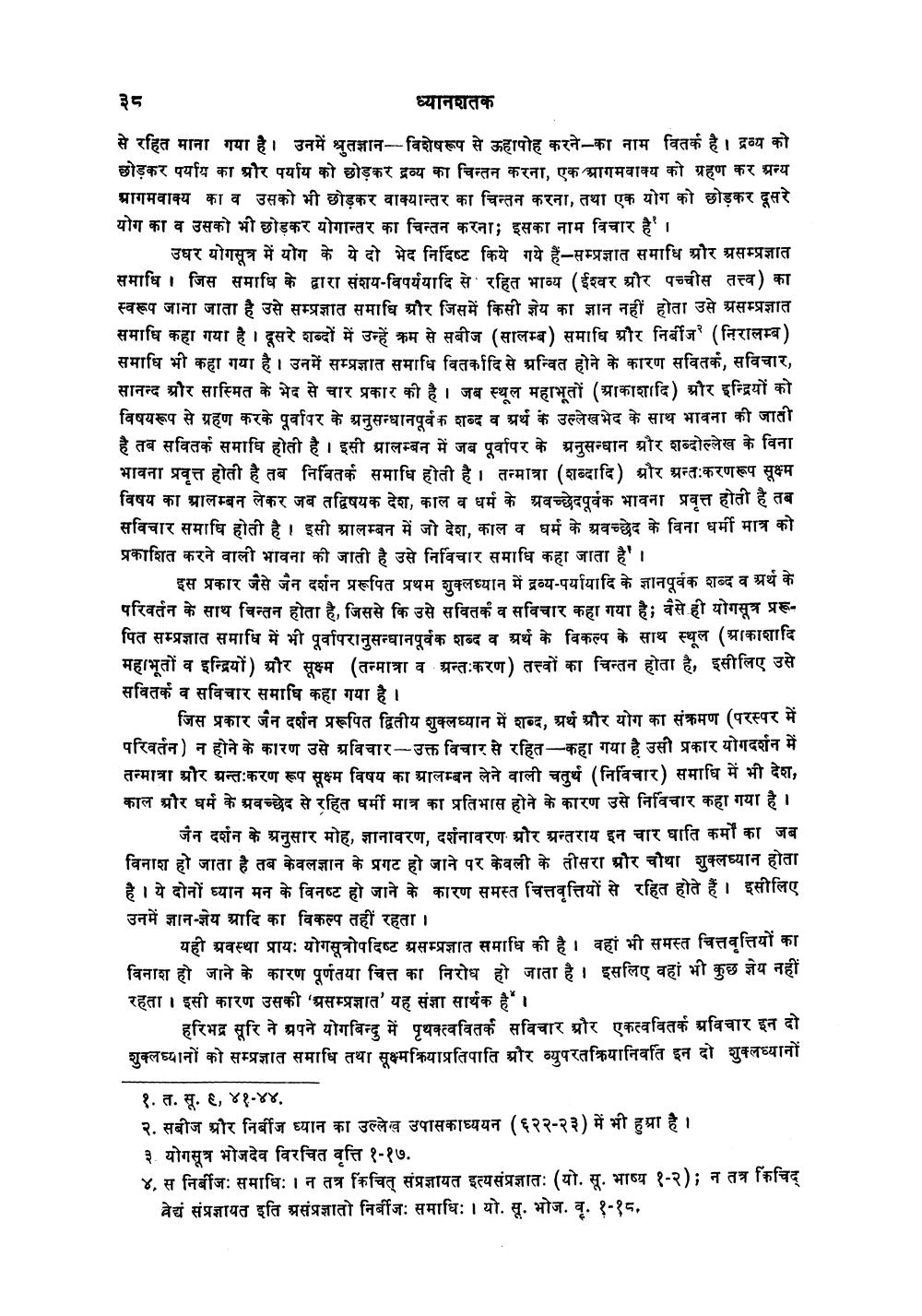________________
३८
ध्यानशतक
से रहित माना गया है। उनमें श्रुतज्ञान-विशेषरूप से ऊहापोह करने का नाम वितर्क है। द्रव्य को छोड़कर पर्याय का और पर्याय को छोड़कर द्रव्य का चिन्तन करना, एक पागमवाक्य को ग्रहण कर अन्य मागमवाक्य का व उसको भी छोड़कर वाक्यान्तर का चिन्तन करना, तथा एक योग को छोड़कर दूसरे योग का व उसको भी छोड़कर योगान्तर का चिन्तन करना; इसका नाम विचार है।
उधर योगसूत्र में योग के ये दो भेद निर्दिष्ट किये गये हैं-सम्प्रज्ञात समाधि और असम्प्रज्ञात समाधि । जिस समाधि के द्वारा संशय-विपर्ययादि से रहित भाव्य (ईश्वर और पच्चीस तत्त्व) का स्वरूप जाना जाता है उसे सम्प्रज्ञात समाधि और जिसमें किसी ज्ञेय का ज्ञान नहीं होता उसे असम्प्रज्ञात समाधि कहा गया है। दूसरे शब्दों में उन्हें क्रम से सबीज (सालम्ब) समाधि और निर्बीज' (निरालम्ब) समाधि भी कहा गया है। उनमें सम्प्रज्ञात समाधि वितर्कादि से अन्वित होने के कारण सवितर्क, सविचार, सानन्द और सास्मित के भेद से चार प्रकार की है। जब स्थूल महाभूतों (आकाशादि) और इन्द्रियों को विषयरूप से ग्रहण करके पूर्वापर के अनुसन्धानपूर्वक शब्द व अर्थ के उल्लेखभेद के साथ भावना की जाती है तब सवितर्क समाधि होती है। इसी पालम्बन में जब पूर्वापर के अनुसन्धान और शब्दोल्लेख के विना भावना प्रवृत्त होती है तब निर्वितर्क समाधि होती है। तन्मात्रा (शब्दादि) और अन्तःकरणरूप सूक्ष्म विषय का पालम्बन लेकर जब तद्विषयक देश, काल व धर्म के अवच्छेदपूर्वक भावना प्रवृत्त होती है तब सविचार समाधि होती है। इसी पालम्बन में जो देश, काल व धर्म के अवच्छेद के विना धर्मी मात्र को प्रकाशित करने वाली भावना की जाती है उसे निर्विचार समाधि कहा जाता है।
इस प्रकार जैसे जैन दर्शन प्ररूपित प्रथम शुक्लध्यान में द्रव्य-पर्यायादि के ज्ञानपूर्वक शब्द व अर्थ के परिवर्तन के साथ चिन्तन होता है, जिससे कि उसे सवितर्क व सविचार कहा गया है। वैसे ही योगसूत्र प्ररूपित सम्प्रज्ञात समाधि में भी पूर्वापरानुसन्धानपूर्वक शब्द व अर्थ के विकल्प के साथ स्थूल (आकाशादि महाभूतों व इन्द्रियों) और सूक्ष्म (तन्मात्रा व अन्तःकरण) तत्त्वों का चिन्तन होता है, इसीलिए उसे सवितर्क व सविचार समाधि कहा गया है।
जिस प्रकार जैन दर्शन प्ररूपित द्वितीय शुक्लध्यान में शब्द, अर्थ और योग का संक्रमण (परस्पर में परिवर्तन) न होने के कारण उसे अविचार-उक्त विचार से रहित कहा गया है उसी प्रकार योगदर्शन में तन्मात्रा और अन्तःकरण रूप सूक्ष्म विषय का पालम्बन लेने वाली चतुर्थ (निर्विचार) समाधि में भी देश, काल और धर्म के प्रवच्छेद से रहित धर्मी मात्र का प्रतिभास होने के कारण उसे निर्विचार कहा गया है।
जैन दर्शन के अनुसार मोह, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन चार घाति कर्मों का जब विनाश हो जाता है तब केवलज्ञान के प्रगट हो जाने पर केवली के तीसरा और चौथा शुक्लध्यान होता है। ये दोनों ध्यान मन के विनष्ट हो जाने के कारण समस्त चित्तवत्तियों से रहित होते हैं। इसीलिए उनमें ज्ञान-ज्ञेय आदि का विकल्प तहीं रहता।
यही अवस्था प्रायः योगसूत्रोपदिष्ट असम्प्रज्ञात समाधि की है। वहां भी समस्त चित्तवृत्तियों का विनाश हो जाने के कारण पूर्णतया चित्त का निरोध हो जाता है। इसलिए वहां भी कुछ ज्ञेय नहीं रहता। इसी कारण उसकी 'असम्प्रज्ञात' यह संज्ञा सार्थक है।
हरिभद्र सूरि ने अपने योगबिन्दू में पृथक्त्ववितर्क सविचार और एकत्ववितर्क अविचार इन दो शुक्लध्यानों को सम्प्रज्ञात समाधि तथा सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति और व्यूपरतक्रियानिवति इन दो शुक्लध्यानों
१. त. सू. ६, ४१-४४. २. सबीज और निर्बीज ध्यान का उल्लेख उपासकाध्ययन (६२२-२३) में भी हुआ है। ३. योगसूत्र भोजदेव विरचित वृत्ति १-१७. ४. स निर्बीजः समाधिः । न तत्र किंचित् संप्रज्ञायत इत्यसंप्रज्ञातः (यो. सू. भाष्य १-२); न तत्र किंचिद्
वेद्यं संप्रज्ञायत इति असंप्रज्ञातो निर्बीजः समाधिः । यो. सू. भोज. वृ. १-१८,