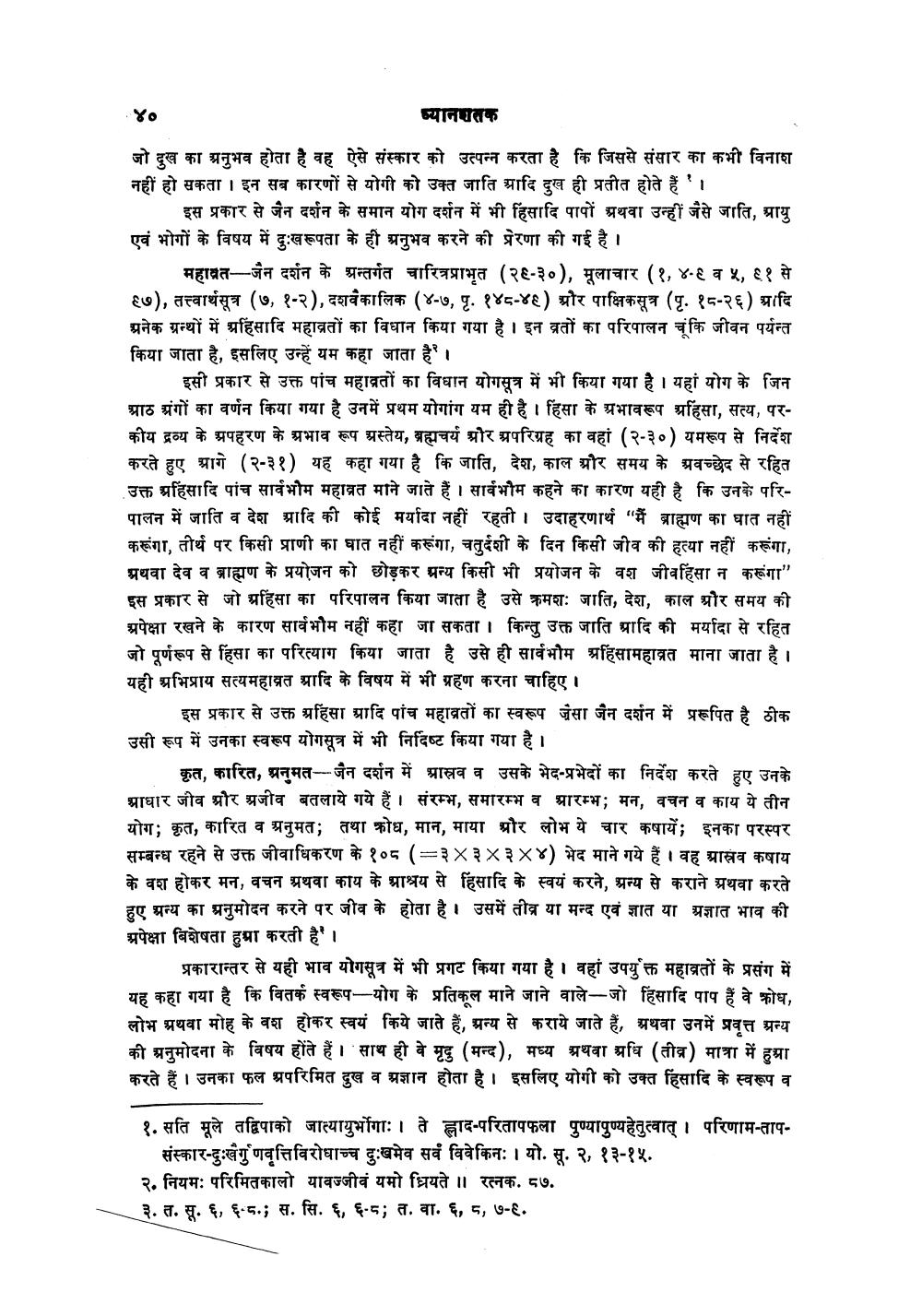________________
ध्यानशतक
जो
दुख का अनुभव होता है वह ऐसे संस्कार को उत्पन्न करता है कि जिससे संसार का कभी विनाश नहीं हो सकता । इन सब कारणों से योगी को उक्त जाति आदि दुख ही प्रतीत होते हैं ' ।
इस प्रकार से जैन दर्शन के समान योग दर्शन में भी हिंसादि पापों अथवा उन्हीं जैसे जाति, प्रायु एवं भोगों के विषय में दुःखरूपता के ही अनुभव करने की प्रेरणा की गई है ।
४०
महाव्रत - जैन दर्शन के अन्तर्गत चारित्रप्राभृत ( २६-३०), मूलाचार (१, ४-६ व ५, ६१ से ६७), तत्त्वार्थ सूत्र (७, १-२ ), दशवेकालिक (४-७, पृ. १४८-४६ ) और पाक्षिकसूत्र (पृ. १८-२६) प्रदि अनेक ग्रन्थों में श्रहिंसादि महाव्रतों का विधान किया गया है । इन व्रतों का परिपालन चूंकि जीवन पर्यन्त किया जाता है, इसलिए उन्हें यम कहा जाता है ।
I
इसी प्रकार से उक्त पांच महाव्रतों का विधान योगसूत्र में भी किया गया है । यहां योग के जिन आठ अंगों का वर्णन किया गया है उनमें प्रथम योगांग यम ही है। हिंसा के प्रभावरूप अहिंसा, सत्य, परकीय द्रव्य के अपहरण के प्रभाव रूप अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का वहां ( २-३० ) यमरूप से निर्देश करते हुए आगे (२-३१) यह कहा गया है कि जाति, देश, काल और समय के अवच्छेद से रहित . उक्त अहिंसादि पांच सार्वभौम महाव्रत माने जाते हैं । सार्वभौम कहने का कारण यही है कि उनके परिपालन में जाति व देश आदि की कोई मर्यादा नहीं रहती । उदाहरणार्थ "मैं ब्राह्मण का घात नहीं करूंगा, तीर्थ पर किसी प्राणी का घात नहीं करूंगा, चतुर्दशी दिन किसी जीव की हत्या नहीं करूंगा, अथवा देव व ब्राह्मण के प्रयोजन को छोड़कर अन्य किसी भी प्रयोजन के वश जीवहिंसा न करूंगा” इस प्रकार से जो अहिंसा का परिपालन किया जाता है क्रमशः जाति, देश, काल और समय की अपेक्षा रखने के कारण सार्वभौम नहीं कहा जा सकता । किन्तु उक्त जाति प्रादि की मर्यादा से रहित जो पूर्णरूप से हिंसा का परित्याग किया जाता है उसे ही सार्वभौम अहिंसामहाव्रत माना जाता है । यही अभिप्राय सत्यमहाव्रत आदि के विषय में भी ग्रहण करना चाहिए ।
के
उसे
इस प्रकार से उक्त अहिंसा आदि पांच महाव्रतों का स्वरूप जैसा जैन दर्शन में प्ररूपित है ठीक उसी रूप में उनका स्वरूप योगसूत्र में भी निर्दिष्ट किया गया है ।
कृत, कारित, अनुमत - जैन दर्शन में प्रास्रव व उसके भेद-प्रभेदों का निर्देश करते हुए उनके आधार जीव और जीव बतलाये गये हैं । संरम्भ, समारम्भ व प्रारम्भ; मन, वचन व काय ये तीन योग; कृत, कारित व अनुमत; तथा क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार कषायें; इनका परस्पर सम्बन्ध रहने से उक्त जीवाधिकरण के १०८ (३३३x४ ) भेद माने गये हैं । वह श्रास्रव कषाय के वश होकर मन, वचन अथवा काय के श्राश्रय से हिंसादि के स्वयं करने, अन्य से कराने अथवा करते हुए अन्य का अनुमोदन करने पर जीव के होता है उसमें तीव्र या मन्द एवं ज्ञात या अज्ञात भाव की अपेक्षा बिशेषता हुआ करती है ।
।
प्रकारान्तर से यही भाव योगसूत्र में भी प्रगट किया गया है। वहां उपर्युक्त महाव्रतों के प्रसंग में
हिंसादि पाप हैं वे क्रोध,
यह कहा गया है कि वितर्क स्वरूप - योग के प्रतिकूल माने जाने वाले - जो कराये जाते हैं,
लोभ अथवा मोह के वश होकर स्वयं किये जाते हैं, अन्य से की अनुमोदना के विषय होते हैं। साथ ही वे मृदु (मन्द), करते हैं । उनका फल श्रपरिमित दुख व अज्ञान होता है । इसलिए योगी को उक्त हिंसादि के स्वरूप व
अथवा उनमें प्रवृत्त अन्य मध्य अथवा अधि (तीव्र) मात्रा में हुआ
१. सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः । ते ह्लाद - परितापफला पुण्यापुण्यहेतुत्वात् । परिणाम-तापसंस्कार-दुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः । यो. सू. २, १३-१५.
२. नियमः परिमितकालो यावज्जीवं यमो ध्रियते ॥ रत्नक. ८७.
३. त. सू. ६, ६-८. स. सि. ६, ६-८; त. वा. ६, ८, ७-६.