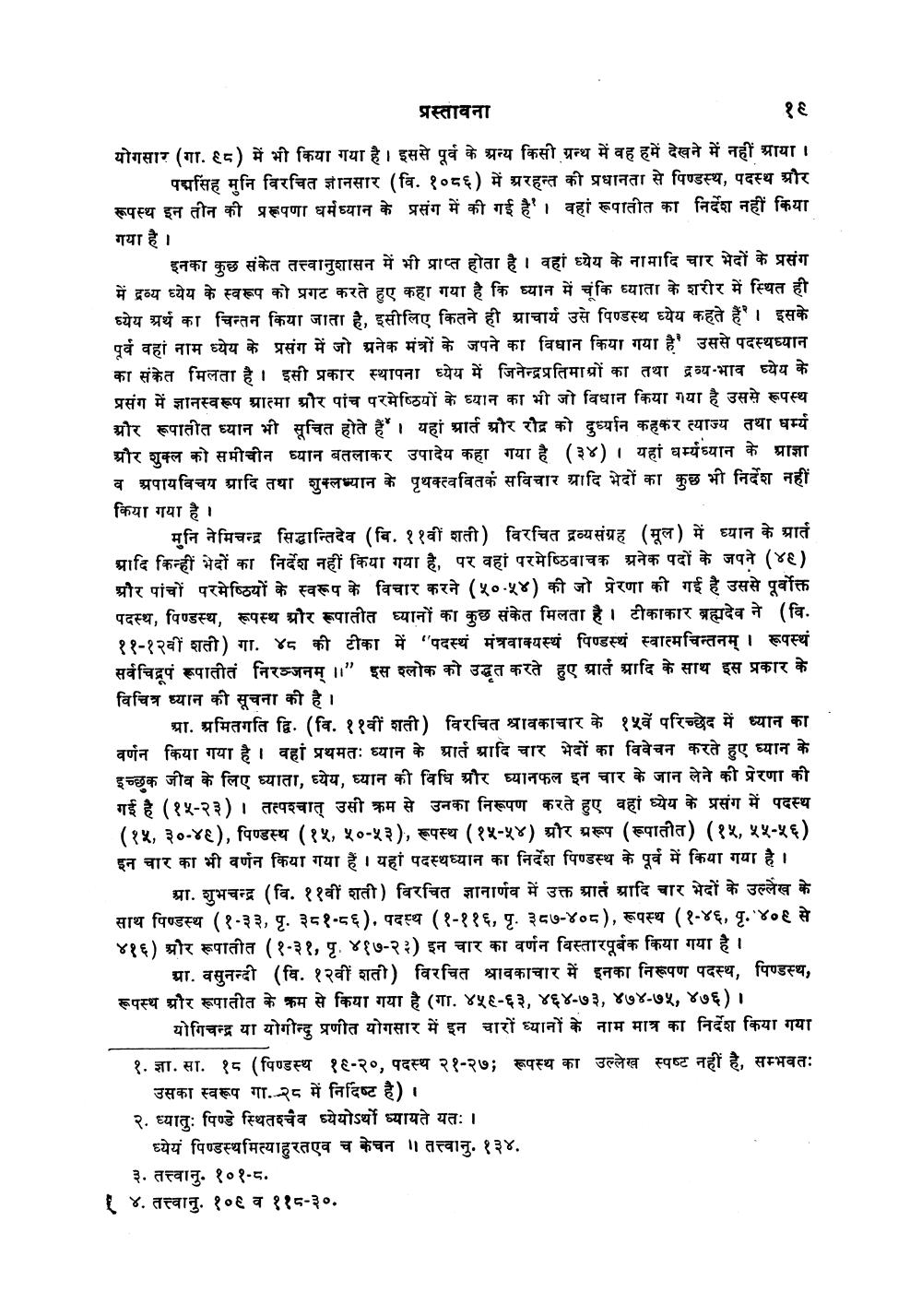________________
प्रस्तावना
१६
योगसार (गा.१८) में भी किया गया है। इससे पूर्व के अन्य किसी ग्रन्थ में वह हमें देखने में नहीं आया।
पद्मसिंह मुनि विरचित ज्ञानसार (वि. १०८६) में अरहन्त की प्रधानता से पिण्डस्थ, पदस्थ और रूपस्थ इन तीन की प्ररूपणा धर्मध्यान के प्रसंग में की गई है। वहां रूपातीत का निर्देश नहीं किया गया है।
इनका कुछ संकेत तत्त्वानुशासन में भी प्राप्त होता है। वहां ध्येय के नामादि चार भेदों के प्रसंग में द्रव्य ध्येय के स्वरूप को प्रगट करते हुए कहा गया है कि ध्यान में चूंकि ध्याता के शरीर में स्थित ही ध्येय अर्थ का चिन्तन किया जाता है, इसीलिए कितने ही प्राचार्य उस पिण्डस्थ ध्येय कहते हैं। इसके पूर्व वहां नाम ध्येय के प्रसंग में जो अनेक मंत्रों के जपने का विधान किया गया है। उससे पदस्थध्यान का संकेत मिलता है। इसी प्रकार स्थापना ध्येय में जिनेन्द्रप्रतिमानों का तथा द्रव्य-भाव ध्येय के प्रसंग में ज्ञानस्वरूप प्रात्मा और पांच परमेष्ठियों के ध्यान का भी जो विधान किया गया है उससे रूपस्थ और रूपातीत ध्यान भी सूचित होते हैं। यहां प्रार्त और रौद्र को दुर्ध्यान कहकर त्याज्य तथा धर्म्य और शुक्ल को समीचीन ध्यान बतलाकर उपादेय कहा गया है (३४)। यहां धर्म्यध्यान के प्राज्ञा व अपायविचय आदि तथा शुक्लध्यान के पृथक्त्ववितर्क सविचार आदि भेदों का कुछ भी निर्देश नहीं किया गया है।
मुनि नेमिचन्द्र सिद्धान्तिदेव (वि. ११वीं शती) विरचित द्रव्यसंग्रह (मूल) में ध्यान के प्रार्त प्रादि किन्हीं भेदों का निर्देश नहीं किया गया है, पर वहां परमेष्ठिवाचक अनेक पदों के जपने (४६) और पांचों परमेष्ठियों के स्वरूप के विचार करने (५०.५४) की जो प्रेरणा की गई है उससे पूर्वोक्त पदस्थ, पिण्डस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ध्यानों का कुछ संकेत मिलता है। टीकाकार ब्रह्मदेव ने (वि. ११-१२वीं शती) गा. ४८ की टीका में "पदस्थं मंत्रवाक्यस्थं पिण्डस्थं स्वात्मचिन्तनम् । रूपस्थं सर्वचिद्रूपं रूपातीतं निरञ्जनम् ॥” इस श्लोक को उद्धत करते हुए आर्त आदि के साथ इस प्रकार के विचित्र ध्यान की सूचना की है।
प्रा. अमितगति द्वि. (वि. ११वीं शती) विरचित श्रावकाचार के १५वें परिच्छेद में ध्यान का वर्णन किया गया है। वहां प्रथमतः ध्यान के प्रार्त आदि चार भेदों का विवेचन करते हुए ध्यान के इच्छुक जीव के लिए ध्याता, ध्येय, ध्यान की विधि और ध्यानफल इन चार के जान लेने की प्रेरणा की गई है (१५-२३)। तत्पश्चात् उसी क्रम से उनका निरूपण करते हुए वहां ध्येय के प्रसंग में पदस्थ (१५, ३०-४६), पिण्डस्थ (१५, ५०-५३), रूपस्थ (१५-५४) और अरूप (रूपातीत) (१५, ५५-५६) इन चार का भी वर्णन किया गया हैं। यहां पदस्थध्यान का निर्देश पिण्डस्थ के पूर्व में किया गया है।
प्रा. शुभचन्द्र (वि. ११वीं शती) विरचित ज्ञानार्णव में उक्त आर्त आदि चार भेदों के उल्लेख के साथ पिण्डस्थ (१.३३, पृ. ३८१.८६), पदस्थ (१-११६, पृ. ३८७-४०८), रूपस्थ (१.४६, पृ. ४०६ से ४१६) और रूपातीत (१-३१, पृ. ४१७-२३) इन चार का वर्णन विस्तारपूर्वक किया गया है ।
प्रा. वसुनन्दी (वि. १२वीं शती) विरचित श्रावकाचार में इनका निरूपण पदस्थ, पिण्डस्थ, रूपस्थ और रूपातीत के क्रम से किया गया है (गा. ४५६-६३, ४६४-७३, ४७४-७५, ४७६)।
योगिचन्द्र या योगीन्दु प्रणीत योगसार में इन चारों ध्यानों के नाम मात्र का निर्देश किया गया १. ज्ञा. सा. १८ (पिण्डस्थ १६-२०, पदस्थ २१-२७; रूपस्थ का उल्लेख स्पष्ट नहीं है, सम्भवतः
उसका स्वरूप गा.२८ में निर्दिष्ट है)। २. ध्यातुः पिण्डे स्थितश्चैव ध्येयोऽर्थो ध्यायते यतः ।
ध्येयं पिण्डस्थमित्याहरतएव च केचन ॥ तत्त्वानु. १३४. ३. तत्त्वानु. १०१-८. १४. तत्त्वानु. १०६ व ११८-३०.