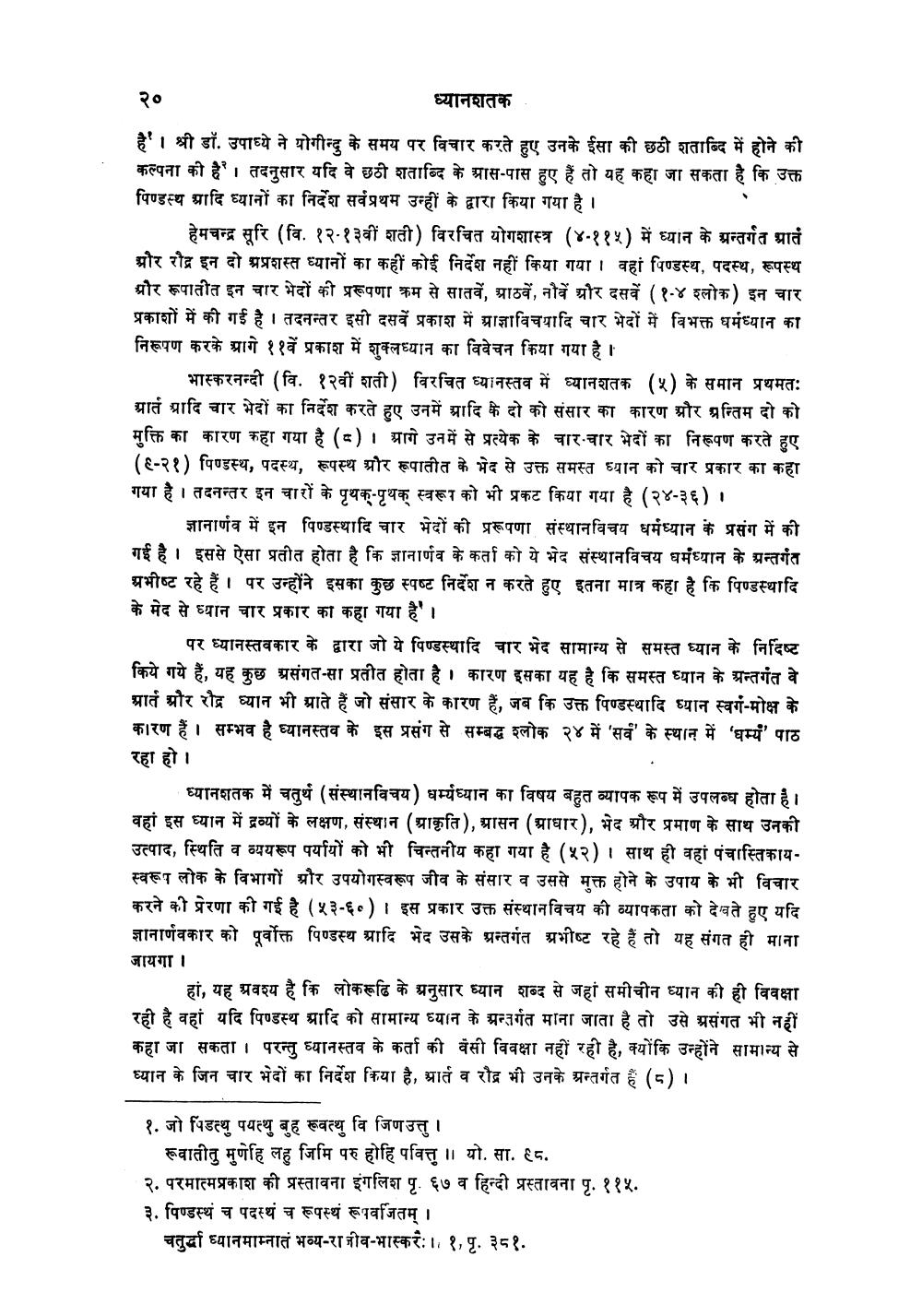________________
२०
ध्यानशतक
है। श्री डॉ. उपाध्ये ने योगीन्दु के समय पर विचार करते हए उनके ईसा की छठी शताब्दि में होने की कल्पना की है। तदनुसार यदि वे छठी शताब्दि के आस-पास हुए हैं तो यह कहा जा सकता है कि उक्त पिण्डस्थ आदि ध्यानों का निर्देश सर्वप्रथम उन्हीं के द्वारा किया गया है।
हेमचन्द्र सूरि (वि. १२-१३वीं शती) विरचित योगशास्त्र (४-११५) में ध्यान के अन्तर्गत पातं और रौद्र इन दो अप्रशस्त ध्यानों का कहीं कोई निर्देश नहीं किया गया। वहां पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत इन चार भेदों की प्ररूपणा क्रम से सातवें, आठवें, नौवें और दसवें (१.४ श्लोक) इन चार प्रकाशों में की गई है । तदनन्तर इसी दसवें प्रकाश में प्राज्ञाविचयादि चार भेदों में विभक्त धर्मध्यान का निरूपण करके आगे ११वें प्रकाश में शक्लध्यान का विवेचन किया गया है।
भास्करनन्दी (वि. १२वीं शती) विरचित ध्यानस्तव में ध्यानशतक (५) के समान प्रथमतः आर्त आदि चार भेदों का निर्देश करते हुए उनमें आदि के दो को संसार का कारण और अन्तिम दो को मुक्ति का कारण कहा गया है (८)। आगे उनमें से प्रत्येक के चार-चार भेदों का निरूपण करते हुए (६-२१) पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत के भेद से उक्त समस्त ध्यान को चार प्रकार का कहा गया है । तदनन्तर इन चारों के पृथक्-पृथक् स्वरूप को भी प्रकट किया गया है (२४-३६) ।
ज्ञानार्णव में इन पिण्डस्थादि चार भेदों की प्ररूपणा संस्थानविचय धर्मध्यान के प्रसंग में की गई है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ज्ञानार्णव के कर्ता को ये भेद संस्थानविचय धर्मध्यान के अन्तर्गत अभीष्ट रहे हैं। पर उन्होंने इसका कुछ स्पष्ट निर्देश न करते हुए इतना मात्र कहा है कि पिण्डस्थादि के मेद से ध्यान चार प्रकार का कहा गया है।
पर ध्यानस्तवकार के द्वारा जो ये पिण्डस्थादि चार भेद सामान्य से समस्त ध्यान के निर्दिष्ट किये गये हैं, यह कुछ असंगत-सा प्रतीत होता है। कारण इसका यह है कि समस्त ध्यान के अन्तर्गत वे प्रार्त और रौद्र ध्यान भी आते हैं जो संसार के कारण हैं, जब कि उक्त पिण्डस्थादि ध्यान स्वर्ग-मोक्ष के कारण हैं। सम्भव है ध्यानस्तव के इस प्रसंग से सम्बद्ध श्लोक २४ में 'सर्व' के स्थान में 'धम्य' पाठ रहा हो।
ध्यानशतक में चतुर्थ (संस्थानविचय) धर्म्यध्यान का विषय बहुत व्यापक रूप में उपलब्ध होता है। वहां इस ध्यान में द्रव्यों के लक्षण, संस्थान (ग्राकृति), प्रासन (प्राधार), भेद और प्रमाण के साथ उनकी उत्पाद, स्थिति व व्ययरूप पर्यायों को भी चिन्तनीय कहा गया है (५२)। साथ ही वहां पंचास्तिकायस्वरूप लोक के विभागों और उपयोगस्वरूप जीव के संसार व उससे मुक्त होने के उपाय के भी विचार करने की प्रेरणा की गई है (५३-६०)। इस प्रकार उक्त संस्थान विचय की व्यापकता को देखते हुए यदि ज्ञानार्णवकार को पूर्वोक्त पिण्डस्थ आदि भेद उसके अन्तर्गत अभीष्ट रहे हैं तो यह संगत ही माना जायगा।
हां, यह अवश्य है कि लोकरूढि के अनुसार ध्यान शब्द से जहां समीचीन ध्यान की ही विवक्षा रही है वहां यदि पिण्डस्थ आदि को सामान्य ध्यान के अन्तर्गत माना जाता है तो उसे असंगत भी नहीं कहा जा सकता। परन्तु ध्यानस्तव के कर्ता की वैसी विवक्षा नहीं रही है, क्योंकि उन्होंने सामान्य से ध्यान के जिन चार भेदों का निर्देश किया है, आर्त व रौद्र भी उनके अन्तर्गत हैं (८)।
१. जो पिंडत्थु पयत्थु बुह रूवत्थु वि जिणउत्तु ।
रूवातीतु मुणेहि लहु जिमि परु होहि पवित्तु ।। यो. सा. ६८. २. परमात्मप्रकाश की प्रस्तावना इंगलिश पृ. ६७ व हिन्दी प्रस्तावना पृ. ११५. ३. पिण्डस्थं च पदस्थं च रूपस्थं रूपवजितम् ।
चतुर्दा ध्यानमाम्नातं भव्य-राजीव-भास्करैः।। १, पृ. ३८१.