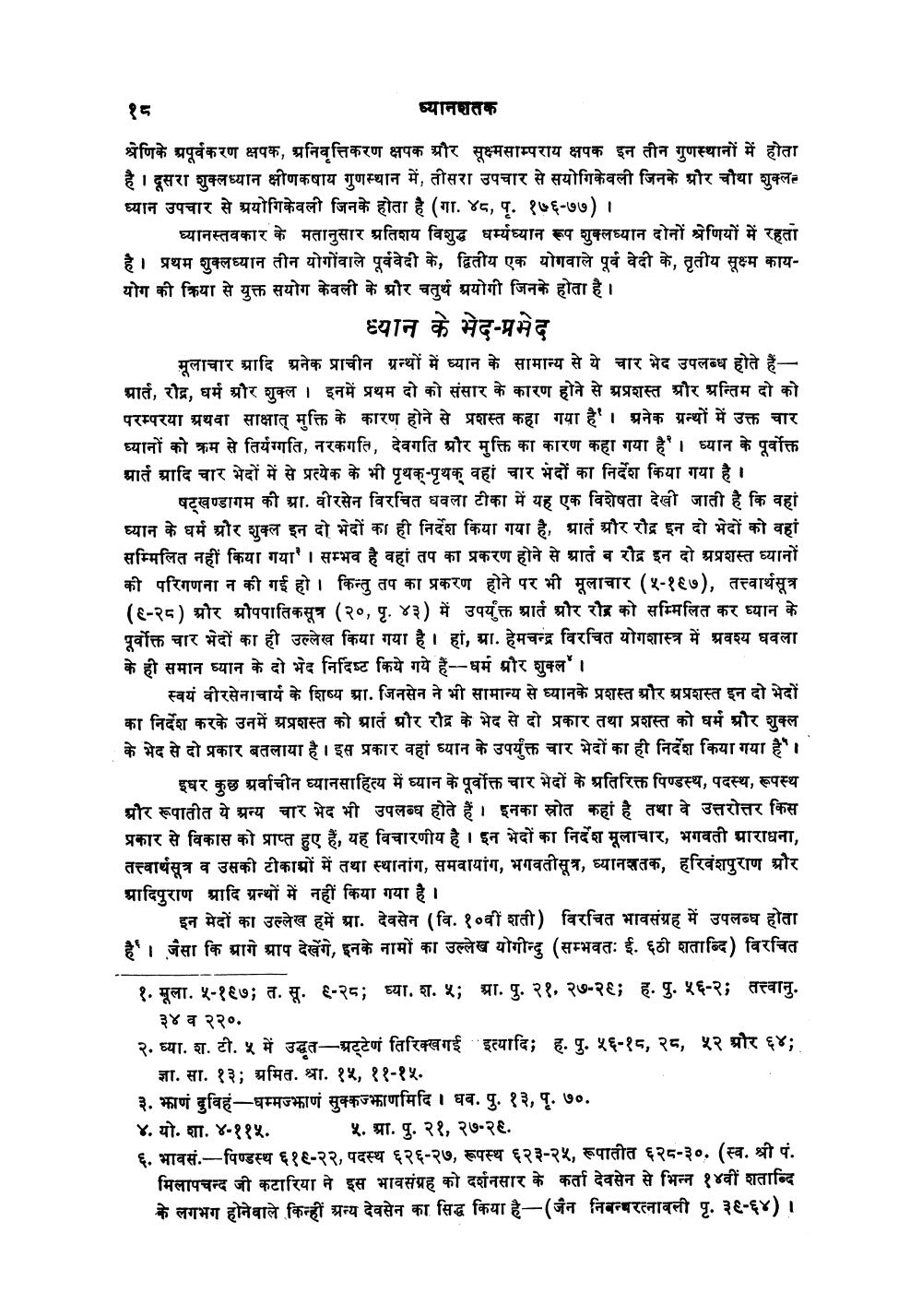________________
ध्यानशतक
श्रेणिके अपूर्वकरण क्षपक, अनिवृत्तिकरण क्षपक और सूक्ष्मसाम्पराय क्षपक इन तीन गुणस्थानों में होता है। दूसरा शुक्लध्यान क्षीणकषाय गुणस्थान में, तीसरा उपचार से सयोगिकेवली जिनके और चौथा शुक्ला ध्यान उपचार से अयोगिकेवली जिनके होता है (गा. ४८, पृ. १७६-७७)।
ध्यानस्तवकार के मतानुसार अतिशय विशुद्ध धर्म्यध्यान रूप शुक्लध्यान दोनों श्रेणियों में रहता है। प्रथम शुक्लध्यान तीन योगोंवाले पूर्ववेदी के, द्वितीय एक योगवाले पूर्व वेदी के, तृतीय सूक्ष्म काययोग की क्रिया से युक्त सयोग केवली के और चतुर्थ अयोगी जिनके होता है।
ध्यान के भेद-प्रभेद मूलाचार आदि अनेक प्राचीन ग्रन्थों में ध्यान के सामान्य से ये चार भेद उपलब्ध होते हैंप्रात, रौद्र, धर्म और शुक्ल । इनमें प्रथम दो को संसार के कारण होने से अप्रशस्त और अन्तिम दो को परम्परया अथवा साक्षात् मुक्ति के कारण होने से प्रशस्त कहा गया है। अनेक ग्रन्थों में उक्त चार ध्यानों को क्रम से तिर्यग्गति, नरकगति, देवगति और मुक्ति का कारण कहा गया है। ध्यान के पूर्वोक्त मार्त आदि चार भेदों में से प्रत्येक के भी पृथक-पृथक् वहां चार भेदों का निर्देश किया गया है।
षट्खण्डागम की प्रा. वीरसेन विरचित धवला टीका में यह एक विशेषता देखी जाती है कि वहां ध्यान के धर्म और शुक्ल इन दो भेदों का ही निर्देश किया गया है, प्रार्त और रौद्र इन दो भेदों को वहां सम्मिलित नहीं किया गया । सम्भव है वहां तप का प्रकरण होने से प्रार्त व रौद्र इन दो अप्रशस्त ध्यानों की परिगणना न की गई हो। किन्तु तप का प्रकरण होने पर भी मूलाचार (५-१६७), तत्त्वार्थसूत्र (६-२८) और प्रोपपातिकसूत्र (२०, पृ. ४३) में उपर्युक्त पात और रौद्र को सम्मिलित कर ध्यान के पूर्वोक्त चार भेदों का ही उल्लेख किया गया है। हां, प्रा. हेमचन्द्र विरचित योगशास्त्र में अवश्य धवला के ही समान ध्यान के दो भेद निर्दिष्ट किये गये हैं-धर्म और शुक्ल ।
स्वयं वीरसेनाचार्य के शिष्य प्रा. जिनसेन ने भी सामान्य से ध्यानके प्रशस्त और अप्रशस्त इन दो भेदों का निर्देश करके उनमें अप्रशस्त को प्रात और रौद्र के भेद से दो प्रकार तथा प्रशस्त को धर्म और शुक्ल के भेद से दो प्रकार बतलाया है । इस प्रकार वहां ध्यान के उपर्युक्त चार भेदों का ही निर्देश किया गया है।
इधर कुछ अर्वाचीन ध्यानसाहित्य में ध्यान के पूर्वोक्त चार भेदों के अतिरिक्त पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ये अन्य चार भेद भी उपलब्ध होते हैं। इनका स्रोत कहां है तथा वे उत्तरोत्तर किस प्रकार से विकास को प्राप्त हुए हैं, यह विचारणीय है । इन भेदों का निर्देश मूलाचार, भगवती माराधना, तत्त्वार्थसूत्र व उसको टीकामों में तथा स्थानांग, समवायांग, भगवतीसूत्र, ध्यानशतक, हरिवंशपुराण और प्रादिपुराण आदि ग्रन्थों में नहीं किया गया है।
इन मेदों का उल्लेख हमें प्रा. देवसेन (वि. १०वीं शती) विरचित भावसंग्रह में उपलब्ध होता है। जैसा कि आगे आप देखेंगे, इनके नामों का उल्लेख योगीन्दु (सम्भवतः ई. ६ठी शताब्दि) विरचित
१. मूला. ५-१९७; त. सू. ६-२८; ध्या. श. ५; प्रा. पु. २१, २७-२६) ह. पु. ५६-२, तत्त्वानु.
३४ व २२०. २. ध्या. श. टी. ५ में उद्धृत-अटेणं तिरिक्खगई इत्यादि; ह. पु. ५६-१८, २८, ५२ और ६४; ___ ज्ञा. सा. १३; अमित. श्रा. १५, ११-१५. ३. झाणं दुविहं-धम्मज्झाणं सुक्कज्झाणमिदि । धव. पु. १३, पृ. ७०. ४. यो. शा. ४-११५. ५. प्रा. पु. २१, २७-२६.. ६. भावसं.-पिण्डस्थ ६१६-२२, पदस्थ ६२६-२७, रूपस्थ ६२३-२५, रूपातीत ६२८-३०. (स्व. श्री पं. मिलापचन्द जी कटारिया ने इस भावसंग्रह को दर्शनसार के कर्ता देवसेन से भिन्न १४वीं शतान्दि के लगभग होनेवाले किन्हीं अन्य देवसेन का सिद्ध किया है-(जैन निवन्धरत्नावली पृ. ३६-६४)।