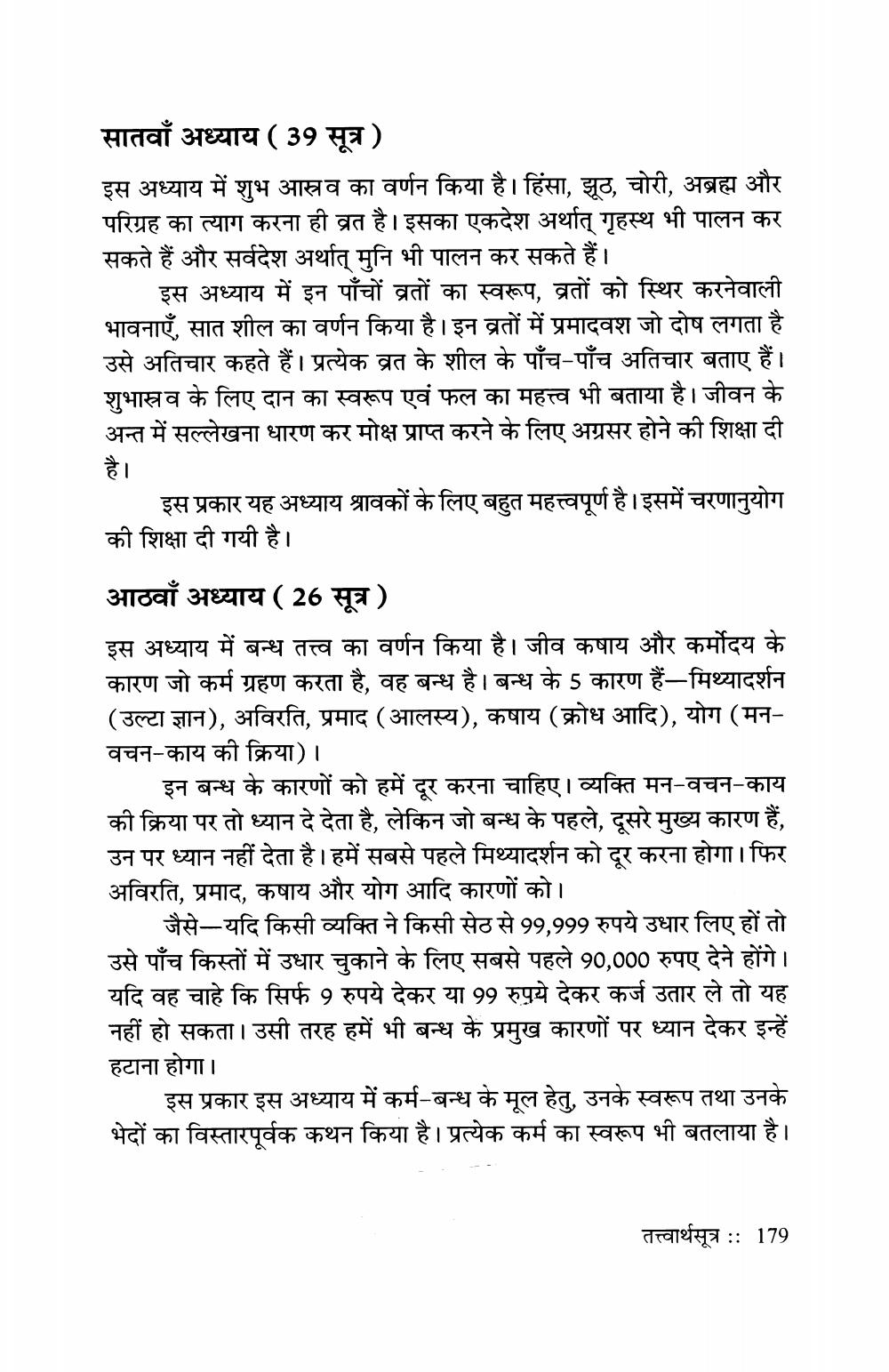________________
सातवाँ अध्याय ( 39 सूत्र) इस अध्याय में शुभ आस्रव का वर्णन किया है। हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह का त्याग करना ही व्रत है। इसका एकदेश अर्थात् गृहस्थ भी पालन कर सकते हैं और सर्वदेश अर्थात् मुनि भी पालन कर सकते हैं।
__इस अध्याय में इन पाँचों व्रतों का स्वरूप, व्रतों को स्थिर करनेवाली भावनाएँ, सात शील का वर्णन किया है। इन व्रतों में प्रमादवश जो दोष लगता है उसे अतिचार कहते हैं। प्रत्येक व्रत के शील के पाँच-पाँच अतिचार बताए हैं। शुभास्रव के लिए दान का स्वरूप एवं फल का महत्त्व भी बताया है। जीवन के अन्त में सल्लेखना धारण कर मोक्ष प्राप्त करने के लिए अग्रसर होने की शिक्षा दी
इस प्रकार यह अध्याय श्रावकों के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसमें चरणानुयोग की शिक्षा दी गयी है। आठवाँ अध्याय ( 26 सूत्र) इस अध्याय में बन्ध तत्त्व का वर्णन किया है। जीव कषाय और कर्मोदय के कारण जो कर्म ग्रहण करता है, वह बन्ध है। बन्ध के 5 कारण हैं-मिथ्यादर्शन (उल्टा ज्ञान), अविरति, प्रमाद (आलस्य), कषाय (क्रोध आदि), योग (मनवचन-काय की क्रिया)।
इन बन्ध के कारणों को हमें दूर करना चाहिए। व्यक्ति मन-वचन-काय की क्रिया पर तो ध्यान दे देता है, लेकिन जो बन्ध के पहले, दूसरे मुख्य कारण हैं, उन पर ध्यान नहीं देता है। हमें सबसे पहले मिथ्यादर्शन को दूर करना होगा। फिर अविरति, प्रमाद, कषाय और योग आदि कारणों को।
जैसे-यदि किसी व्यक्ति ने किसी सेठ से 99,999 रुपये उधार लिए हों तो उसे पाँच किस्तों में उधार चुकाने के लिए सबसे पहले 90,000 रुपए देने होंगे। यदि वह चाहे कि सिर्फ 9 रुपये देकर या 99 रुपये देकर कर्ज उतार ले तो यह नहीं हो सकता। उसी तरह हमें भी बन्ध के प्रमुख कारणों पर ध्यान देकर इन्हें हटाना होगा।
इस प्रकार इस अध्याय में कर्म-बन्ध के मूल हेतु, उनके स्वरूप तथा उनके भेदों का विस्तारपूर्वक कथन किया है। प्रत्येक कर्म का स्वरूप भी बतलाया है।
तत्त्वार्थसूत्र :: 179