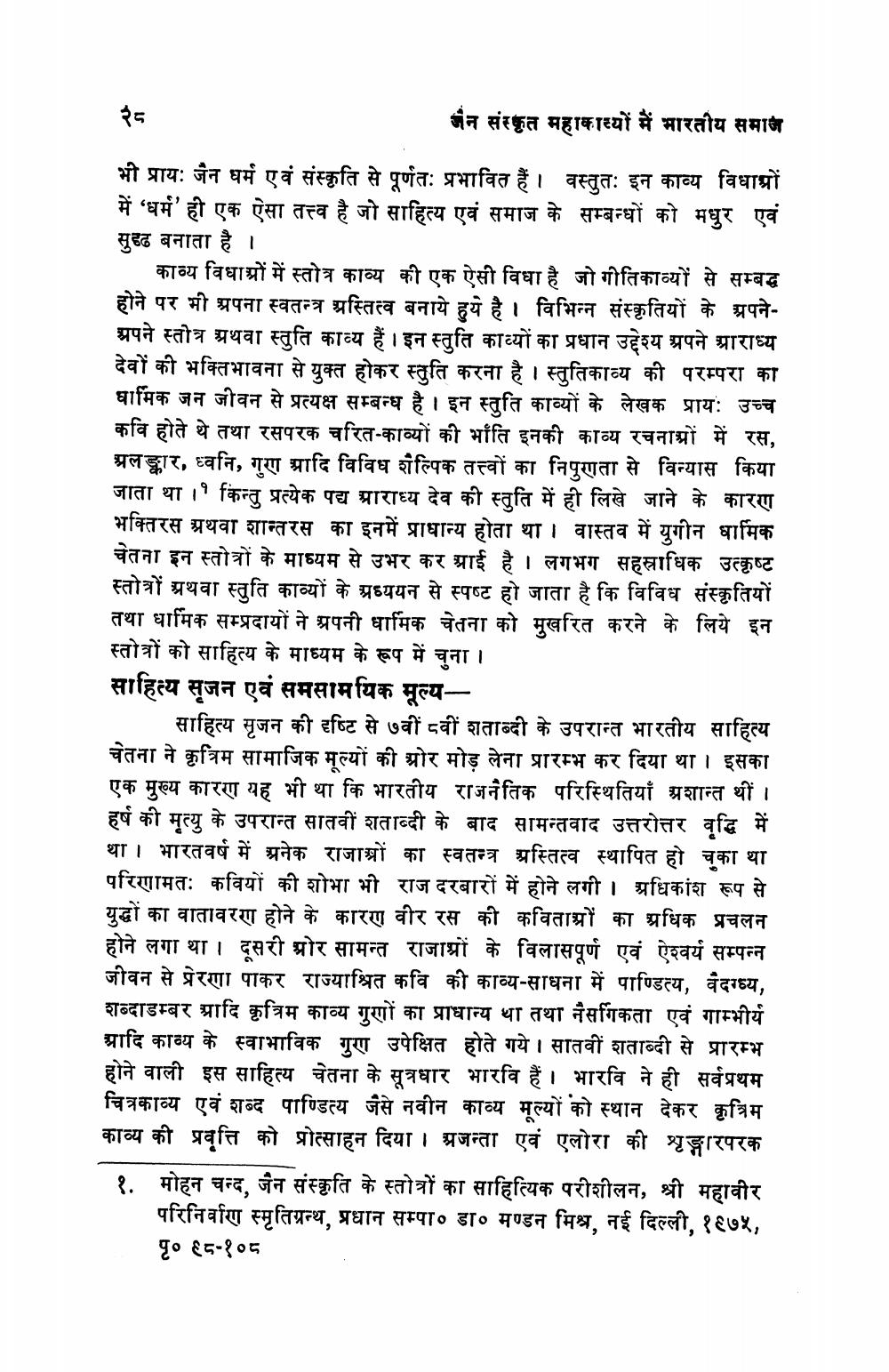________________
जैन संस्कृत महाकायों में भारतीय समाज
भी प्रायः जैन धर्म एवं संस्कृति से पूर्णतः प्रभावित हैं। वस्तुतः इन काव्य विधात्रों में 'धर्म' ही एक ऐसा तत्त्व है जो साहित्य एवं समाज के सम्बन्धों को मधुर एवं सुदृढ बनाता है । ___काव्य विधाओं में स्तोत्र काव्य की एक ऐसी विधा है जो गीतिकाव्यों से सम्बद्ध होने पर भी अपना स्वतन्त्र अस्तित्व बनाये हुये है। विभिन्न संस्कृतियों के अपनेअपने स्तोत्र अथवा स्तुति काव्य हैं । इन स्तुति काव्यों का प्रधान उद्देश्य अपने आराध्य देवों की भक्तिभावना से युक्त होकर स्तुति करना है । स्तुतिकाव्य की परम्परा का धार्मिक जन जीवन से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। इन स्तुति काव्यों के लेखक प्राय: उच्च कवि होते थे तथा रसपरक चरित-काव्यों की भांति इनकी काव्य रचनाओं में रस, अलङ्कार, ध्वनि, गुण आदि विविध शैल्पिक तत्त्वों का निपुणता से विन्यास किया जाता था ।' किन्तु प्रत्येक पद्य आराध्य देव की स्तुति में ही लिखे जाने के कारण भक्तिरस अथवा शान्तरस का इनमें प्राधान्य होता था। वास्तव में युगीन धार्मिक चेतना इन स्तोत्रों के माध्यम से उभर कर आई है । लगभग सहस्राधिक उत्कृष्ट स्तोत्रों अथवा स्तुति काव्यों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि विविध संस्कृतियों तथा धार्मिक सम्प्रदायों ने अपनी धार्मिक चेतना को मुखरित करने के लिये इन स्तोत्रों को साहित्य के माध्यम के रूप में चुना। साहित्य सृजन एवं समसामयिक मूल्य
साहित्य सृजन की दृष्टि से ७वीं ८वीं शताब्दी के उपरान्त भारतीय साहित्य चेतना ने कृत्रिम सामाजिक मूल्यों की ओर मोड़ लेना प्रारम्भ कर दिया था। इसका एक मुख्य कारण यह भी था कि भारतीय राजनैतिक परिस्थितियाँ प्रशान्त थीं। हर्ष की मृत्यु के उपरान्त सातवीं शताब्दी के बाद सामन्तवाद उत्तरोत्तर वृद्धि में था। भारतवर्ष में अनेक राजाओं का स्वतन्त्र अस्तित्व स्थापित हो चुका था परिणामतः कवियों की शोभा भी राज दरबारों में होने लगी। अधिकांश रूप से युद्धों का वातावरण होने के कारण वीर रस की कविताओं का अधिक प्रचलन होने लगा था। दूसरी ओर सामन्त राजारों के विलासपूर्ण एवं ऐश्वर्य सम्पन्न जीवन से प्रेरणा पाकर राज्याश्रित कवि की काव्य-साधना में पाण्डित्य, वैदग्ध्य, शब्दाडम्बर आदि कृत्रिम काव्य गुणों का प्राधान्य था तथा नैसर्गिकता एवं गाम्भीर्य आदि काव्य के स्वाभाविक गुण उपेक्षित होते गये । सातवीं शताब्दी से प्रारम्भ होने वाली इस साहित्य चेतना के सूत्रधार भारवि हैं। भारवि ने ही सर्वप्रथम चित्रकाव्य एवं शब्द पाण्डित्य जैसे नवीन काव्य मूल्यों को स्थान देकर कृत्रिम काव्य की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया। अजन्ता एवं एलोरा की शृङ्गारपरक
मोहन चन्द, जैन संस्कृति के स्तोत्रों का साहित्यिक परीशीलन, श्री महावीर परिनिर्वाण स्मृतिग्रन्थ, प्रधान सम्पा० डा० मण्डन मिश्र, नई दिल्ली, १६७५, पृ०६८-१०८