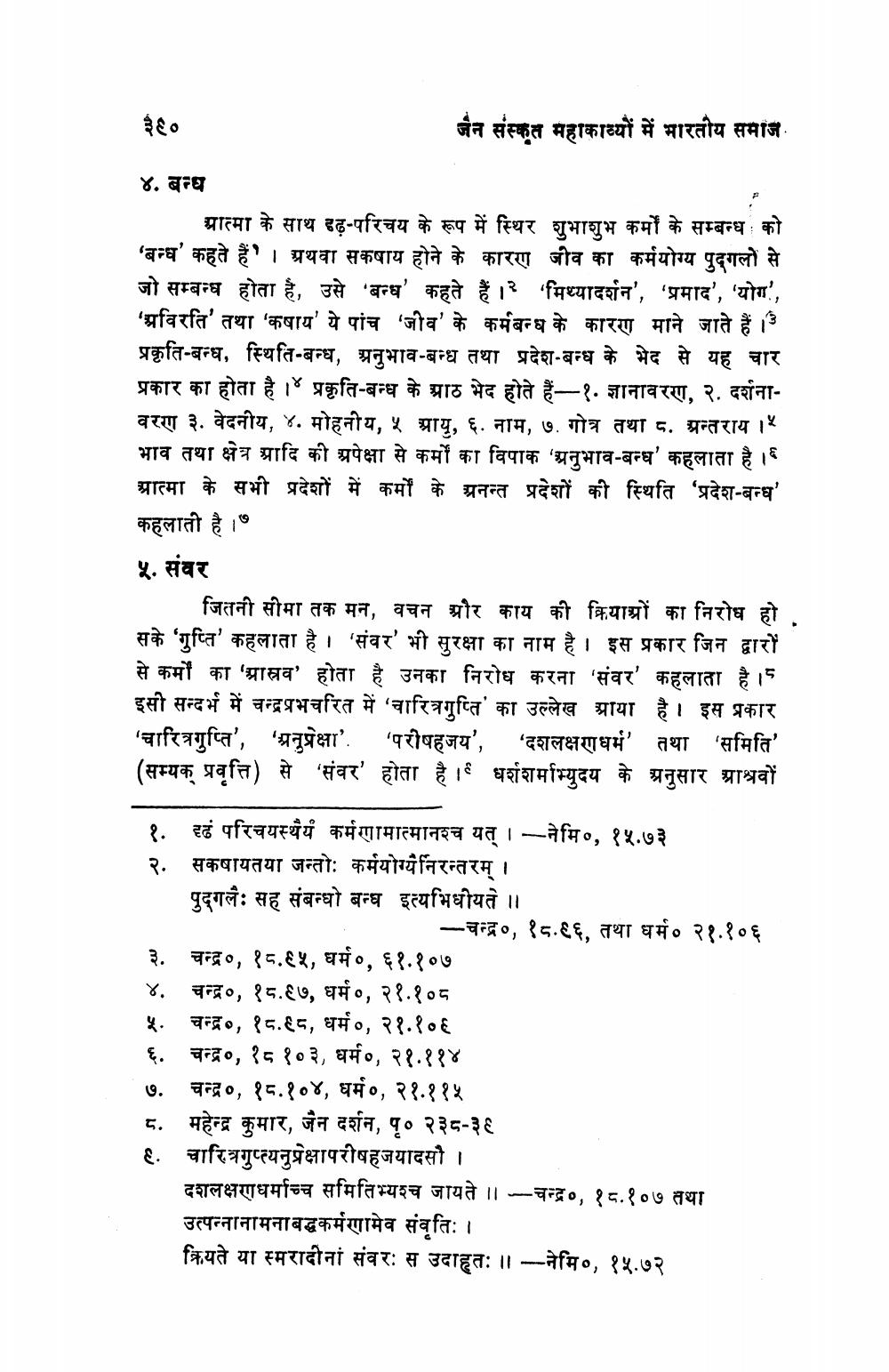________________
जैन संस्कृत महाकाव्यों में भारतीय समाज
४. बन्ध
__ प्रात्मा के साथ हढ़-परिचय के रूप में स्थिर शुभाशुभ कर्मों के सम्बन्ध को 'बन्ध' कहते हैं । अथवा सकषाय होने के कारण जीव का कर्मयोग्य पुद्गलों से जो सम्बन्ध होता है, उसे 'बन्ध' कहते हैं । २ 'मिथ्यादर्शन', 'प्रमाद', 'योग', 'अविरति' तथा 'कषाय' ये पांच 'जीव' के कर्मबन्ध के कारण माने जाते हैं। प्रकृति-बन्ध, स्थिति-बन्ध, अनुभाव-बन्ध तथा प्रदेश-बन्ध के भेद से यह चार प्रकार का होता है। प्रकृति-बन्ध के पाठ भेद होते हैं-१. ज्ञानावरण, २. दर्शनावरण ३. वेदनीय, ४. मोहनीय, ५ आयु, ६. नाम, ७. गोत्र तथा ८. अन्तराय । भाव तथा क्षेत्र आदि की अपेक्षा से कर्मों का विपाक 'अनुभाव-बन्ध' कहलाता है । ६ आत्मा के सभी प्रदेशों में कर्मों के अनन्त प्रदेशों की स्थिति 'प्रदेश-बन्ध'
कहलाती है ।
५. संवर
जितनी सीमा तक मन, वचन और काय की क्रियाओं का निरोध हो . सके 'गुप्ति' कहलाता है। 'संवर' भी सुरक्षा का नाम है। इस प्रकार जिन द्वारों से कर्मों का 'प्रास्रव' होता है उनका निरोध करना 'संवर' कहलाता है। इसी सन्दर्भ में चन्द्रप्रभचरित में ‘चारित्रगुप्ति का उल्लेख आया है। इस प्रकार 'चारित्रगुप्ति', 'अनुप्रेक्षा'. 'परीषहजय', 'दशलक्षणधर्म' तथा 'समिति' (सम्यक् प्रवृत्ति) से 'संवर' होता है। धर्शशर्माभ्युदय के अनुसार प्राश्रवों
१. दृढं परिचयस्थैर्य कर्मणामात्मानश्च यत् । -नेमि०, १५.७३ २. सकषायतया जन्तोः कर्मयोग्यनिरन्तरम् । पुद्गलैः सह संबन्धो बन्ध इत्यभिधीयते ।।
-चन्द्र०, १८.६६, तथा धर्म० २१.१०६ ३. चन्द्र०, १८.६५, धर्म०, ६१.१०७ ४. चन्द्र०, १८.६७, धर्म०, २१.१०८ ५. चन्द्र०, १८.९८, धर्म०, २१.१०६ ६. चन्द्र०, १८ १०३, धर्म०, २१.११४ ७. चन्द्र०, १८.१०४, धर्म०, २१.११५ ८. महेन्द्र कुमार, जैन दर्शन, पृ० २३८-३६
चारित्रगुप्त्यनुप्रेक्षापरीषहजयादसौ । दशलक्षणधर्माच्च समितिभ्यश्च जायते ।। -चन्द्र०, १८.१०७ तथा उत्पन्नानामनाबद्धकर्मणामेव संवृतिः । क्रियते या स्मरादीनां संवरः स उदाहृतः ।। -नेमि०, १५.७२