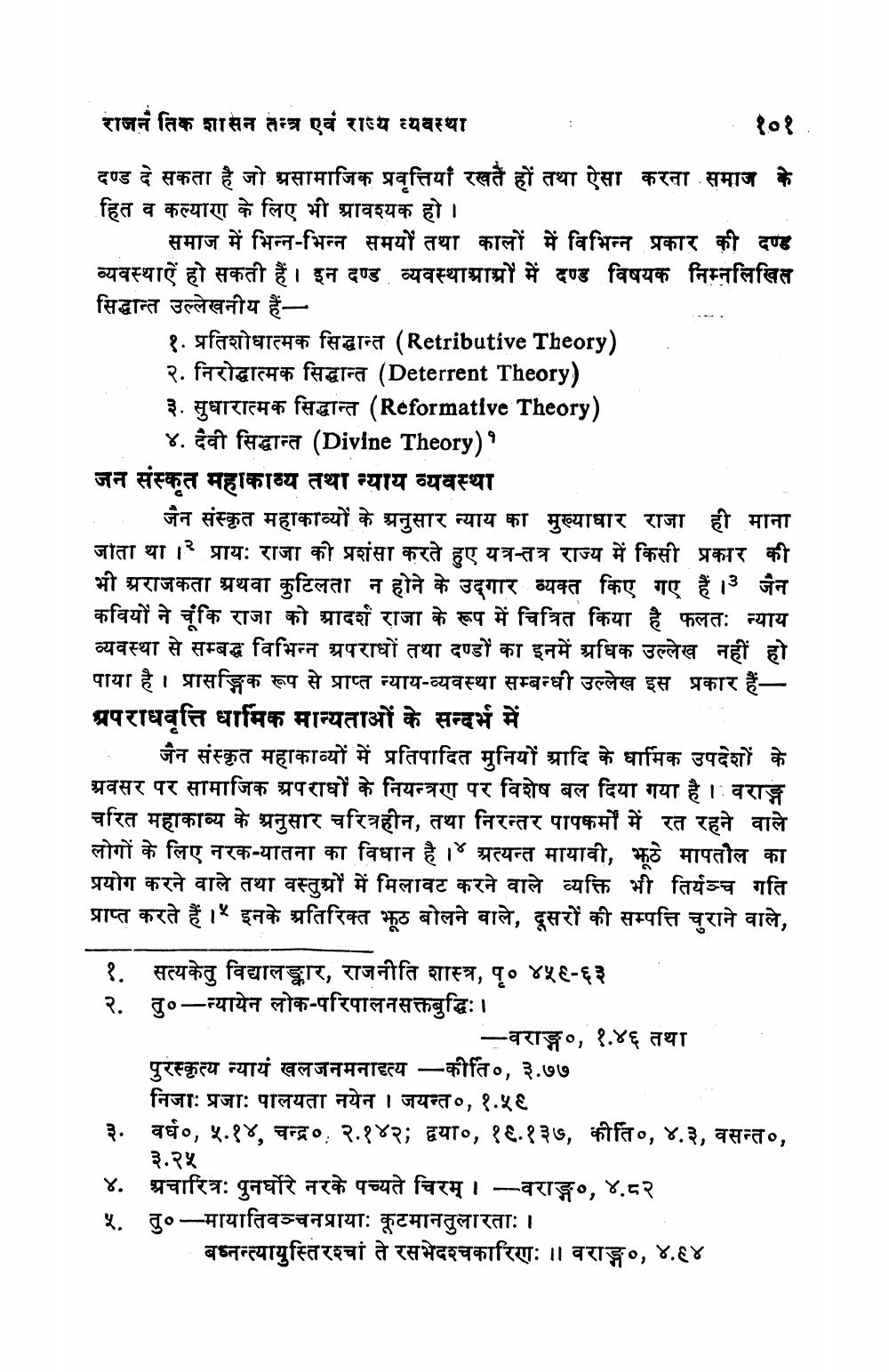________________
राजन तिक शासन तन्त्र एवं राज्य व्यवस्था
१०१
दण्ड दे सकता है जो प्रसामाजिक प्रवृत्तियाँ रखते हों तथा ऐसा करना समाज के हित व कल्याण के लिए भी श्रावश्यक हो ।
समाज में भिन्न-भिन्न समयों तथा कालों में विभिन्न प्रकार की दण्ड व्यवस्थाएं हो सकती हैं। इन दण्ड व्यवस्थामानों में दण्ड विषयक निम्नलिखित सिद्धान्त उल्लेखनीय हैं
१. प्रतिशोधात्मक सिद्धान्त ( Retributive Theory ) २. निरोद्धात्मक सिद्धान्त ( Deterrent Theory )
३. सुधारात्मक सिद्धान्त ( Reformative Theory ) ४. दैवी सिद्धान्त (Divine Theory ) '
जन संस्कृत महाकाव्य तथा न्याय व्यवस्था
जैन संस्कृत महाकाव्यों के अनुसार न्याय का मुख्याधार राजा ही माना जाता था । प्रायः राजा की प्रशंसा करते हुए यत्र-तत्र राज्य में किसी प्रकार की भी अराजकता अथवा कुटिलता न होने के उद्गार व्यक्त किए गए हैं । 3 जैन कवियों ने चूंकि राजा को आदर्श राजा के रूप में चित्रित किया है फलतः न्याय व्यवस्था से सम्बद्ध विभिन्न अपराधों तथा दण्डों का इनमें अधिक उल्लेख नहीं हो पाया है । प्रासङ्गिक रूप से प्राप्त न्याय व्यवस्था सम्बन्धी उल्लेख इस प्रकार हैं— श्रपराधवृत्ति धार्मिक मान्यताओं के सन्दर्भ में
जैन संस्कृत महाकाव्यों में प्रतिपादित मुनियों आदि के धार्मिक उपदेशों के अवसर पर सामाजिक अपराधों के नियन्त्रण पर विशेष बल दिया गया है । वराङ्ग चरित महाकाव्य के अनुसार चरित्रहीन, तथा निरन्तर पापकर्मों में रत रहने वाले लोगों के लिए नरक यातना का विधान है । अत्यन्त मायावी, झूठे मापतौल का प्रयोग करने वाले तथा वस्तुनों में मिलावट करने वाले व्यक्ति भी तिर्यञ्च गति प्राप्त करते हैं । इनके अतिरिक्त झूठ बोलने वाले, दूसरों की सम्पत्ति चुराने वाले,
१. सत्यकेतु विद्यालङ्कार, राजनीति शास्त्र, पृ० ४५९-६३ २. तु० – न्यायेन लोक-परिपालनसक्तबुद्धिः ।
— वराङ्ग०, १.४६ तथा
पुरस्कृत्य न्यायं खलजनमनादृत्य -कीर्ति ०, ३.७७ निजाः प्रजाः पालयता नयेन । जयन्त०, १.५६
वर्ध०, ५.१४, चन्द्र० २.१४२; द्वया०, १६.१३७, कीर्ति०, ४.३, वसन्त०,
३.२५
४.८२
४. प्रचारित्रः पुनर्घोरे नरके पच्यते चिरम् । – वराङ्ग०, ५. तु० – मायातिवञ्चनप्रायाः कूटमानतुला रताः ।
नन्त्यायुस्तिरश्चां ते रसभेदश्चकारिणः । वराङ्ग०, ४.६४