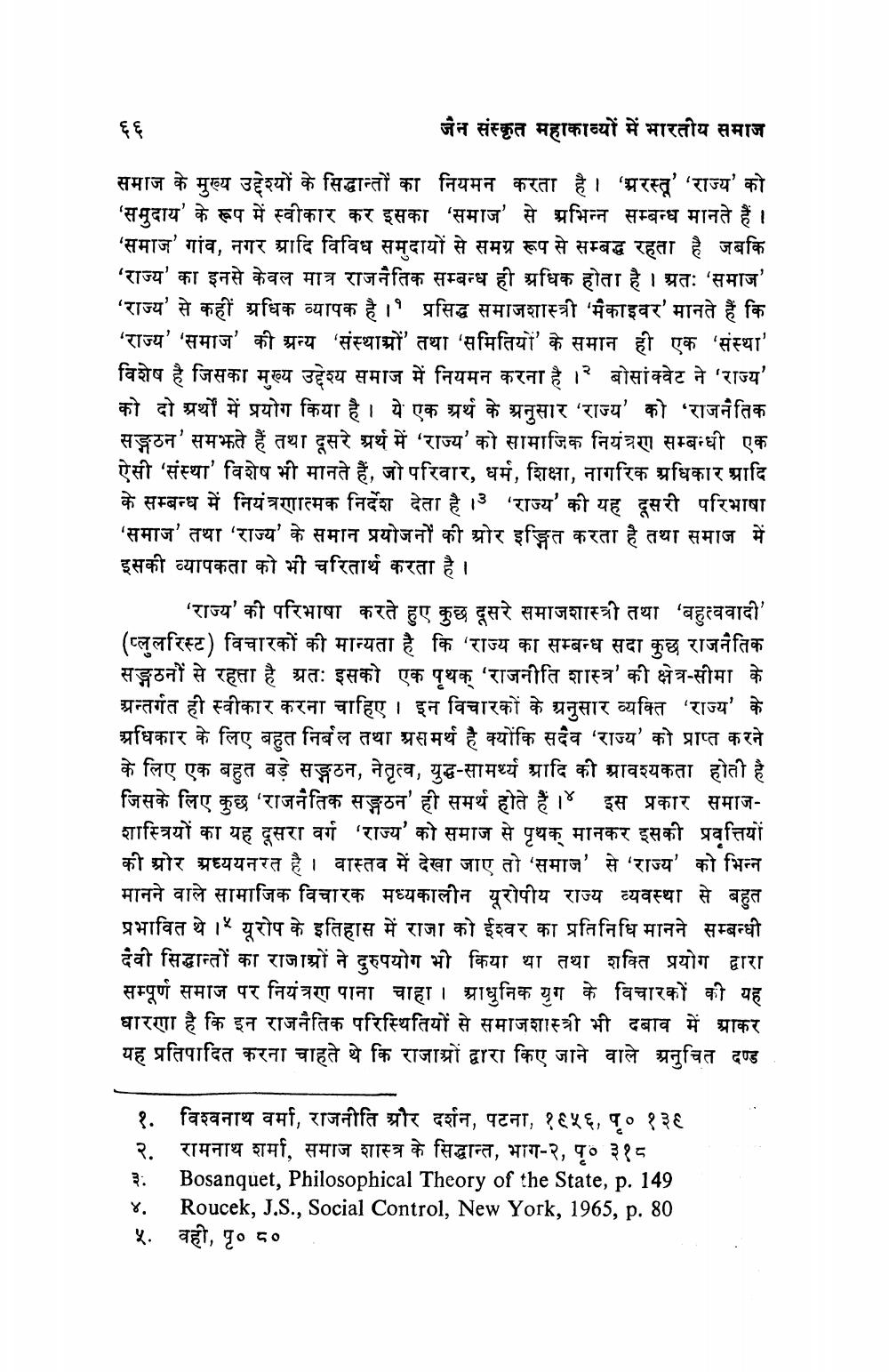________________
६६
जैन संस्कृत महाकाव्यों में भारतीय समाज
समाज के मुख्य उद्देश्यों के सिद्धान्तों का नियमन करता है। 'अरस्तू' 'राज्य' को 'समुदाय' के रूप में स्वीकार कर इसका 'समाज' से अभिन्न सम्बन्ध मानते हैं। 'समाज' गांव, नगर आदि विविध समदायों से समग्र रूप से सम्बद्ध रहता है जबकि 'राज्य' का इनसे केवल मात्र राजनैतिक सम्बन्ध ही अधिक होता है । अतः 'समाज' 'राज्य' से कहीं अधिक व्यापक है ।' प्रसिद्ध समाजशास्त्री 'मैकाइवर' मानते हैं कि 'राज्य' 'समाज' की अन्य संस्थाओं' तथा 'समितियों के समान ही एक 'संस्था' विशेष है जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में नियमन करना है ।२ बोसांक्वेट ने 'राज्य' को दो अर्थों में प्रयोग किया है। ये एक अर्थ के अनुसार 'राज्य' को 'राजनैतिक सङ्गठन' समझते हैं तथा दूसरे अर्थ में 'राज्य' को सामाजिक नियंत्रण सम्बन्धी एक ऐसी संस्था' विशेष भी मानते हैं, जो परिवार, धर्म, शिक्षा, नागरिक अधिकार प्रादि के सम्बन्ध में नियंत्रणात्मक निर्देश देता है ।3 ‘राज्य' की यह दूसरी परिभाषा 'समाज' तथा 'राज्य' के समान प्रयोजनों की ओर इङ्गित करता है तथा समाज में इसकी व्यापकता को भी चरितार्थ करता है ।
‘राज्य' की परिभाषा करते हुए कुछ दूसरे समाजशास्त्री तथा 'बहुत्ववादी' (प्लुलरिस्ट) विचारकों की मान्यता है कि 'राज्य का सम्बन्ध सदा कुछ राजनैतिक सङ्गठनों से रहता है अतः इसको एक पृथक् 'राजनीति शास्त्र' की क्षेत्र-सीमा के अन्तर्गत ही स्वीकार करना चाहिए। इन विचारकों के अनुसार व्यक्ति ‘राज्य' के अधिकार के लिए बहुत निर्बल तथा असमर्थ है क्योंकि सदैव 'राज्य' को प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़े सङ्गठन, नेतृत्व, युद्ध-सामर्थ्य आदि की आवश्यकता होती है जिसके लिए कुछ 'राजनैतिक सङ्गठन' ही समर्थ होते हैं। इस प्रकार समाजशास्त्रियों का यह दूसरा वर्ग 'राज्य' को समाज से पृथक् मानकर इसकी प्रवृत्तियों की ओर अध्ययनरत है। वास्तव में देखा जाए तो 'समाज' से 'राज्य' को भिन्न मानने वाले सामाजिक विचारक मध्यकालीन यूरोपीय राज्य व्यवस्था से बहुत प्रभावित थे ।५ यूरोप के इतिहास में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानने सम्बन्धी देवी सिद्धान्तों का राजाओं ने दुरुपयोग भी किया था तथा शक्ति प्रयोग द्वारा सम्पूर्ण समाज पर नियंत्रण पाना चाहा। आधुनिक युग के विचारकों की यह धारणा है कि इन राजनैतिक परिस्थितियों से समाजशास्त्री भी दबाव में आकर यह प्रतिपादित करना चाहते थे कि राजारों द्वारा किए जाने वाले अनुचित दण्ड
१. विश्वनाथ वर्मा, राजनीति और दर्शन, पटना, १६५६, पृ० १३६ २. रामनाथ शर्मा, समाज शास्त्र के सिद्धान्त, भाग-२, पृ० ३१८ । ३. Bosanquet, Philosophical Theory of the State, p. 149 ४. Roucek, J.S., Social Control, New York, 1965, p. 80 ५. वही, पृ० ८०