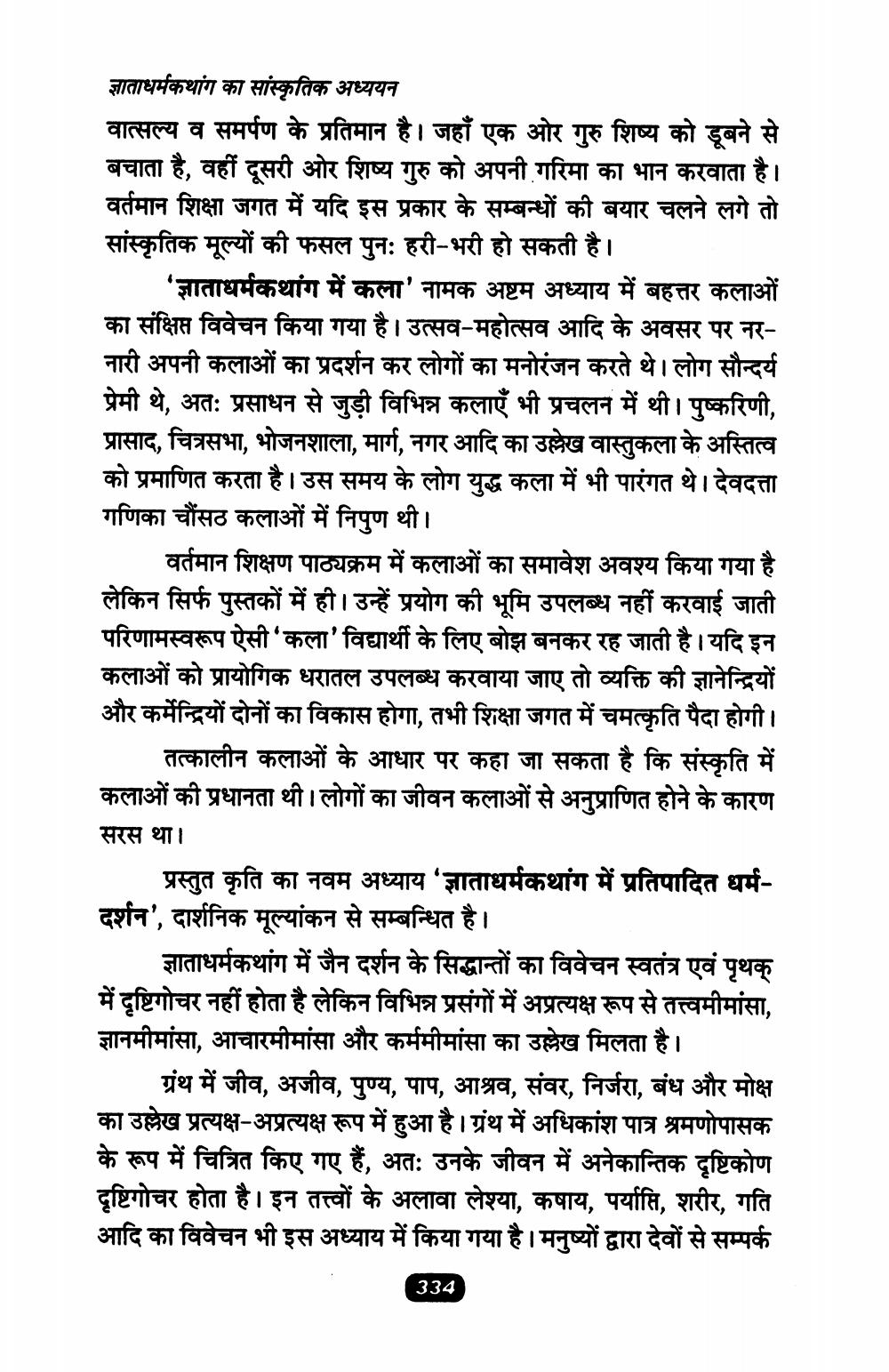________________
ज्ञाताधर्मकथांग का सांस्कृतिक अध्ययन वात्सल्य व समर्पण के प्रतिमान है। जहाँ एक ओर गुरु शिष्य को डूबने से बचाता है, वहीं दूसरी ओर शिष्य गुरु को अपनी गरिमा का भान करवाता है। वर्तमान शिक्षा जगत में यदि इस प्रकार के सम्बन्धों की बयार चलने लगे तो सांस्कृतिक मूल्यों की फसल पुनः हरी-भरी हो सकती है।
_ 'ज्ञाताधर्मकथांग में कला' नामक अष्टम अध्याय में बहत्तर कलाओं का संक्षिप्त विवेचन किया गया है। उत्सव-महोत्सव आदि के अवसर पर नरनारी अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर लोगों का मनोरंजन करते थे। लोग सौन्दर्य प्रेमी थे, अतः प्रसाधन से जुड़ी विभिन्न कलाएँ भी प्रचलन में थी। पुष्करिणी, प्रासाद, चित्रसभा, भोजनशाला, मार्ग, नगर आदि का उल्लेख वास्तुकला के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। उस समय के लोग युद्ध कला में भी पारंगत थे। देवदत्ता गणिका चौंसठ कलाओं में निपुण थी।
वर्तमान शिक्षण पाठ्यक्रम में कलाओं का समावेश अवश्य किया गया है लेकिन सिर्फ पुस्तकों में ही। उन्हें प्रयोग की भूमि उपलब्ध नहीं करवाई जाती परिणामस्वरूप ऐसी'कला' विद्यार्थी के लिए बोझ बनकर रह जाती है। यदि इन कलाओं को प्रायोगिक धरातल उपलब्ध करवाया जाए तो व्यक्ति की ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों दोनों का विकास होगा, तभी शिक्षा जगत में चमत्कृति पैदा होगी।
तत्कालीन कलाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि संस्कृति में कलाओं की प्रधानता थी। लोगों का जीवन कलाओं से अनुप्राणित होने के कारण सरस था।
प्रस्तुत कृति का नवम अध्याय 'ज्ञाताधर्मकथांग में प्रतिपादित धर्मदर्शन', दार्शनिक मूल्यांकन से सम्बन्धित है।
ज्ञाताधर्मकथांग में जैन दर्शन के सिद्धान्तों का विवेचन स्वतंत्र एवं पृथक् में दृष्टिगोचर नहीं होता है लेकिन विभिन्न प्रसंगों में अप्रत्यक्ष रूप से तत्त्वमीमांसा, ज्ञानमीमांसा, आचारमीमांसा और कर्ममीमांसा का उल्लेख मिलता है।
ग्रंथ में जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष का उल्लेख प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप में हुआ है। ग्रंथ में अधिकांश पात्र श्रमणोपासक के रूप में चित्रित किए गए हैं, अत: उनके जीवन में अनेकान्तिक दृष्टिकोण दृष्टिगोचर होता है। इन तत्त्वों के अलावा लेश्या, कषाय, पर्याप्ति, शरीर, गति आदि का विवेचन भी इस अध्याय में किया गया है। मनुष्यों द्वारा देवों से सम्पर्क
334