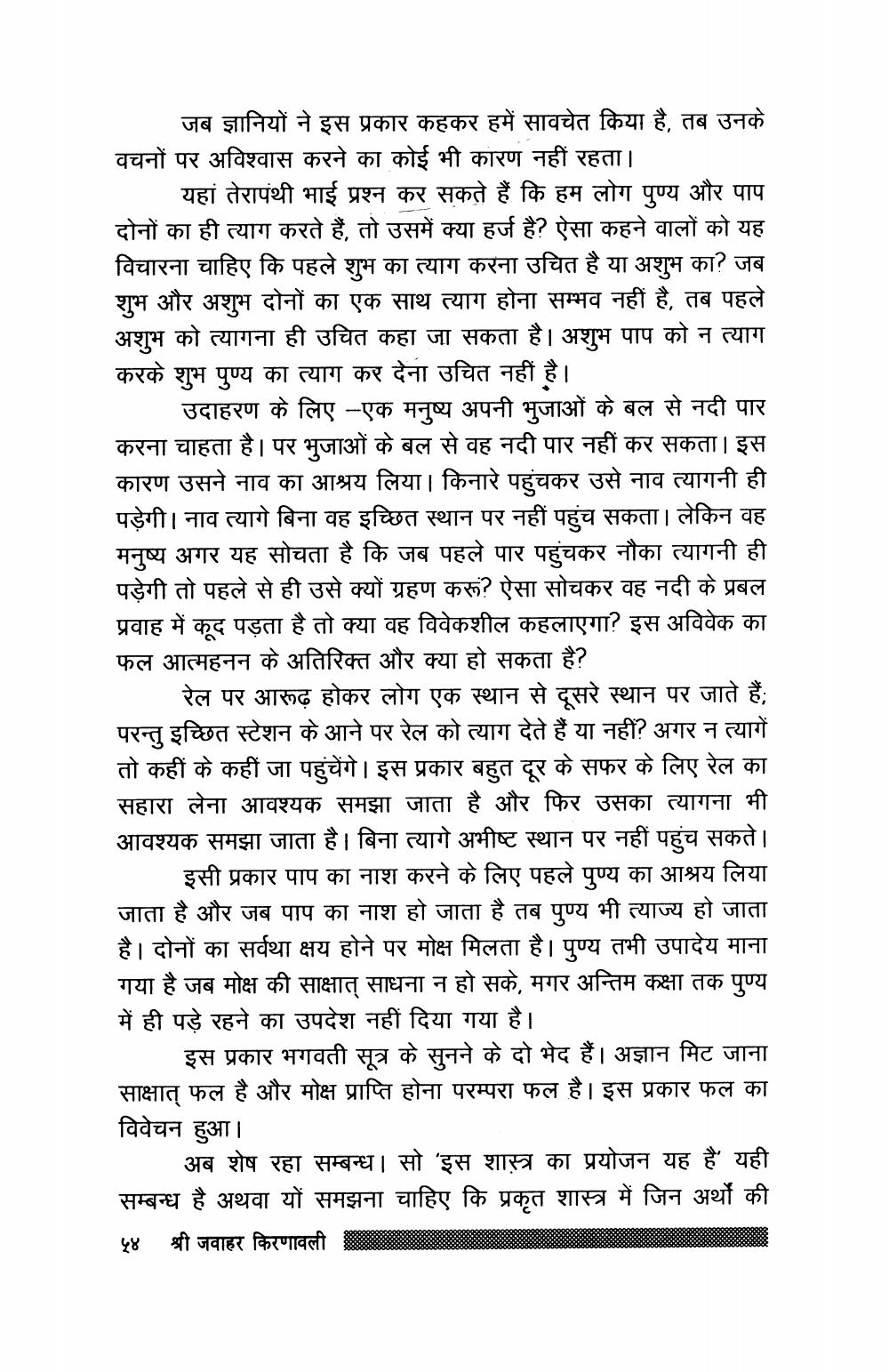________________
जब ज्ञानियों ने इस प्रकार कहकर हमें सावचेत किया है, तब उनके वचनों पर अविश्वास करने का कोई भी कारण नहीं रहता।
यहां तेरापंथी भाई प्रश्न कर सकते हैं कि हम लोग पुण्य और पाप दोनों का ही त्याग करते हैं, तो उसमें क्या हर्ज है? ऐसा कहने वालों को यह विचारना चाहिए कि पहले शुभ का त्याग करना उचित है या अशुभ का? जब शुभ और अशुभ दोनों का एक साथ त्याग होना सम्भव नहीं है, तब पहले अशुभ को त्यागना ही उचित कहा जा सकता है। अशुभ पाप को न त्याग करके शुभ पुण्य का त्याग कर देना उचित नहीं है।
उदाहरण के लिए –एक मनुष्य अपनी भुजाओं के बल से नदी पार करना चाहता है। पर भुजाओं के बल से वह नदी पार नहीं कर सकता। इस कारण उसने नाव का आश्रय लिया। किनारे पहुंचकर उसे नाव त्यागनी ही पड़ेगी। नाव त्यागे बिना वह इच्छित स्थान पर नहीं पहुंच सकता। लेकिन वह मनुष्य अगर यह सोचता है कि जब पहले पार पहुंचकर नौका त्यागनी ही पड़ेगी तो पहले से ही उसे क्यों ग्रहण करूं? ऐसा सोचकर वह नदी के प्रबल प्रवाह में कूद पड़ता है तो क्या वह विवेकशील कहलाएगा? इस अविवेक का फल आत्महनन के अतिरिक्त और क्या हो सकता है?
रेल पर आरूढ़ होकर लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं; परन्तु इच्छित स्टेशन के आने पर रेल को त्याग देते हैं या नहीं? अगर न त्यागें तो कहीं के कहीं जा पहुंचेंगे। इस प्रकार बहुत दूर के सफर के लिए रेल का सहारा लेना आवश्यक समझा जाता है और फिर उसका त्यागना भी आवश्यक समझा जाता है। बिना त्यागे अभीष्ट स्थान पर नहीं पहुंच सकते।
इसी प्रकार पाप का नाश करने के लिए पहले पुण्य का आश्रय लिया जाता है और जब पाप का नाश हो जाता है तब पुण्य भी त्याज्य हो जाता है। दोनों का सर्वथा क्षय होने पर मोक्ष मिलता है। पुण्य तभी उपादेय माना गया है जब मोक्ष की साक्षात् साधना न हो सके, मगर अन्तिम कक्षा तक पुण्य में ही पड़े रहने का उपदेश नहीं दिया गया है।
इस प्रकार भगवती सूत्र के सुनने के दो भेद हैं। अज्ञान मिट जाना साक्षात् फल है और मोक्ष प्राप्ति होना परम्परा फल है। इस प्रकार फल का विवेचन हुआ।
अब शेष रहा सम्बन्ध। सो 'इस शास्त्र का प्रयोजन यह है' यही सम्बन्ध है अथवा यों समझना चाहिए कि प्रकृत शास्त्र में जिन अर्थों की ५४ श्री जवाहर किरणावली