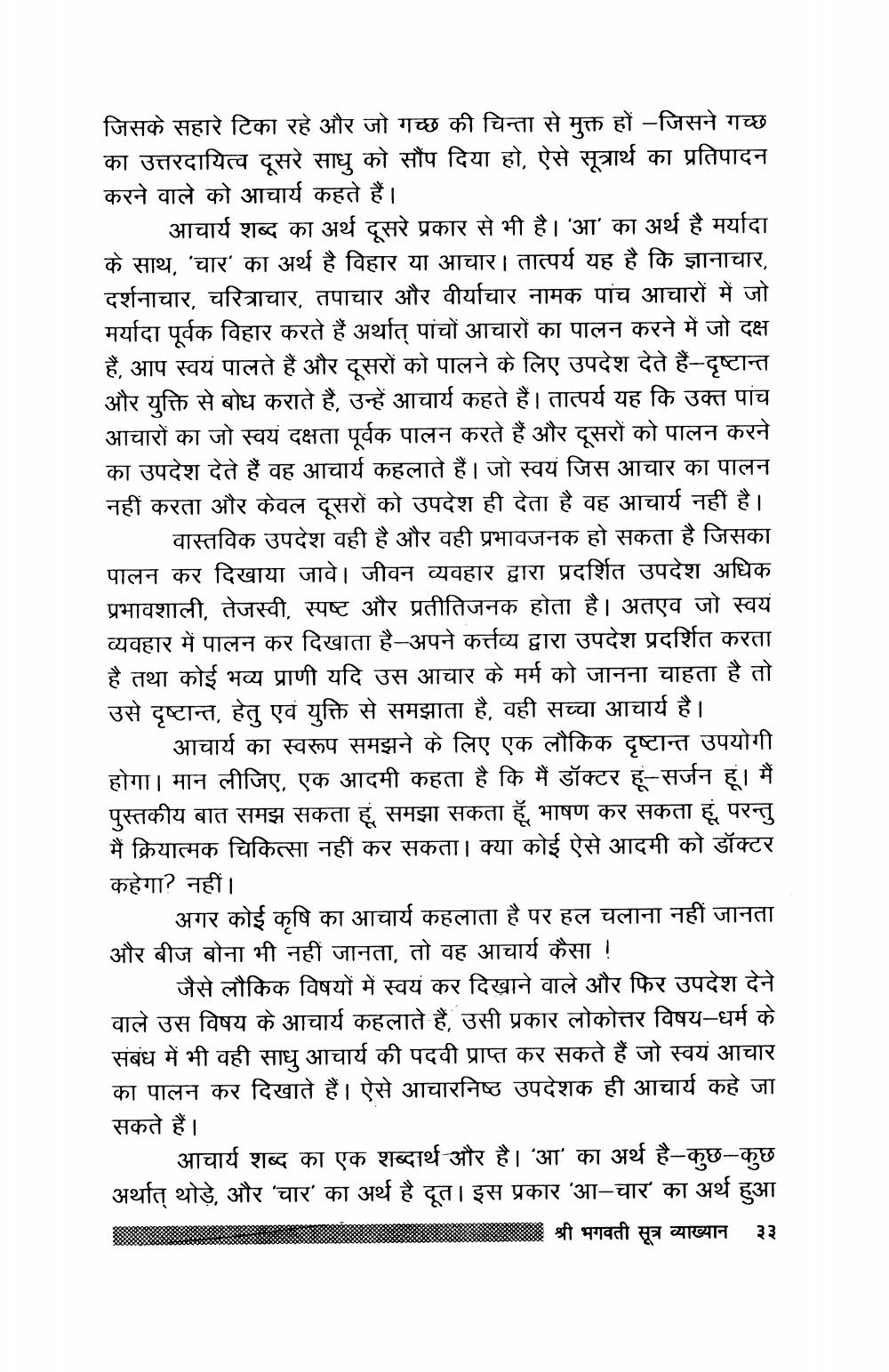________________
जिसके सहारे टिका रहे और जो गच्छ की चिन्ता से मुक्त हों -जिसने गच्छ का उत्तरदायित्व दूसरे साधु को सौंप दिया हो, ऐसे सूत्रार्थ का प्रतिपादन करने वाले को आचार्य कहते हैं।
आचार्य शब्द का अर्थ दूसरे प्रकार से भी है। 'आ' का अर्थ है मर्यादा के साथ, 'चार' का अर्थ है विहार या आचार। तात्पर्य यह है कि ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार, तपाचार और वीर्याचार नामक पांच आचारों में जो मर्यादा पूर्वक विहार करते हैं अर्थात् पांचों आचारों का पालन करने में जो दक्ष हैं, आप स्वयं पालते हैं और दूसरों को पालने के लिए उपदेश देते हैं-दृष्टान्त और युक्ति से बोध कराते हैं, उन्हें आचार्य कहते हैं। तात्पर्य यह कि उक्त पांच आचारों का जो स्वयं दक्षता पूर्वक पालन करते हैं और दूसरों को पालन करने का उपदेश देते हैं वह आचार्य कहलाते हैं। जो स्वयं जिस आचार का पालन नहीं करता और केवल दूसरों को उपदेश ही देता है वह आचार्य नहीं है।
वास्तविक उपदेश वही है और वही प्रभावजनक हो सकता है जिसका पालन कर दिखाया जावे। जीवन व्यवहार द्वारा प्रदर्शित उपदेश अधिक प्रभावशाली, तेजस्वी, स्पष्ट और प्रतीतिजनक होता है। अतएव जो स्वयं व्यवहार में पालन कर दिखाता है-अपने कर्तव्य द्वारा उपदेश प्रदर्शित करता है तथा कोई भव्य प्राणी यदि उस आचार के मर्म को जानना चाहता है तो उसे दृष्टान्त, हेतु एवं युक्ति से समझाता है, वही सच्चा आचार्य है।
आचार्य का स्वरूप समझने के लिए एक लौकिक दृष्टान्त उपयोगी होगा। मान लीजिए, एक आदमी कहता है कि मैं डॉक्टर हूं-सर्जन हूं। मैं पुस्तकीय बात समझ सकता हूं समझा सकता हूँ, भाषण कर सकता हूं परन्तु मैं क्रियात्मक चिकित्सा नहीं कर सकता। क्या कोई ऐसे आदमी को डॉक्टर कहेगा? नहीं।
अगर कोई कृषि का आचार्य कहलाता है पर हल चलाना नहीं जानता और बीज बोना भी नहीं जानता, तो वह आचार्य कैसा !
जैसे लौकिक विषयों में स्वयं कर दिखाने वाले और फिर उपदेश देने वाले उस विषय के आचार्य कहलाते हैं, उसी प्रकार लोकोत्तर विषय-धर्म के संबंध में भी वही साधु आचार्य की पदवी प्राप्त कर सकते हैं जो स्वयं आचार का पालन कर दिखाते हैं। ऐसे आचारनिष्ठ उपदेशक ही आचार्य कहे जा सकते हैं।
__ आचार्य शब्द का एक शब्दार्थ और है। 'आ' का अर्थ है-कुछ-कुछ अर्थात् थोड़े, और 'चार' का अर्थ है दूत। इस प्रकार 'आ-चार का अर्थ हुआ
श्री भगवती सूत्र व्याख्यान ३३
B8