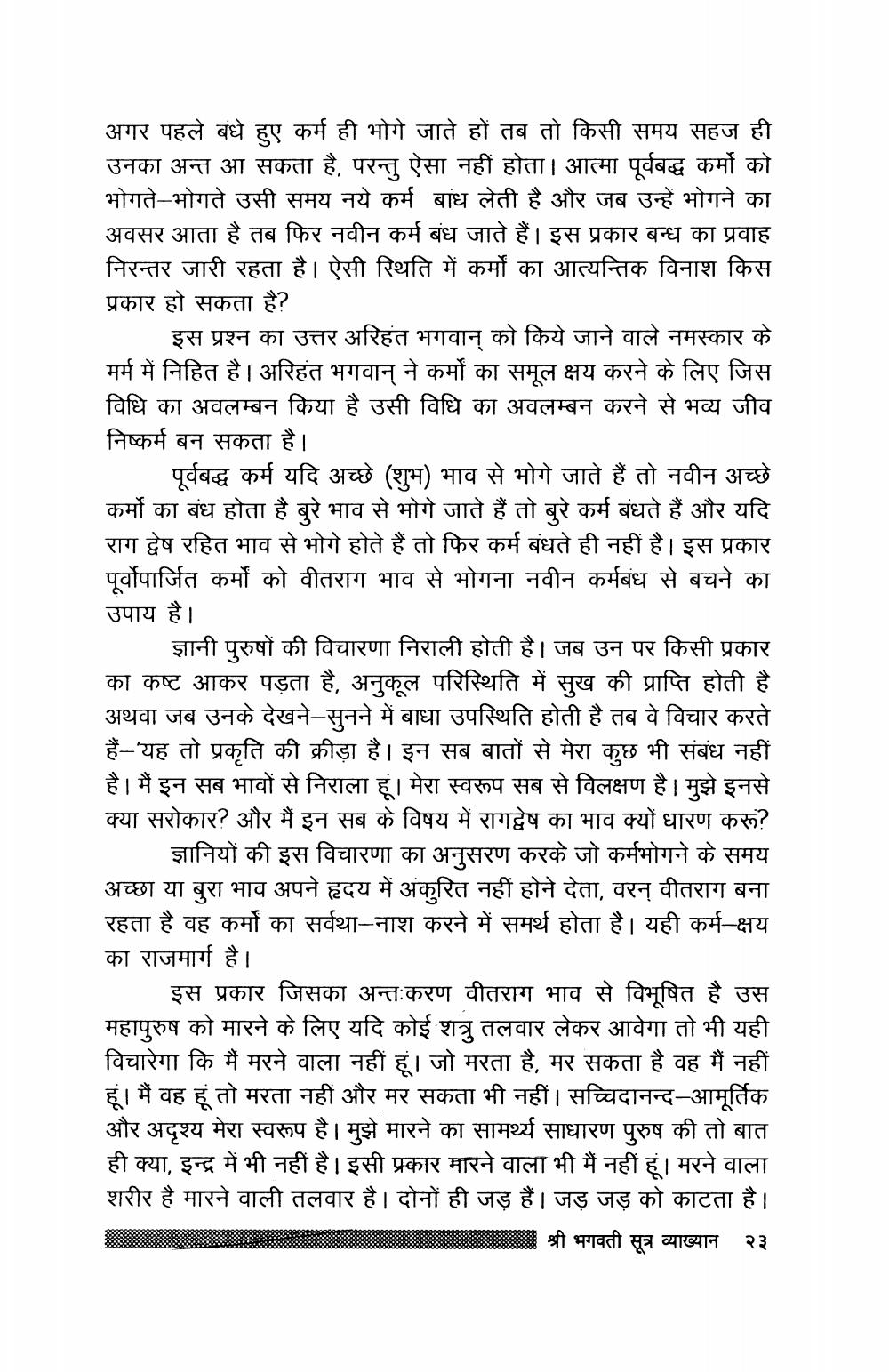________________
अगर पहले बंधे हुए कर्म ही भोगे जाते हों तब तो किसी समय सहज ही उनका अन्त आ सकता है, परन्तु ऐसा नहीं होता । आत्मा पूर्वबद्ध कर्मों को भोगते-भोगते उसी समय नये कर्म बांध लेती है और जब उन्हें भोगने का अवसर आता है तब फिर नवीन कर्म बंध जाते हैं। इस प्रकार बन्ध का प्रवाह निरन्तर जारी रहता है। ऐसी स्थिति में कर्मों का आत्यन्तिक विनाश किस प्रकार हो सकता है?
इस प्रश्न का उत्तर अरिहंत भगवान् को किये जाने वाले नमस्कार के मर्म में निहित है। अरिहंत भगवान् ने कर्मों का समूल क्षय करने के लिए जिस विधि का अवलम्बन किया है उसी विधि का अवलम्बन करने से भव्य जीव निष्कर्म बन सकता है ।
पूर्वबद्ध कर्म यदि अच्छे (शुभ) भाव से भोगे जाते हैं तो नवीन अच्छे कर्मों का बंध होता है बुरे भाव से भोगे जाते हैं तो बुरे कर्म बंधते हैं और यदि राग द्वेष रहित भाव से भोगे होते हैं तो फिर कर्म बंधते ही नहीं है । इस प्रकार पूर्वोपार्जित कर्मों को वीतराग भाव से भोगना नवीन कर्मबंध से बचने का उपाय है।
ज्ञानी पुरुषों की विचारणा निराली होती है। जब उन पर किसी प्रकार का कष्ट आकर पड़ता है, अनुकूल परिस्थिति में सुख की प्राप्ति होती है अथवा जब उनके देखने-सुनने में बाधा उपस्थिति होती है तब वे विचार करते हैं - यह तो प्रकृति की क्रीड़ा है। इन सब बातों से मेरा कुछ भी संबंध नहीं है। मैं इन सब भावों से निराला हूं। मेरा स्वरूप सब से विलक्षण है। मुझे इनसे क्या सरोकार ? और मैं इन सब के विषय में रागद्वेष का भाव क्यों धारण करू ? ज्ञानियों की इस विचारणा का अनुसरण करके जो कर्मभोगने के समय अच्छा या बुरा भाव अपने हृदय में अंकुरित नहीं होने देता, वरन् वीतराग बना रहता है वह कर्मों का सर्वथा नाश करने में समर्थ होता है । यही कर्म-क्षय का राजमार्ग है।
इस प्रकार जिसका अन्तःकरण वीतराग भाव से विभूषित है उस महापुरुष को मारने के लिए यदि कोई शत्रु तलवार लेकर आवेगा तो भी यही विचारेगा कि मैं मरने वाला नहीं हूं। जो मरता है, मर सकता है वह मैं नहीं हूं। मैं वह हूं तो मरता नहीं और मर सकता भी नहीं । सच्चिदानन्द - आमूर्तिक और अदृश्य मेरा स्वरूप है । मुझे मारने का सामर्थ्य साधारण पुरुष की तो बात ही क्या, इन्द्र में भी नहीं है। इसी प्रकार मारने वाला भी मैं नहीं हूं। मरने वाला शरीर है मारने वाली तलवार है। दोनों ही जड़ हैं। जड़ जड़ को काटता है ।
श्री भगवती सूत्र व्याख्यान २३