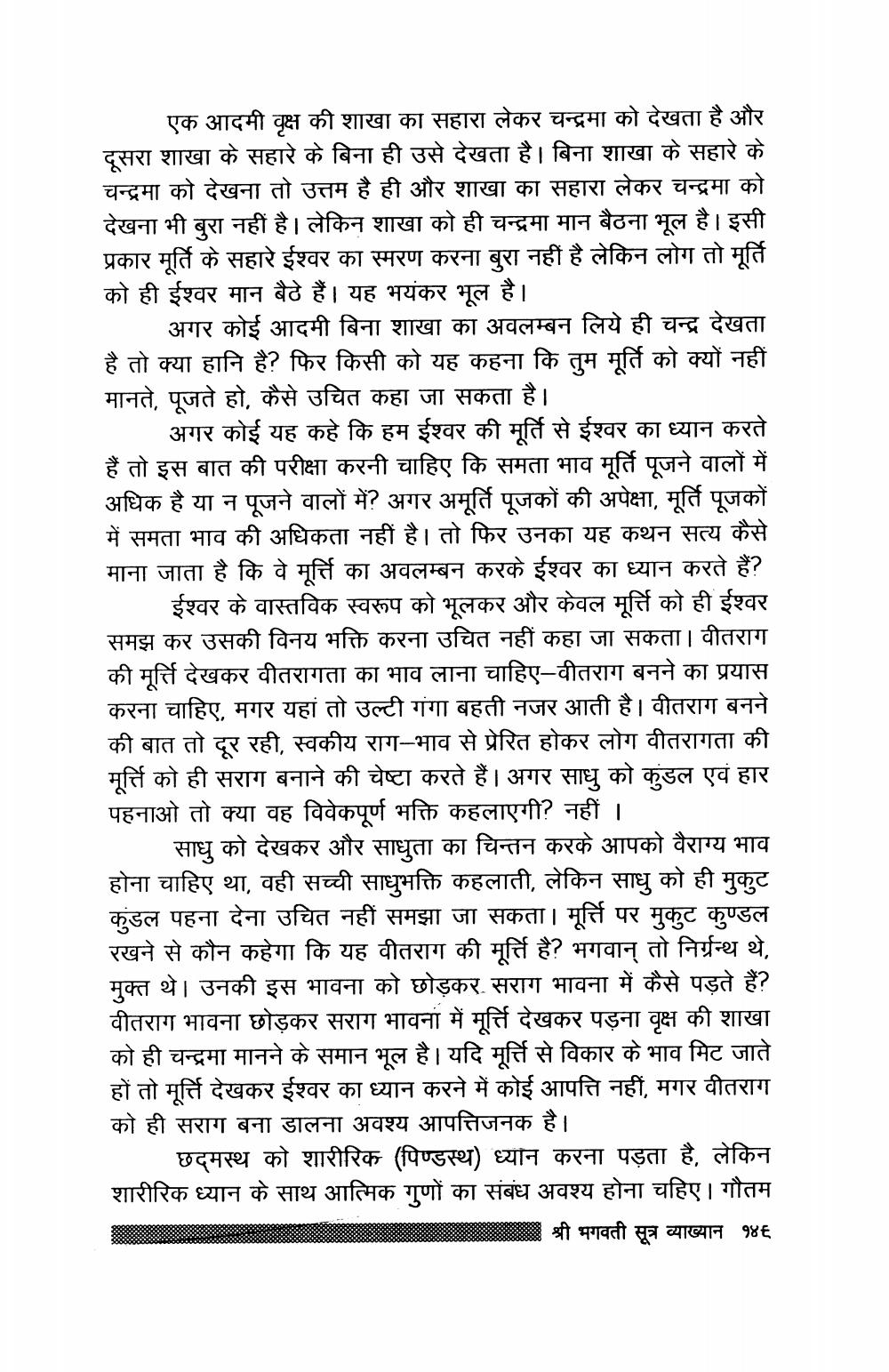________________
एक आदमी वृक्ष की शाखा का सहारा लेकर चन्द्रमा को देखता है और दूसरा शाखा के सहारे के बिना ही उसे देखता है। बिना शाखा के सहारे के चन्द्रमा को देखना तो उत्तम है ही और शाखा का सहारा लेकर चन्द्रमा को देखना भी बुरा नहीं है । लेकिन शाखा को ही चन्द्रमा मान बैठना भूल है । इसी प्रकार मूर्ति के सहारे ईश्वर का स्मरण करना बुरा नहीं है लेकिन लोग तो मूर्ति को ही ईश्वर मान बैठे हैं। यह भयंकर भूल है ।
अगर कोई आदमी बिना शाखा का अवलम्बन लिये ही चन्द्र देखता है तो क्या हानि है? फिर किसी को यह कहना कि तुम मूर्ति को क्यों नहीं मानते, पूजते हो, कैसे उचित कहा जा सकता है।
अगर कोई यह कहे कि हम ईश्वर की मूर्ति से ईश्वर का ध्यान करते हैं तो इस बात की परीक्षा करनी चाहिए कि समता भाव मूर्ति पूजने वालों में अधिक है या न पूजने वालों में? अगर अमूर्ति पूजकों की अपेक्षा, मूर्ति पूजकों में समता भाव की अधिकता नहीं है। तो फिर उनका यह कथन सत्य कैसे माना जाता है कि वे मूर्ति का अवलम्बन करके ईश्वर का ध्यान करते हैं? ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को भूलकर और केवल मूर्त्ति को ही ईश्वर समझ कर उसकी विनय भक्ति करना उचित नहीं कहा जा सकता। वीतराग की मूर्ति देखकर वीतरागता का भाव लाना चाहिए - वीतराग बनने का प्रयास करना चाहिए, मगर यहां तो उल्टी गंगा बहती नजर आती है। वीतराग बनने की बात तो दूर रही, स्वकीय राग-भाव से प्रेरित होकर लोग वीतरागता की मूर्ति को ही सराग बनाने की चेष्टा करते हैं। अगर साधु को कुंडल एवं हार पहनाओ तो क्या वह विवेकपूर्ण भक्ति कहलाएगी? नहीं ।
साधु को देखकर और साधुता का चिन्तन करके आपको वैराग्य भाव होना चाहिए था, वही सच्ची साधुभक्ति कहलाती, लेकिन साधु को ही मुकुट कुंडल पहना देना उचित नहीं समझा जा सकता । मूर्त्ति पर मुकुट कुण्डल रखने से कौन कहेगा कि यह वीतराग की मूर्ति है ? भगवान् तो निर्ग्रन्थ थे, मुक्त थे। उनकी इस भावना को छोड़कर सराग भावना में कैसे पड़ते हैं? वीतराग भावना छोड़कर सराग भावना में मूर्त्ति देखकर पड़ना वृक्ष की शाखा को ही चन्द्रमा मानने के समान भूल है । यदि मूर्ति से विकार के भाव मिट जाते हों तो मूर्त्ति देखकर ईश्वर का ध्यान करने में कोई आपत्ति नहीं, मगर वीतराग को ही सराग बना डालना अवश्य आपत्तिजनक है ।
छद्मस्थ को शारीरिक ( पिण्डस्थ) ध्यान करना पड़ता है, लेकिन शारीरिक ध्यान के साथ आत्मिक गुणों का संबंध अवश्य होना चहिए । गौतम श्री भगवती सूत्र व्याख्यान १४६