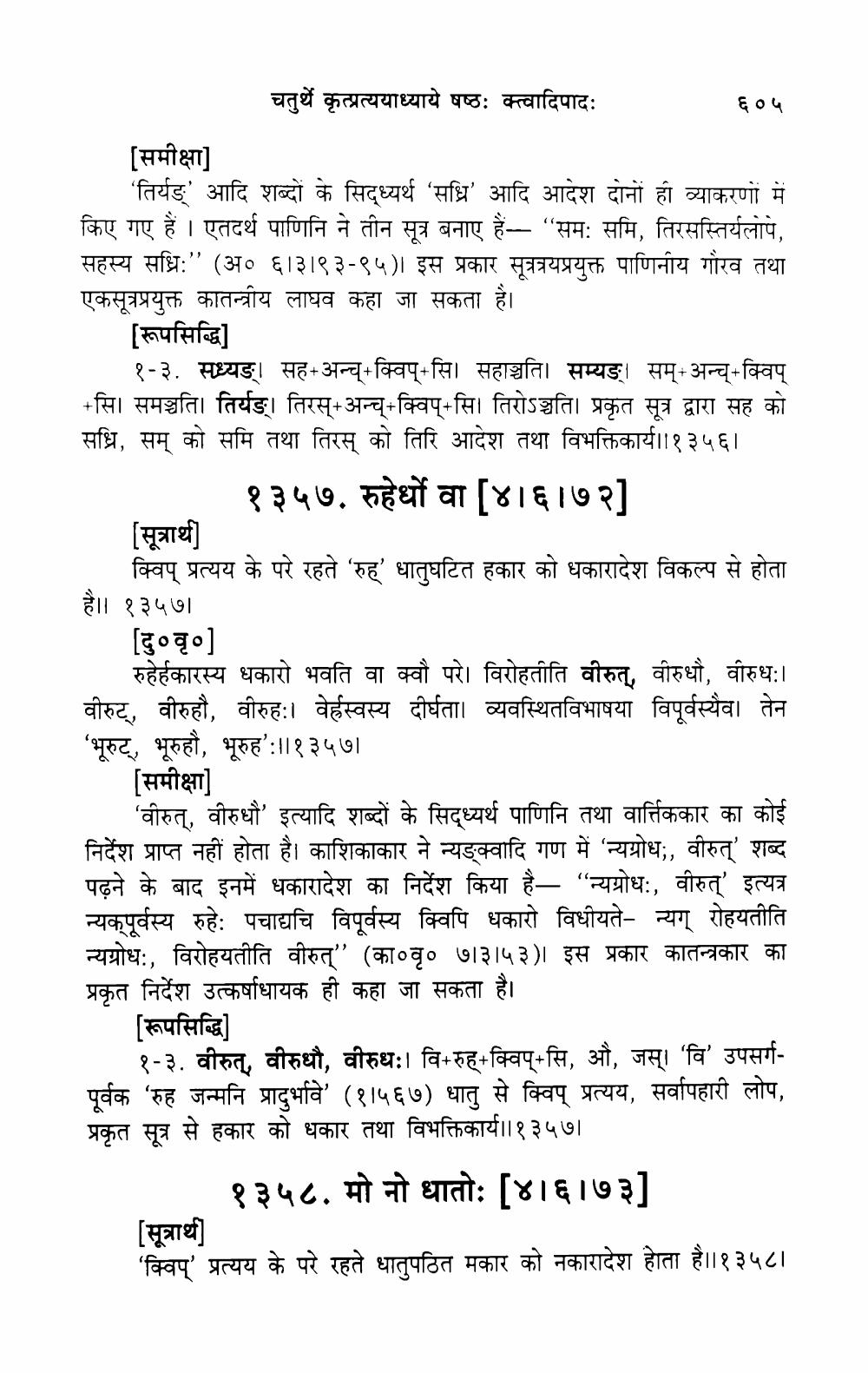________________
चतुर्थे कृत्प्रत्ययाध्याये षष्ठः क्त्वादिपादः
६०५
[समीक्षा]
'तिर्यङ्' आदि शब्दों के सिद्ध्यर्थ 'सधि' आदि आदेश दोनों ही व्याकरणों में किए गए हैं । एतदर्थ पाणिनि ने तीन सूत्र बनाए हैं- "समः समि, तिरसस्तिर्यलोपे, सहस्य सध्रि:” (अ० ६ । ३ । ९३-९५ ) । इस प्रकार सूत्रत्रयप्रयुक्त पाणिनीय गौरव तथा एकसूत्रप्रयुक्त कातन्त्रीय लाघव कहा जा सकता है।
[रूपसिद्धि]
१-३. सध्यङ् । सह + अन्च् + क्विप् + सि । सहाञ्चति । सम्यङ् । सम् + अन्च्+ क्विप् +सि। समञ्चति। तिर्यङ्। तिरस् + अन्च् + क्विप् + सि । तिरोऽञ्चति । प्रकृत सूत्र द्वारा सह को सधि, सम् को समि तथा तिरस् को तिरि आदेश तथा विभक्तिकार्य ।। १३५६।
१३५७. रुहेर्धो वा [४।६।७२ ]
[सूत्रार्थ]
क्विप् प्रत्यय के परे रहते 'रुह्' धातुघटित हकार को धकारादेश विकल्प से होता है ।। १३५७
[दु०वृ० ]
रुहेर्हकारस्य धकारो भवति वा क्वौ परे । विरोहतीति वीरुत्, वीरुधौ, वीरुधः । वीरुट्, वीरुहौ, वीरुहः। वेर्हस्वस्य दीर्घता । व्यवस्थितविभाषया विपूर्वस्यैव । तेन 'भूरुट्, भूरुहौ, भूरुह' ।। १३५७।
[समीक्षा]
'वीरुत्, वीरुधौ' इत्यादि शब्दों के सिद्ध्यर्थ पाणिनि तथा वार्त्तिककार का कोई निर्देश प्राप्त नहीं होता है । काशिकाकार ने न्यङ्क्वादि गण में 'न्यग्रोध, वीरुत्' शब्द पढ़ने के बाद इनमें धकारादेश का निर्देश किया है - " न्यग्रोधः, वीरुत्' इत्यत्र न्यक्पूर्वस्य रुहेः पचाद्यचि विपूर्वस्य क्विपि धकारो विधीयते - न्यग् रोहयतीति न्यग्रोधः, विरोहयतीति वीरुत्" (का०वृ० ७।३।५३) । इस प्रकार कातन्त्रकार का प्रकृत निर्देश उत्कर्षाधायक ही कहा जा सकता है।
[रूपसिद्धि]
१- ३. वीरुत्, वीरुधौ, वीरुधः । वि + रुह् + क्विप् + सि, औ, जस्। 'वि' उपसर्गपूर्वक 'रुह जन्मनि प्रादुर्भावे' (१/५६७) धातु से क्विप् प्रत्यय, सर्वापहारी लोप, प्रकृत सूत्र से हकार को धकार तथा विभक्तिकार्य ।। १३५७।
१३५८. मो नो धातोः [४ । ६ । ७३]
[ सूत्रार्थ]
'क्विप्' प्रत्यय के परे रहते धातुपठित मकार को नकारादेश होता है ।। १३५८।