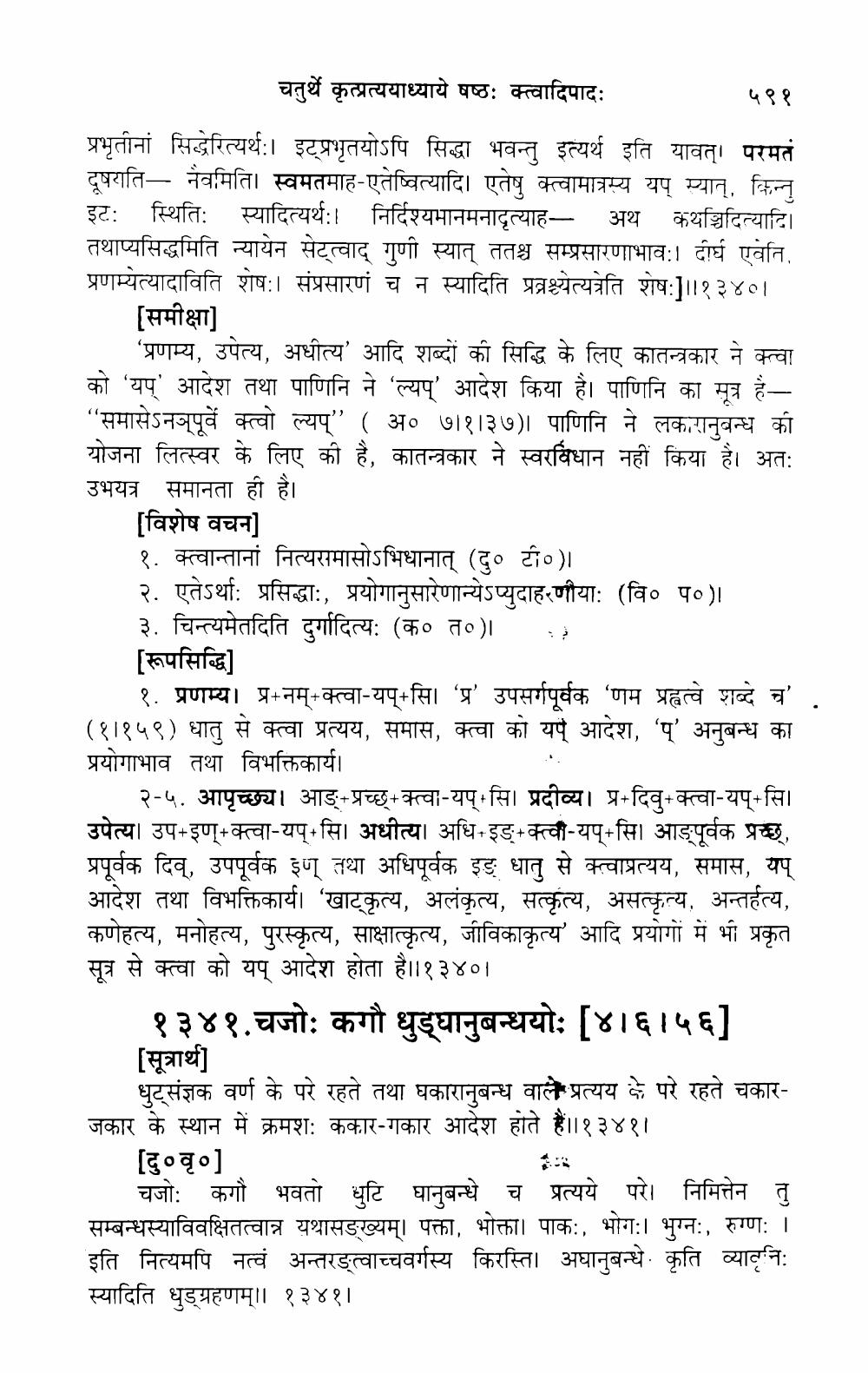________________
चतुर्थे कृत्प्रत्ययाध्याये षष्ठः क्त्वादिपादः प्रभृतीनां सिद्धेरित्यर्थः। इट्प्रभृतयोऽपि सिद्धा भवन्तु इत्यर्थ इति यावत्। परमतं दूषगति- नैवमिति। स्वमतमाह-एतेष्वित्यादि। एतेषु क्त्वामात्रस्य यप् स्यात्, किन्तु इट: स्थितिः स्यादित्यर्थः। निर्दिश्यभानमनादृत्याह- अथ कथञ्चिदित्यादि। तथाप्यसिद्धमिति न्यायेन सेट्त्वाद् गुणी स्यात् ततश्च सम्प्रसारणाभावः। दीर्घ एवंति. प्रणम्येत्यादाविति शेषः। संप्रसारणं च न स्यादिति प्रव्रश्श्येत्यत्रेति शेष:]||१३४०।
[समीक्षा]
'प्रणम्य, उपेत्य, अधीत्य' आदि शब्दों की सिद्धि के लिए कातन्त्रकार ने क्त्वा को ‘यप्' आदेश तथा पाणिनि ने 'ल्यप्' आदेश किया है। पाणिनि का सूत्र है“समासेऽनपूर्वे क्त्वो ल्यप्” ( अ० ७।१।३७)। पाणिनि ने लकारानुबन्ध की योजना लित्स्वर के लिए की है, कातन्त्रकार ने स्वरविधान नहीं किया है। अत: उभयत्र समानता ही है।
[विशेष वचन] १. क्त्वान्तानां नित्यसमासोऽभिधानात् (दु० टी०)। २. एतेऽर्थाः प्रसिद्धाः, प्रयोगानुसारेणान्येऽप्युदाहरणीयाः (वि० प०)। ३. चिन्त्यमेतदिति दुर्गादित्य: (क० त०)। [रूपसिद्धि]
१. प्रणम्य। प्र नम्+क्त्वा-यप+सि। 'प्र' उपसर्गपूर्वक ‘णम प्रह्वत्वे शब्द च' (१।१५९) धातु से क्त्वा प्रत्यय, समास, क्त्वा को यप आदेश, ‘प्' अनुबन्ध का प्रयोगाभाव तथा विभक्तिकार्य।
२-५. आपृच्छ्य। आङ्-प्रच्छ+क्त्वा-यप्सि। प्रदीव्य। प्र+दिवु+क्त्वा-यप्-सि। उपेत्य। उप-इण्+क्त्वा-यप्+सि। अधीत्य। अधि, इङ्+क्त्वा-यप्+सि। आफूर्वक प्रच्छ्, प्रपूर्वक दिव्, उपपूर्वक इण तथा अधिपूर्वक इङ् धातु से क्त्वाप्रत्यय, समास, यप् आदेश तथा विभक्तिकार्य। 'खाट्कृत्य, अलंकृत्य, सत्कृत्य, असत्कृत्य, अन्तर्हत्य, कणेहत्य, मनोहत्य, पुरस्कृत्य, साक्षात्कृत्य, जीविकाकृत्य' आदि प्रयोगों में भी प्रकृत सूत्र से क्त्वा को यप् आदेश होता है।।१३४०।
१३४१.चजोः कगौ धुड्यानुबन्धयोः [४।६।५६] [सूत्रार्थ]
धुटसंज्ञक वर्ण के परे रहते तथा घकारानुबन्ध वाले प्रत्यय के परे रहते चकारजकार के स्थान में क्रमश: ककार-गकार आदेश होते हैं।।१३४१।
[दु०वृ०]
चजोः कगौ भवतो धुटि घानुबन्धे च प्रत्यये परे। निमित्तेन तु सम्बन्धस्याविवक्षितत्वान्न यथासङ्ख्यम्। पक्ता, भोक्ता। पाकः, भोग:। भुग्नः, रुग्णः । इति नित्यमपि नत्वं अन्तरङ्त्वाच्चवर्गस्य किरस्ति। अघानुबन्धे. कृति व्यावृनिः स्यादिति धुड्ग्रहणम्।। १३४१।