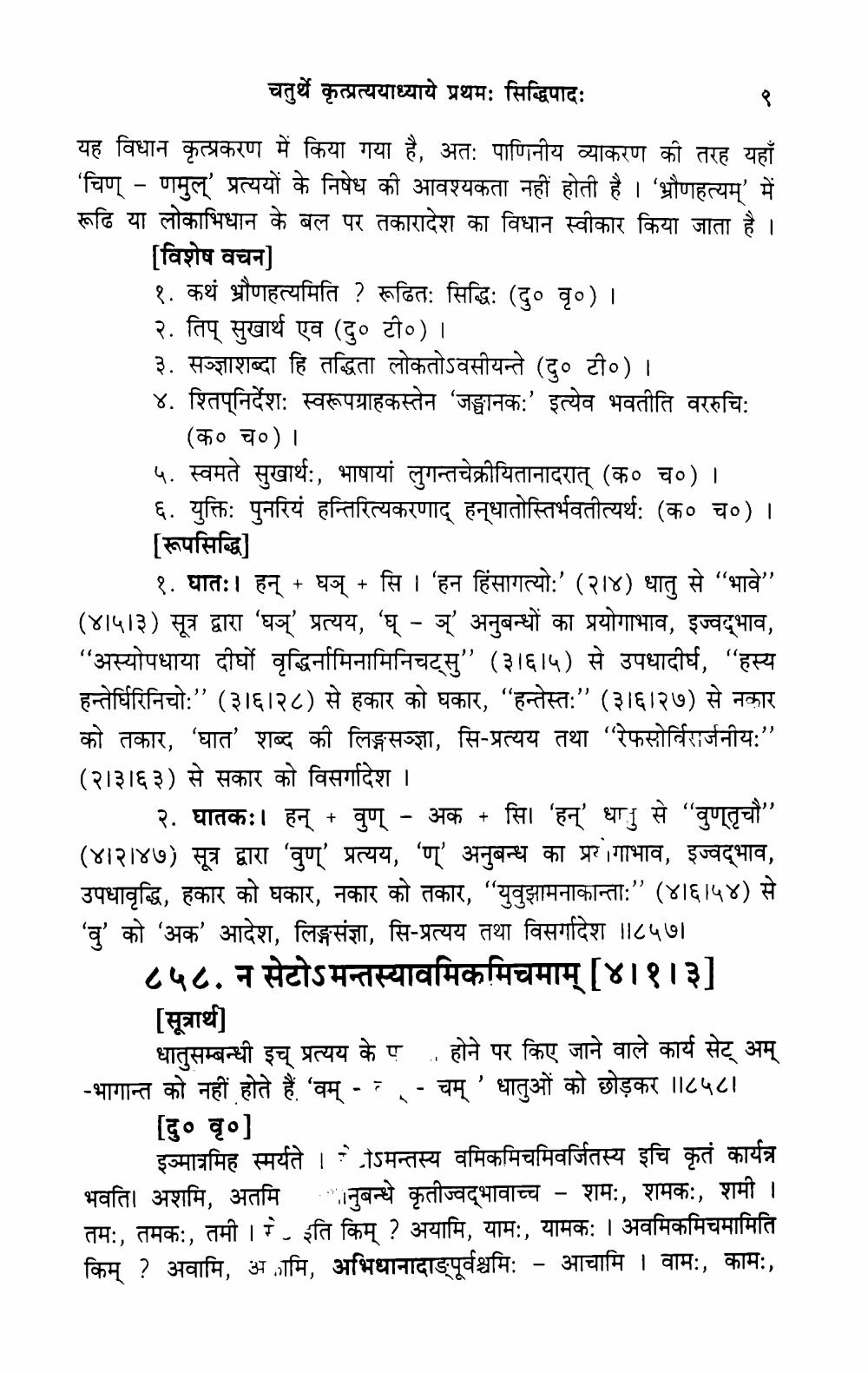________________
चतुर्थे कृत्प्रत्ययाध्याये प्रथमः सिद्धिपादः यह विधान कृत्प्रकरण में किया गया है, अत: पाणिनीय व्याकरण की तरह यहाँ 'चिण् - णमुल्' प्रत्ययों के निषेध की आवश्यकता नहीं होती है । 'भ्रौणहत्यम्' में रूढि या लोकाभिधान के बल पर तकारादेश का विधान स्वीकार किया जाता है ।
[विशेष वचन १. कथं भ्रौणहत्यमिति ? रूढित: सिद्धि: (दु० वृ०) । २. तिप् सुखार्थ एव (दु० टी०)। ३. सज्ञाशब्दा हि तद्धिता लोकतोऽवसीयन्ते (दु० टी०) । ४. स्तिनिर्देश: स्वरूपग्राहकस्तेन 'जङ्घानकः' इत्येव भवतीति वररुचिः
(क० च०) । ५. स्वमते सुखार्थः, भाषायां लुगन्तचेक्रीयितानादरात् (क० च०) । ६. युक्तिः पुनरियं हन्तिरित्यकरणाद् हन्धातोस्तिर्भवतीत्यर्थः (क० च०) । [रूपसिद्धि]
१. घातः। हन् + घञ् + सि । 'हन हिंसागत्योः' (२।४) धातु से “भावे" (४।५।३) सूत्र द्वारा ‘घञ्' प्रत्यय, ‘घ् - ज्' अनुबन्धों का प्रयोगाभाव, इज्वद्भाव, "अस्योपधाया दीघों वृद्धिर्नामिनामिनिचट्सु' (३।६।५) से उपधादीर्घ, “हस्य हन्तेषिरिनिचोः' (३।६।२८) से हकार को घकार, “हन्तेस्तः'' (३।६।२७) से नकार को तकार, 'घात' शब्द की लिङ्गसञ्जा, सि-प्रत्यय तथा “रेफसोर्विसर्जनीयः" (२।३।६३) से सकार को विसर्गादेश ।।
२. घातकः। हन् + वुण् - अक + सि। 'हन्' धातु से “वुण्तृचौ" (४।२।४७) सूत्र द्वारा 'वुण्' प्रत्यय, 'ण' अनुबन्ध का प्ररोगाभाव, इज्वद्भाव, उपधावृद्धि, हकार को घकार, नकार को तकार, “युवुझामनाकान्ताः' (४।६।५४) से 'वु' को 'अक' आदेश, लिङ्गसंज्ञा, सि-प्रत्यय तथा विसर्गादेश ||८५७।
८५८. न सेटोऽमन्तस्यावमिकमिचमाम् [४।१।३] [सूत्रार्थ]
धातुसम्बन्धी इच् प्रत्यय के ए .. होने पर किए जाने वाले कार्य सेट अम् -भागान्त को नहीं होते हैं. 'वम् - - चम् ' धातुओं को छोड़कर ।।८५८।
[दु० वृ०]
इमात्रमिह स्मर्यते । ऽमन्तस्य वमिकमिचमिवर्जितस्य इचि कृतं कार्यत्र भवति। अशमि, अतमि नुबन्धे कृतीज्वभावाच्च - शमः, शमकः, शमी । तमः, तमकः, तमी । रे - इति किम् ? अयामि, यामः, यामकः । अवमिकमिचमामिति किम् ? अवामि, अामि, अभिधानादापर्वश्चमिः - आचामि । वामः, कामः,