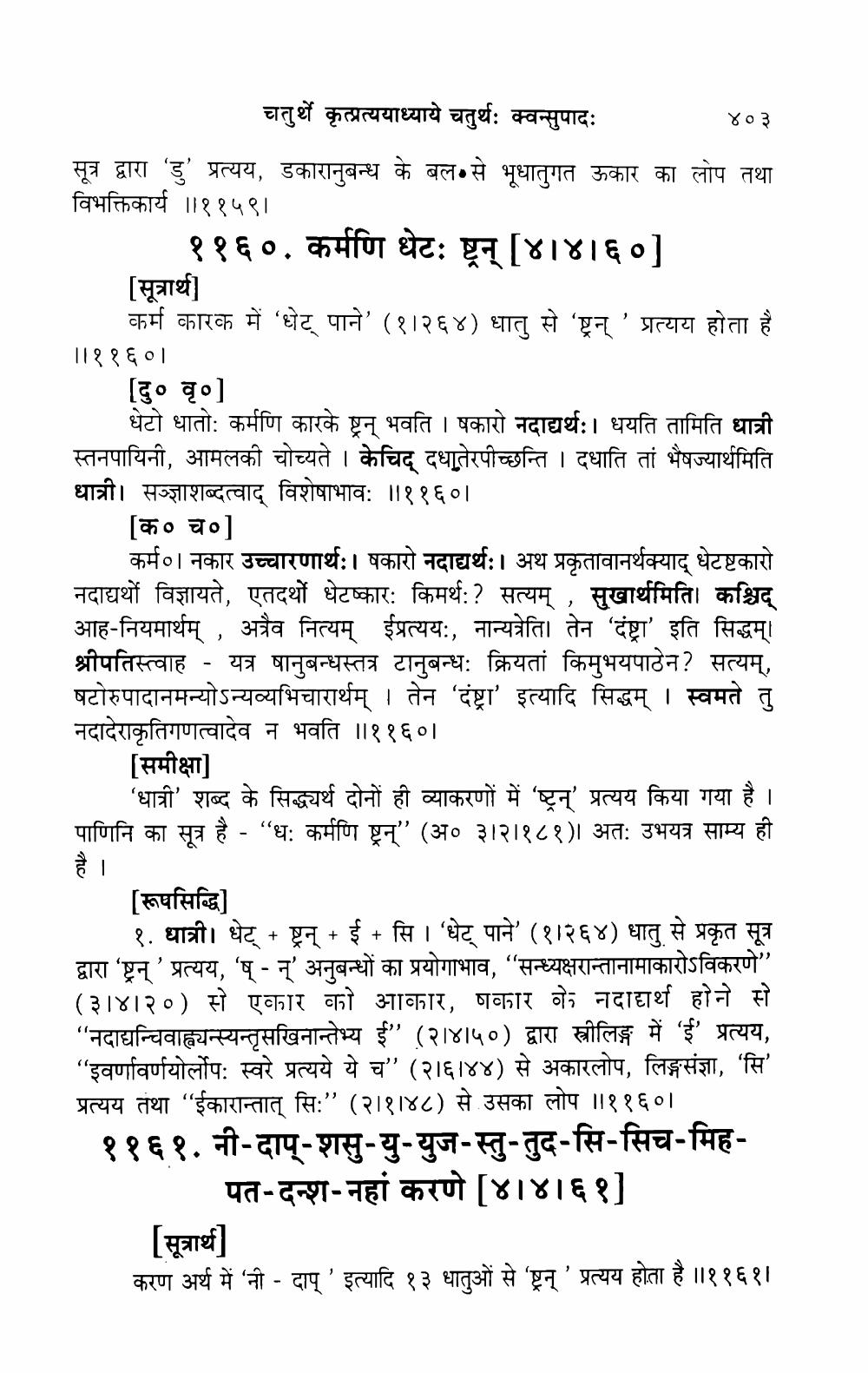________________
चतुर्थे कृत्प्रत्ययाध्याये चतुर्थः क्वन्सुपादः
४०३ सूत्र द्वारा ‘डु' प्रत्यय, डकारानुबन्ध के बल से भूधातुगत ऊकार का लोप तथा विभक्तिकार्य ॥११५९।।
११६०. कर्मणि धेटः ष्टन् [४।४।६०] [सूत्रार्थ
कर्म कारक में 'धेट पाने' (१।२६४) धातु से ‘ष्ट्रन् ' प्रत्यय होता है ।।११६०।
[दु० वृ०]
धेटो धातोः कर्मणि कारके ष्ट्रन् भवति । षकारो नदाद्यर्थः। धयति तामिति धात्री स्तनपायिनी, आमलकी चोच्यते । केचिद् दधातेरपीच्छन्ति । दधाति तां भैषज्यार्थमिति धात्री। सज्ञाशब्दत्वाद् विशेषाभावः ॥११६०।
[क० च०]
कर्म०। नकार उच्चारणार्थः। षकारो नदाद्यर्थः। अथ प्रकृतावानर्थक्याद् धेटष्टकारो नदाद्यर्थो विज्ञायते, एतदर्थो धेटष्कार: किमर्थः? सत्यम् , सुखार्थमिति। कश्चिद् आह-नियमार्थम् , अत्रैव नित्यम् ईप्रत्ययः, नान्यत्रेति। तेन ‘दंष्ट्रा' इति सिद्धम्। श्रीपतिस्त्वाह - यत्र षानुबन्धस्तत्र टानुबन्धः क्रियतां किमुभयपाठेन? सत्यम्, षटोरुपादानमन्योऽन्यव्यभिचारार्थम् । तेन ‘दंष्ट्रा' इत्यादि सिद्धम् । स्वमते तु नदादेराकृतिगणत्वादेव न भवति ।।११६०।
[समीक्षा]
'धात्री' शब्द के सिद्ध्यर्थ दोनों ही व्याकरणों में ‘ष्ट्रन्' प्रत्यय किया गया है । पाणिनि का सूत्र है - "ध: कर्मणि ष्ट्रन्' (अ० ३।२।१८१)। अत: उभयत्र साम्य ही
[रूपसिद्धि]
१. धात्री। धेट् + ष्ट्रन् + ई + सि । 'धेट पाने' (१।२६४) धातु से प्रकृत सूत्र द्वारा 'ष्ट्रन् ' प्रत्यय, 'ष् - न्' अनुबन्धों का प्रयोगाभाव, “सन्ध्यक्षरान्तानामाकारोऽविकरणे" (३।४।२०) से एकार को आकार, षकार के नदाघार्थ होने से "नदाद्यन्चिवायन्स्यन्तृसखिनान्तेभ्य ई" (२।४।५०) द्वारा स्त्रीलिङ्ग में 'ई' प्रत्यय, "इवर्णावर्णयोर्लोप: स्वरे प्रत्यये ये च' (२।६।४४) से अकारलोप, लिङ्गसंज्ञा, 'सि' प्रत्यय तथा “ईकारान्तात् सिः' (२।१।४८) से उसका लोप ॥११६०। ११६१. नी-दाप-शसु-यु-युज-स्तु-तुद-सि-सिच-मिह
पत-दन्श-नहां करणे [४।४।६१] [सूत्रार्थ] करण अर्थ में 'नी - दाप् ' इत्यादि १३ धातुओं से 'ष्ट्रन् ' प्रत्यय होता है ।।११६१।